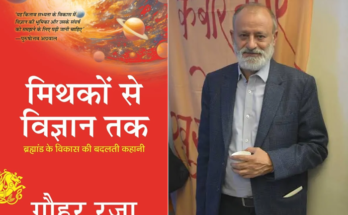गत दो-तीन दशकों में वाम लेखक संगठनों का प्रभाव क्षीण हुआ है। उनमें कई तरह के विचलन, विभ्रम और विरूपताएं देखने को मिल रही हैं। गत दिनों भाजपा मनोनीत एक राज्यपाल की जीवनी का संपादन राज्य के दो वरिष्ठ प्रगतिशील लेखकों द्वारा किया जाना इसका एक सामयिक उदाहरण है। इन लेखकों के इस कृत्य के बारे में न प्रलेस राज्य संगठन ने कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण दिया न ही राष्ट्रीय संगठन ने। उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना तो दूर की बात है।
विडंबना यह है कि जब ये लेखक संगठन अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं तब ये अपनी कमजोरियों को अपने मौन से व्याख्यायित कर रहे हैं। ऐसे में नैतिकता की बात करना वाकई कष्टदायक है। वाम लेखक संगठनों का एक गौरवपूर्ण इतिहास है जिसे समझना संप्रति आवश्यक भी है और उचित भी है। प्रगतिशील लेखक संघ के जन्म के पाँच साल में ही देश की हर भाषा में यह आन्दोलन अपनी जड़ें जमा चुका था। प्रत्येक भाषा के बड़े रचनाकार इस आन्दोलन के साथ थे। बड़ी दिलचस्प बात है कि इसके स्थापना सम्मेलन के समय अधिकांश उर्दू के विद्वान थे तथा हिन्दी के कुछ ही लेखक थे। इनमें बड़े नाम प्रेमचंद एवं जैनेन्द्र के थे। उस समय के नौजवान रचनाकार रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, राहुल सांकृत्यायन आदि भी शामिल थे लेकिन बड़ी संख्या उर्दू लेखकों की ही थी, जो प्रगतिशील आन्दोलन में प्राण फूंकने में लगे थे।
अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सरकारी हमले के खिलाफ़ लेखक संगठनों का संयुक्त बयान
उर्दू लेखकों में सज्जाद जहीर, डॉ. रशीद जहाँ, डॉ. अब्दुल अलीम, मजाज, फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी, मौलाना हसरत मुहानी, सागर निजामी, महमूदुज्जफर, चौधरी मौहम्मद अली रुदौलवी आदि सुप्रसिद्ध रहे हैं। और भी बहुत से नौजवान रचनाकार इसमें सक्रिय थे जो आगे चलकर बड़े लेखक हुए। साथ ही प्रगतिशील आन्दोलन का आधार स्तम्भ भी बने। इस आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्य देश को विदेशी शासन के मुक्ति तथा साधारण लोगों के लिए आजादी का महत्त्व बताना था, लेकिन एक ऐसा वर्ग था जो जमींदारों एवं पूँजीपतियों से मुक्ति चाहता था। इनमें से अधिकांश मार्क्सवाद से प्रभावित थे। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें ऊँच-नीच का भेदभाव न हो। शोषण आधारित व्यक्तिगत सम्पत्ति इकट्ठी करने का अधिकार न हो। महिलाओं एवं दलितों को समान अधिकार दिलाने की बात की गई। जिन चार लोगों ने सम्मेलन के आयोजन में सबसे बडी भूमिका निभाई उनमें बन्ने भाई के अलावा डॉ. रशीद जहाँ, डॉ. अब्दुल अलीम तथा महमूदुज्जफर शामिल थे। बन्ने भाई और रशीद जहाँ की भूमिका की उनके शताब्दी वर्ष में काफी चर्चा हुई, किन्तु डॉ. अब्दुल अलीम के योगदान को प्रमुखता से रेखांकित नहीं किया गया।
मुंशी प्रेमचंद की भी इसमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। प्रेमचंद तो सबके प्रेरणास्रोत थे। जिस आशा और विश्वास के साथ वे अपना किराया लगाकार सज्जाद जहीर के घर पहुंच गये तथा बिना औपचारिकताओं के बेतकल्लुफ होकर मिले इससे सभी अभिभूत थे। उन्हें शरद बाबू ने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। उनका इस सादगी से आना तथा प्रगतिशील लेखकों एवं साहित्य की परिभाषा को व्याख्यायित करते हुए उसे जनता से जोड़ना एक नये आन्दोलन को जन्म देना था। प्रेमचंद ने सबसे पहले यह कहा कि सच्चे साहित्य की नींव मानवीय सौन्दर्य, आजादी और मानवीय जज्बों पर आधारित होनी चाहिए। मौलाना हसरत मुहानी की तकरीर ने भी प्रगतिशील आन्दोलन के स्वरूप के नये अंदाज को पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे साहित्य को राष्ट्रीय मुक्ति का स्वर बनना चाहिए। उसे साम्राज्यवादियों तथा अत्याचारी अमीरों का प्रतिरोध करना चाहिए। उसे मजदूरों, किसानों तथा शोषितों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक साहित्य को समाजवाद का सद्उपदेश देना चाहिए।
प्रेमचंद का सूरदास आज भी ज़मीन हड़पे जाने का विरोध कर रहा है और गोली खा रहा है!
आजादी के बाद यह संगठन कमजोर होने लगा। इसके कारण कुछ व्यक्ति नहीं हैं। लोगों का यह ख्याल गलत है कि रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान तथा हिन्दी-उर्दू के विवाद के कारण संगठन कमजोर हुआ। यह अर्द्धसत्य है। तथ्य यह है कि स्वतंत्रता के बाद बहुत से लेखकों के सपने पूरे हो गये। वे चाहते थे कि देश आजाद हो जाय और स्वतंत्र गणतंत्र बन जाय, किन्तु बहुत से लोग साम्यवाद से नेहरूवाद की ओर चले गये और नेहरू को ही मसीहा मानने लगे। दुनिया के अधिकांश मध्यवर्गीय व्यक्ति यही करते हैं- एक नई राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था के आते ही उसके प्रशंसक हो जाते हैं। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। क्रांतिकारी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन सबसे कठिन है समाज की संरचना को बदलना। इस संरचना के लिए जितना राजनैतिक आन्दोलन महत्त्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा सामाजिक आन्दोलन महत्त्वपूर्ण है।
सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि यहां 19वीं शताब्दी में आर्य समाज तथा सर सैय्यद के आन्दोलन के बाद कोई भी बड़ा सामाजिक आन्दोलन नहीं हुआ। आर्य समाज की एक समय बड़ी प्रगतिशील भूमिका थी। स्त्रियों और अछूतों के संबंध में अपने समय में उसके विचार बहुत प्रगतिशील थे। स्वामी दयानंद ने भारतेन्दु से कहा कि मेरा बस चले तो हिन्दुस्तान के सभी मंदिरों की मूर्तियाँ गंगा में बहा दूं। इस मूर्ति पूजा ने देश को बर्बाद करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। डी.ए.वी. शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर उन्होंने शिक्षा में क्रांतिकारी कार्य किया, किन्तु 1925 के बाद आर्य समाज उसी दलदल में फंस गया जिससे वह समाज के निकालने में लगा था। पाखंड एवं संकीर्णता उनमें भी समा गयी। सर सैय्यद अहमद खाँ का आन्दोलन भी नयी रोशनी फैलाने वाला था। लोगों को अज्ञान के अंधेरे से निकालने का सबसे संगठित प्रयास था। सर सैय्यद की मृत्यु के बाद जिन लोगों ने इस पर कब्जा जमाया उनके पास न तो सर सैय्यद जैसी दूरदर्शिता थी न ही कोई सोच थी। उन लोगों ने यूनीवर्सिटी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। फिर भी अलीगढ़ में एक छोटे से वर्ग ने उनकी गलत नीतियों का खुलकर विरोध किया। इनमें सरदार जाफरी, अख्तर रायपुरी, मजाज, जांनिसार अख्तर तथा इस्मत चुगताई और रशीद जहाँ जैसे प्रमुख रचनाकार थे। आले अहमद शुरूर भी इसमें शामिल थे। प्रमुख बुद्धिजीवियों में मो. हबीब, कारी महमूद, डॉ. ख्वाजा तथा उनके सहयोगी अन्दर से सदैव अनुचित नीतियों का विरोध करते थे। डॉ. जाकिर हुसैन ने तो अलग होकर जामिया मिल्लिया की स्थापना की जो आज एक बड़े विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है।
प्रगतिशील लेखक संघ की सबसे बडी कामयाबी यह थी कि हिंदी-उर्दू तथा पंजाबी तीनों भाषाओं के अदीबों ने धर्म के आधार पर विभाजन का जमकर विरोध किया था। इसे साम्राज्य की चाल बताते हुए एक ला-इलाज रोग बताया। हिन्दू महासभा को मुस्लिम लीग की बहिन बताया। यह ऐतिहासिक कार्य प्रगतिशील लेखकों ने ही किया। अतः आज उनकी उपयोगिता के समुचित मूल्यांकन की जरूरत है।
कांग्रेस में भी प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी दोनों प्रकार की शक्तियां सक्रिय थीं। देश विभाजन ने भी प्रगतिशील आन्दोलन को कमजोर किया। आम हिन्दी का लेखक समझता था कि उर्दू पाकिस्तान की राजभाषा हो गई है। अतः हम हमें उर्दू से क्या मतलब। यह नीति पाकिस्तान के लिए तो सुविधाजन थी लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक माहौल में यह फिट नहीं था। इसी तर्क को आगे बढाते हुए लोगों ने कहा कि उर्दू वहां की राजभाषा कैसे हो सकती है। वहां की राजभाषा सिंधी, पश्तो या कोई अन्य भाषा होनी चाहिए थी, उर्दू नहीं। इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के आंदोलन ने उर्दू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया। यशपाल का ’झूठा सच‘, राही मासूम रजा का ’आधा गाँव‘ तथा भीष्म साहनी का ’तमस‘ इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करते हैं।
भाषा, संस्कृति का बहुत जटिल पहलू है। उसका सम्बन्ध भावना से अधिक है। इसके लिए निरन्तर प्रयास किये जाते रहे कि हिन्दी-उर्दू करीब से करीबतर होती जाय। पहले भी बहुत से प्रयास हुए किन्तु वह असफल रहे। प्रगतिशील लेखक संघ इसी प्रयास में बंट गया। उसमें दो खेमे हो गये- उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ तथा हिन्दी प्रगतिशील लेखक संघ। राही जैसे रचनाकार जो हिन्दी-उर्दू में समान रूप से लिखते थे, उन्होंने कहा कि किधर जाऊँ हिन्दी में, उर्दू में। तभी उन्होंने कहा कि प्रगतिशीलता एक होती है। हिन्दी या उर्दू की अलग-अलग नहीं होती है। वस्तुतः यह दुविधा व्यक्तित्व के टकराहट की थी। इसके पीछे ऐतिहासिक तर्क न था। जब कोई बड़ा आन्दोलन नहीं होता तो लेखकों एवं बुद्धिजीवियों के अहम् टकराने लगते हैं जिससे नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही समस्या आजादी के बाद प्रगतिशील लेखक संघ के दरपेश आई, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रगतिशील लेखक संघ का ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है। भक्ति आन्दोलन के बाद यह दूसरा बडा आन्दोलन है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। एक नई चेतना तथा नये सोच का प्रसार किया। सामाजिक समस्या को बदलने का भी भरसक प्रयास किया तथा उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे। स्त्रियों की समस्या को भी प्रमुखता से रेखांकित किया। उन्होंने दलित एवं स्त्रियों के सम्बन्ध में कोई आदर्श बात न करके व्यवहार में उनकी उन्नति के लिए कार्य किए।
डॉ. रशीद जहाँ, इस्मत चुगताई, कुरर्तुल एन हैदर, हाजरा बेगम जैसी उर्दू की लेखिकाओं ने प्रगतिशील आन्दोलन को अखिलता प्रदान की। हिन्दी में महादेवी वर्मा तथा सुभद्रा कुमारी चौहान भी प्रगतिशील आन्दोलन से मुतास्सिर रहीं। नारी जीवन के संबंध में डॉ. रशीद जहाँ तथा महादेवी वर्मा में काफी समानता है। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में आज भी अनेक नारी रचनाकार हैं जो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं।
हिंदी भाषा पर बातचीत: क्या हिंदी वालों को हिन्दी से प्यार नहीं है?
आज दलित विमर्श की बड़ी चर्चा है और इसमें दलित रचनाकार पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध कम, मार्क्सवाद का विरोध ज्यादा कर रहे हैं। आजादी से पहले दलितों की समस्याओं पर मार्क्सवादी रचनाकारों एवं बुद्धिजीवियों ने व्यवहारिक स्तर पर जो किया उसका भी मूल्यांकन करने तथा लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। देश के मार्क्सवादी आज भी दलितों के साथ सक्रिय भागीदारी कर हाशिये के समाज को भूख-गरीबी तथा अशिक्षा से छुटकारा दिलाने की निरन्तर कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को यह नारा दिया था कि ’उच्च शिक्षा प्राप्त करो तथा संघर्ष करो‘। उन्होंने अस्पृश्यता को ऐतिहासिक कोढ़ बताया। उन्होंने तत्कालीन सवर्ण समाज को चेतावनी दी थी कि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें बदलना होगा तथा दलितों केा उनका हक देना हेागा। लॉ कालेज (औरंगाबाद) देश की अग्रणी कालेजों में से है। इसकी स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये संस्थाएं दलितों के लिए अवश्य हैं किन्तु यहां योग्य गैर दलितों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने श्रेष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति पर बहुत जोर दिया था। उनका विचार था कि अध्यापक कई पीढि़यों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है अतः अध्यापक अच्छे होने चाहिए। इन शिक्षा संस्थाओं में गैर दलित शिक्षकों की संख्या अब भी अधिक है।
इसी प्रकार आज नारी विमर्श पर बहुत बहस हो रही है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण नारी को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता देने का पक्षधर है। समानता के सिद्धांत को व्यवहार में भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसके बरअक्स इस दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था का नारी चिंतन है जिसमें नारी को मनचाहे वस्त्रों को पहनने तथा क्लब जाने की पूरी छूट दी है। उनके अनुसार शरीर उनका है जैसा चाहे वैसा प्रयोग करें। इस व्यवस्था के चिंतकों ने नारी को शो-पीस बना दिया है। नारी को विक्रय की वस्तु बना दिया है। हमारे बहुत से लेखक जाने-अनजाने में इसी पतनशील व्यापारिक विचारों के समर्थक हो गये हैं। प्रगतिशील आन्दोलन ने इन दोनों मूल्यों की तुलना की है। यशपाल तथा रांगेय राघव जैसे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें ऐतिहासिक दृष्टि दी है।
किसी भी भाषा का साहित्य नये विचारों एवं नयी समस्याओं से झूझकर ही सच्चा साहित्य बनता है। जिस लेखक के पात्र जितने अधिक चेतनासंपन्न होकर संघर्ष करेंगे उतना ही वे सफल होंगे। प्रगतिशील लेखकों ने कहा कि व्यक्ति जब संघर्ष करता है तो स्वयं को परिस्थितियों को तथा समाज का बदलता है। इससे एक यथार्थवादी परम्परा का जन्म होता है। यथार्थवाद ही किसी साहित्य को महत्त्वपूर्ण बनाता है। रोमानी क्रांतिकारिता साहित्य के लिए एक सीमा के बाद बाधक बन जाती है। एक समय था जब प्रगतिशील साहित्य को हाशिये पर रख दिया गया। धीरे-धीरे रोमानी क्रांतिकारिता का कोहरा छटा तो यह बात समझ में आ गई कि यथार्थवादी साहित्य की स्थायी होता है। हिन्दी-उर्दू में अनेक नये लोग उभर कर आते तो हैं किन्तु दो-तीन अच्छी रचनाओं को लिखने के बाद पूँजीपतियों के आगोश में चले जाते हैं या फिर अराजकता के आकाश में विचरण करने लगते हैं। वस्तुतः जन आन्दोलन से जब तक यह लेखक नहीं जुड़ेंगे और प्रगतिशीलता की बात करेंगे तो यह अर्न्तविरोध बड़ा रचनाकार बनने से रोकेगा। कोई पत्रिका या बडा पत्रकार किसी लेखक को महान नहीं बना सकता। बाजार में बिकाऊ जरूर बना सकता है।
जनता सड़कों पर है, लेखक दड़बों में!
समय के साथ प्रगतिशील लेखक संघ बिखरता चला गया। आज वामपंथियों के तीन संगठन हैं-जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ तथा जन संस्कृति मंच। संगठन के रूप में इन तीनों की स्थिति अच्छी नहीं है। बाजारवादी व्यवस्था ने तीनों को अकेला कर दिया है। मार्क्सवाद सामूहिकता पर बहुत बल देता है। लेखक संगठनों की यही ऐतिहासिक सीमा है। मार्क्सवाद आत्मालोचना के सिद्धांत का हामी है किन्तु ये संगठन आत्मालोचना से उसी तरह डरते हैं जैसे कि साधारण रचनाकार डरते हैं। प्रो. अब्दुल अलीम, जिनका संबंध प्रगतिशील लेखक संघ के पुरोधाओं से है, उन्होंने लेखकों की एक बड़ी मीटिंग में कहा था कि लेखक संगठन बनाना उतना ही कठिन है जितना कि हिरन पर घास लादना, लेकिन हिरन पर घास लादने का कार्य प्रगतिशील लेखक संघ के उत्तराधिकारियों का काम है। इसे कोई दूसरा नहीं कर सकता है।