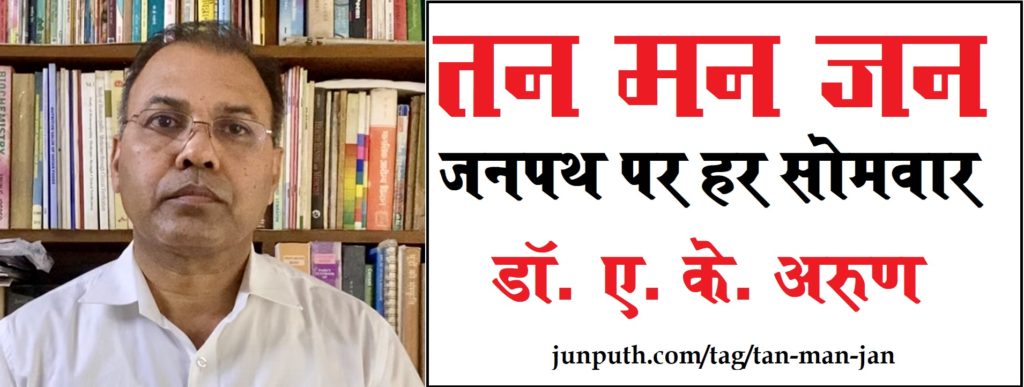कोरोना वायरस संक्रमण की विभीषिका ने भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। आजादी के पहले से देश में जिस बुनियादी जनस्वास्थ्य ढांचे की संकल्पना थी, वह आज 75 वर्ष बाद भी खड़ा नहीं हो पाया है। बारी-बारी से सत्ता पर काबिज सभी मुख्य राजनीतिक दलों में लगभग एक जैसी सोच ही है। जनस्वास्थ्य कभी इन दलों की चिंता का विषय नहीं रहा।
स्वास्थ्य के नाम पर विगत तीन दशकों से निजीकरण को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। वैश्वीकरण के नाम पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया। पांच सितारा अस्पतालों की लाइन लगने लगी और सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के कमजोर हो जाने का परिणाम यह हुआ कि जनस्वास्थ्य की स्थिति खस्ता होती चली गई और आम गरीब लोगों के बीमार होने का सिलसिला बढ़ता गया। फ्लू, दस्त, मलेरिया, टी.बी., एनिमिया, कैंसर, कुपोषण से होने वाले रोग, टिटनेस आदि ने रोगों की जटिलता को बढ़ा दिया और देश में स्वास्थ्य की नई-नई चुनौतियां बढ़ने लगीं। टीकाकरण व महामारियों की रोकथाम की जिम्मेवारी अल्प प्रशिक्षित पैरामेडिकल कार्यकर्ताओं के जिम्मे छोड़कर सभी उच्च प्रशिक्षित चिकित्सक शहर के बड़े अस्पताल या कारपोरेट अस्पताल के विशेषज्ञ के रूप में चिकित्सा कर रहे हैं। ऐसे में महामारियों का बेकाबू होना कोई बड़ी बात नहीं है।
भारत में महामारियों की त्रासदी का सिलसिला कोई नया नहीं है। सन् 1915 से 1926 तक देश में इंसेफेलाइटिस लेटार्मिका नामक संक्रामक महामारी ने कहर बरपाया था। इसमें मनुष्य का मस्तिष्क व उसका केन्द्रीय तंत्र वायरस के मुख्य निशाने पर था। यह संक्रमण भी नाक और मुंह के स्राव से फैलता है। भारत और योरोप ने इस महामारी को झेला था। सन् 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू का कहर था। एवियन एन्फ्लूएन्जा के घातक स्ट्रेन की वजह से उत्पन्न यह महामारी भारत में 1 करोड़ 30 लाख लोगों की मौत का कारण बनी थी। तब दुनिया में 8 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। सन् 1962 से 1975 तक विब्रियो कालरा दुनिया के लिये महामारी था। बंगाल में इस कालरा (हैजा) ने विकराल रूप धरा था। यह दूषित पानी की वजह से फैला था। सन् 1969 में फ्लू, एन्फ्लूएन्जा वायरस के एच3एच2 स्ट्रेन से हांगकांग में फैला और महज दो महीने में ही भारत आ गया। सन् 1974 में चेचक ने भारत में कहर बरपाया था। इसके दो वैरिएन्ट वैरियोला मेजर या माइनर ने काफी तबाही बचाई थी। विश्व में फैले इस महामारी के 60 फीसद मामले भारत में थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से तीन साल तक चले चेचक उन्मूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनएसईपी) की मदद से सन् 1977 में भारत में चेचक मुक्त हुआ था। 1994 में सूरत में फैला जानलेवा प्लेग, सन् 2002-2004 में सार्स, सन् 2006 में डेंगू, सन् 2009 में गुजरात हेपेटाइटिस, सन् 2015 में स्वाइन फ्लू, सन् 2018 में मिपा वायरल प्रकोप देश की जनस्वास्थ्य व्यवस्था पर चुनौती के रूप में रहे हैं।
हम महामारियों के दौर में जी रहे हैं। मानव जीवन में सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ आधुनिकता और उसकी वजह से उत्पन्न परिस्थितियों ने भी कई बीमारियों और महामारियों को सक्रिय कर दिया है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं आत्मप्रशंसा के थोथे नारों पर देश की सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को इनकार कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो खोखली घोषणा की थी उसका परिणाम यह हुआ कि कई मामलों में भारत की स्थिति कई बार दयनीय रही। देश ने सन् 1991 में उत्तरकाशी भूकम्प, 1997 में लातूर भूकम्प, 2001 में गुजरात भूकम्प, 2002 में बंगाल चक्रवात, सन् 2004 में बिहार में बाढ़ के समय विदेशी सहायता स्वीकार की थी लेकिन विगत कई वर्षों से भारत सरकार ने अपनी राजनीति बदल दी और विदेशी सहायता नहीं लेने का तय किया था। सन् 2013 में हुए केदारनाथ धाम त्रासदी, 2014 में कश्मीर बाढ़, फिर 2018 में केरल की भयावह बाढ़ के समय केन्द्र सरकार ने विदेशी मदद दोबारा ली थी मगर कोरोना संक्रमण के संकट में भारत ने विदेशी मदद को स्वीकार करने का फैसला लिया है। इस समय अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, आयरलैन्ड, बेल्जियम, रोमानिया, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, भूटान, सउदी अरब, थाईलैन्ड, फिनलैन्ड, नार्वे, इटली, बंगलादेश, यूएई आदि कोई 20 देश भारत की मदद कर रहे हैं।
अब सवाल है कि वैश्विक आपदा या महामारी के इतने तीव्र दंश झेलने के बावजूद भारत में जनस्वास्थ्य को लेकर इतनी उदासीनता क्यों है। विगत कई दशकों से प्राकृतिक आपदा और महामारियों का वैश्विक कहर झेलने वाले भारत में राजनीतिक दलों की अपरिपक्वता और उनमें दूरदर्शिता का अभाव तथा थोथे अहंकार के कारण लोगों के वाजिब सवाल और जनस्वास्थ्य जैसे मसले कभी प्राथमिकता सूची में जगह नहीं ले पाए। आपदा राहत की लुटेरी व्यवस्था यहां के राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों को ज्यादा रूचती है क्योंकि इसमें ‘‘आपदा में अवसर’’ का अप्रतिम आनन्द और सीधे लाभ की श्रेयस्कारी सुविधा है। वास्तविक आपदा एवं महामारी प्रबन्धन के नाम पर यहां थोथी जुमलेबाजी के अलावे और कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर महज बजट में हर साल चन्द रूपये बढ़ाकर सरकारें वाहवाही लूटती रहती हैं मगर जमीन पर कुछ खास नहीं दिखता। कोरोना महामारी ने उस बढ़े स्वास्थ्य बजट की भी पोल खोल कर रख दी है।
कोरोना महामारी ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को नंगा करके रख दिया है। कई मामलों में तो केन्द्र और राज्य सरकार में टकराव साफ देखे गए हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची के अनुसार जनस्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल और औषधि राज्यों के अधिकार में आते हैं लेकिन कोरोनाकाल में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव शुरू से देखे जा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में तो मोदी सरकार की केन्द्रित नीति का असर साफ दिखा है जिसका दुष्परिणाम कोरोना विस्फोट के रूप में सामने आ चुका है। केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय स्तर पर शौचालय निर्माण, पेयजल मिशन आदि कार्यक्रम ज्यादातर केन्द्र द्वारा संचालित एवं नियंत्रित रहे। मसलन जमीन पर यह योजना उस तरह नहीं दिखी जिस तरह से यह कागजों पर और विज्ञापनों में। यह विडम्बना ही है कि कार्यों का ढोल पीटने के बजाय मोदी सरकार ने अपनी प्रशंसा के कसीदे ज्यादा कढ़वाए जिसे गोदी मीडिया ने बड़े जोर-शोर से प्रचारित किया। कुल मिलाकर यह मोदी जी के छवि निर्माण व उसे बनाए रखने का हथकन्डा ही साबित हुआ।
जन स्वास्थ्य की उपेक्षा की कीमत यह देश और यहां की नादान जनता अकसर चुकाती रही है। आपदाओं और महामारियों से गुजरते हमें सैकड़ों वर्ष हो गए लेकिन हमने इससे न तो कोई सबक लिया और न ही अपने भविष्य की सुरक्षा पर सोचा। सन् 1991 की उत्तरकाशी भूकम्प त्रासदी में मैं करीब एक महीना उत्तरकाशी के चमोली, सिलियारा एवं बूढ़ाकेदार में स्वतंत्र रूप से आपदा राहत में सक्रिय था। भूकम्प के एक महीना बाद तक भी सरकार की राहत वहां के सर्वाधिक प्रभावित गांवों में नहीं पहुंची थी। मेरा निजी अनुभव है कि महीना भर पहले लगे जख्मों पर न तो कोई मलहम न ही कोई पट्टी थी क्योंकि उनके पास प्राथमिक उपचार के साधन तो थे ही नहीं और सरकार भी वहां तक नहीं पहुंची थी। ऐसे ही प्लेग संक्रमण के अफवाह और यथार्थ के द्वंद्व में गुजरात का सुन्दर शहर सूरत बेरौनक हो गया था। बात सन् 1994 की है। तब शहर पूरी तरह खाली हो गया था। लोग अपने ही रिश्तेदारों को घर में पनाह नहीं दे रहे थे। सूरत के प्लेग ने महामारी में संवेदनहीनता को जगजाहिर कर दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि तब नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ कम्यूनिकेबल डिजीजेज के निदेशक डॉ. रहमान की लोगों ने इसलिए हत्या कर दी थी कि रोग नियंत्रण के प्रयासों में वे खुद संक्रमित हो गये थे। ऐसे ही सन् 2001 के भूकम्प में गुजरात बुरी तरह प्रभावित था और लोग बड़ी संख्या में घायल हुए थे। तब भी मैं अपने मित्रों के साथ लगभग एक महीना कच्छ और सौराष्ट्र के कोई 50 से ज्यादा गांवों में अपने संसाधनों से राहत कार्य में लगा था। वहां भी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त थी। जो भी था केवल कागजों पर। स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो मदद की उससे ही लगभग 75 फीसद राहत व बचाव कार्य हुआ।
संक्रमण काल: महामारी के दौर में डॉक्टरों की भूमिका, सीमाएं और प्रोटोकॉल के कुछ सवाल
प्रधानमंत्री मोदी ने ही कहा है कि ‘‘आपदाएं’’ ‘अवसर’’ होती हैं। और इस अवसर का लाभ सरकार, सरकारी बाबू और बड़ी कम्पनियां उठा रही हैं। वर्तमान कोरोना महामारी में ही देख लें। लॉकडाउन में जनता बेहाल लुटती-पिटती रही और सरकारी बाबू, ठेकेदार, कारपोरेट मालदार बनते रहे। आपदा में अवसर का प्रत्येक उदाहरण देश ने कोरोनाकाल में देखा। आज देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर झेल रहा है। पहली लहर में ज्यादातर बुजुर्गों ने अपनी जान गंवाई मगर इस लहर में तो 15 से 45 वर्ष के युवाओं की जान जा रही है। बीते एक हफ्ते में मैं अपने जानने वाले आठ युवाओं की कोरोना संक्रमण से हुई मौत का गवाह बना हूं। इन सबकी उम्र 20 से 45 वर्ष के बीच थी। निजी अस्पतालों और चिकित्सकों की कमाई हजार गुना बढ़ गई है। यहां मैं निःस्वार्थ सेवा में समर्पित चिकित्सकों की बात नहीं कर रहा लेकिन ज्यादातर लोग और अस्पताल मरीजों से लूटने में लगे हैं। मैंने कुछ जरूरतमन्द मरीजों को 40 हजार से 50 हजार रुपये में कोरोना संक्रमण की कथित दवा काले बाजार से खरीदते पाया है। बहरहाल, सरकार और प्रशासन की निष्क्रियता, नकारापन से स्थिति और विस्फोटक बनती गई। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की सबसे ज्यादा कीमत गरीब मेहनतकशों ने चुकाई। यदि देश की प्राथमिक व जनस्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था दुरूस्त होती और प्रशासन ईमानदार होता तो अफरातफरी और बदहाली का यह आलम नहीं होता। मोदी सरकार और प्रदेशों की सरकारों ने देश की जनता को उसके हाल पर ही छोड़ दिया।
आजादी के सत्तर साल बाद भी यदि देश अपने नागरिकों को मुसीबत में मदद नहीं पहुंचा सकता तो राजनीति और प्रशासन में जोंक की तरह चिपके नेताओं और बाबुओं से जनता की नफरत लाजिमी है। दरअसल, राजनीति में जनता को गुमराह कर दलाल और अपराधी नेताओं की सक्रियता ने देश में धर्म, जाति, वर्ग के नाम पर जो अफीम बोया है उसी का परिणाम है कि हम सब कुछ समझकर भी इनको झेल रहे हैं। इसी कोरोनाकाल में शीर्ष नेताओं की मूर्खता का प्रदर्शन भी हमने देखा। अन्धविश्वास के पैरोकार ज्ञान और विज्ञान से अकसर दूर भागते हैं। वे अपनी जनता को कूपमन्डूक व मूर्ख बनाए रखकर अपनी राजनीति चलाते हैं। सन् 2020 की पहली कोरोना लहर में भारत सरकार के खजाने को लुटाकर भी ये नेता देश को इस वैश्विक आपदा में भरोसा नहीं दिला पाए। इस दौरान हमारे देश ने वर्षों में अर्जित अपनी साख भी खोई है। देश के अन्दर और देश से बाहर देश की ऐसी फजीहत पहले कभी नहीं हुई। हाल के चुनावों में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों के भाषणों का मजमून पढ़ लें तो सर धुन लेंगे। ऐसी अमानवीय एवं अश्लील बातें करते ये नेता कभी सम्माननीय लग ही नहीं सकते।
जिस देश में लोगों के जीवन बचाने के लिए आक्सीजन और दवाओं की अपेक्षा महंगे भवन का निर्माण, उड़ने के लिए महंगे जहाज और शेखी बघारने के लिए गगनचुम्बी मूर्तियां प्राथमिकता हों वहां बुनियादी प्राथमिक एवं आपदा चिकित्सा राहत केन्द्रों के इन्तजाम की बात करना बेमानी है। जिन नेताओं का दिल गंगा में बहती देशवासियों की लाशों को देखकर भी नहीं पिघले उसे मानव कहना भी उचित नहीं है। जहां अपने देश के बदहाल लोगों के लिए किये जा रहे सरकारी इन्तजाम में लूट, कालाबाजारी एवं स्तरहीन पदार्थों की सप्लाई पर कोई अफसोस या उसके खिलाफ रोष न हो तो उसे क्या कहेंगे? जनता की गाढ़ी कमाई पर अय्याशी करने वाले नेताओं की बर्बरता को यदि यहां का मीडिया (गोदी मीडिया) ‘‘दरियादिली’’ लिखे/बोले तो फिर हम क्या उम्मीद करें। एक व्यक्ति जो कारपोरेट के मुनाफे की गारंटी हो, देश का सबसे मजबूत निर्णयकर्ता हो और उसे देश में बहुमत का घमण्ड हो तो जनहित में लिखकर, सोचकर, बोलकर या सक्रिय होकर भी आप क्या उखाड़ लेंगे? हालात बेहद नाजुक हैं फिर भी नक्कारखाने में तूती की तरह ही सही बोलते रहिए। यही समय की मांग है। जुबान है तो बोलिए। गूंगे मत रहिए। आवाज असर करती है, उम्मीद है करेगी भी।
फिर होना क्या चाहिये? सीधे तौर पर देश में गांव स्तर पर जनस्वास्थ्य व्यवस्था को कार्य और प्रबन्धन के स्तर पर न केवल मजबूत बल्कि आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की जरूरत है। गांव गणराज्य की कल्पना भारत के पूर्व आइएस एवं सिद्धान्तकार डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा ने स्पष्ट रूप से ढाई दशक पहले ही दी थी जिसे सरकारों ने कूड़े में डाल दिया। यदि जनस्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्धन और कार्यान्वयन गांव या प्रखण्ड के स्तर पर हो तो देश में कभी भी ऐसी मारामारी और हाहाकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आज की महज सरकारी खानापूर्ति एवं वेतनलूट के अड्डे बने हुए हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों के सरकारी संसाधनों की लूट का चस्का अब गांव पंचायत तक पहुंच चुका है। पंचायत चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च कर चुनाव जीतने की इच्छा के पीछे का सच ‘‘लूट’’ नहीं तो और क्या है? इस लूट को रोके बगैर देश में महामारियों, आपदाओं से मानवीय तरीके से निबटना सम्भव नहीं है।
झारखंड: PESA कानून के तहत स्वशासन की आदिवासी परंपरा को पुनर्जीवित करने का मौका
स्कूलों में भौंडे नेताओं की नकली जीवनी पढ़ाने के बजाय प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबन्धन, व्यावहारिक शिक्षा, नैतिक आचरण, सेवा, सहयोग का ज्ञान को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए; स्वास्थ्य और शिक्षा को निजीकरण से मुक्त कर आवश्यक जनसेवा घोषित किया जाए; कारपोरेट व पूंजीपतियों को मनमाने तरीके से मेडिकल व तकनीकी शिक्षा में धन्धे की अनुमति नहीं हो; अस्पतालों को मुनाफे के गणित से मुक्त रखने की नीति बने; प्राथमिक उपचार, आकस्मिक उपचार, आपदा, टीकाकरण, दवा आदि व्यवस्था देश में नागरिकों से मुफ्त मिले; जीवनरक्षक दवाओं, टीका आदि बौद्धिक सम्पदा कानून के दायरे से बाहर हों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के बुनियादी संचालन में राज्य, प्रखण्ड, गांव को प्राथमिकता हो; विकेन्द्रित व्यवस्था में राज्य व केन्द्र केवल सहयोगी बनें। सम्भवतः लाल फीताशाही से मुक्ति के बाद हम लोगों की जान बचा पाएंगे वर्ना किसी नेता की इमेज बनाने-बनाते पूरा देश ही कहीं श्मशान में तब्दील न हो जाए।