अभिषेक श्रीवास्तव
किन्हीं दो व्यक्तियों के जीवन की तुलना अगर नहीं की जा सकती, तो उसी तर्ज पर उन दो व्यक्तियों के जीवन पर बनी फिल्मों की तुलना भी नहीं की जानी चाहिए। यह आदर्श स्थिति है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ”भाग मिल्खा भाग” देखने जाते हैं तो आपके पास ”पान सिंह तोमर” का बेंचमार्क पहले से मौजूद होता है, लिहाज़ा तुलनाओं को रोकना मुश्किल है। इससे इतर हालांकि किसी खिलाड़ी के जीवन पर फिल्म बनाने की कला पर बात करना कहीं ज्यादा आसान और जस्टिफाइड है, इसलिए ”भाग मिल्खा भाग” को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक सामान्य दर्शक की नज़र से देखने पर जो सवाल उठते हैं उन पर बात करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिल्म अच्छी है, बुरी है, कैसी है, इस पर कोई फैसला देना अलग बात है लेकिन सबसे पहले जो सहज सवाल उठते हैं उन्हें क्रम से दर्ज कर लेना ज़रूरी है:
1) मिल्खा सिंह एक छिटपुट छुरीबाज़ से फौजी कैसे बने?
2) इंडिया का कोट मिलने के बाद ही, यानी पहली जीत हासिल करने के बाद ही मिल्खा को अपने घर जाने/अपनी प्रेमिका का हाल लेने का वक्त क्यों मिला?
3) भारतीय फौज पर बनी फिल्मों या कहें भारतीय फौजियों के जीवन की लाइफलाइन कही जाने वाली चिट्ठी मिल्खा के जीवन से क्यों गायब रही? क्या मिल्खा को लिखना नहीं आता था या उनकी प्रेमिका को?
4) मिल्खा के जीजा का स्वभाव मिल्खा के प्रति नरम कैसे हुआ?
5) मिल्खा को दौड़ते वक्त पीछे मुड़ते ही जो घोड़ा दिखाई देता था और बाद में उस घोड़े पर काले कपड़ों में जिन लोगों को दिखाया गया, वे कौन थे?
6) मिल्खा के नाम पर जो छुट्टी घोषित की गई, वह उनकी प्रेमिका से किया गया एक वादा था। यहां प्रेमिका का संदर्भ या उसकी जीवन स्थिति को दिखाना ज़रूरी क्यों नहीं था?
7) तीन घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म में मिल्खा के बचपन के दोस्त समप्रीत को मौलवी द्वारा बचा लिए जाने का कोई दृश्य क्यों नहीं डाला गया और इस बात को पासिंग कमेंट की तरह क्यों उड़ा दिया गया?
8) मिल्खा की सबसे बड़ी जीत 400 मीटर में विश्व रिकॉर्ड की थी जिसके बारे में उन्होंने परची पर लिख कर सहेज कर रखा था। इसका विवरण देने के बजाय भारत-पाकिस्तान मैत्री खेल को प्रमुखता क्यों दी गई?
9) मिल्खा के पाकिस्तान पहुंचने पर हवा में से गिरते परचे दिखाना क्यों ज़रूरी था (खालिक बनाम मिल्खा) जबकि मिल्खा ने अपने इंटरव्यू में इस संदर्भ में अखबारों और बैनरों का जि़क्र किया है?
10) मिल्खा ने इंटरव्यू में वाघा सीमा चौकी से पाकिस्तान में जाने का जि़क्र किया है (जो तब तक बनी नहीं थी), जबकि फिल्म हुसैनीवाला चेकपोस्ट को दिखाती है जो 1970 में बंद हो गया?
11) पतली आवाज़ में बोलने वाले रंगरूट सुरेश कुमार को पूर्वोत्तर के चेहरे-मोहरे वाला दिखाए जाने और उसे प्रकाश राज द्वारा सुरेश कुमारी के नाम से नवाज़े जाने के पीछे कौन सी मानसिकता है?
 |
| देह बनाने से फिल्म नहीं बनती: नकली और असली मिल्खा |
ये सवाल कुछ तो तथ्यात्मक हैं और कुछ जिज्ञासा से उपजे हैं। इन सवालों को हम कैसे बरतें? अगर वास्तव में फिल्म उनके जीवन की घटनाओं पर ही बनी है, तो शक होता है। अगर इसमें नाटकीयता को जबरन डाला गया है, तो यह निर्देशक की बेईमानी है। जिस तरह एक कवि का आत्मकथ्य उसकी कविता होती है, उसी तरह एक खिलाड़ी का आत्मकथ्य उसका खेल होना चाहिए। एक खिलाडी के आत्मकथ्य की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके खेल की सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। यही बात इस फिल्म से नदारद है। मिल्खा जब टिशू पेपर पर लिखे विश्व रिकॉर्ड के समय को आग में झोंक देते हैं, तब जाकर समझ में आता है कि उन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्क्रीन पर आठ विंडो बनाकर इस मामले को जल्दी में निपटा देना और इसके बरक्स पाकिस्तान के साथ मैत्री दौड़ को प्रमुखता देकर फिल्म में लोकप्रिय अंधराष्ट्रवाद की छौंक लगाना किसकी गलती मानी जाएगी? अगर मिल्खा सिंह खुद इस फिल्म के साथ लगातार जुड़े रहे, तो उन्हें आखिर इस पर आपत्ति क्यों नहीं हुई? इसे समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में उनका साक्षात्कार पढ़े जिसमें कूमि कपूर ने उनसे ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की के साथ एक रात के प्रेम वाले संदर्भ में सवाल पूछा है। उन्होंने बड़े कूटनीतिक अंदाज़ में कहा है कि निर्देशक का मानना था कि इससे दर्शक फिल्म को पसंद करेंगे।
इसके ठीक उलट आप शिमित अमीन की निर्देशित ”चक दे इंडिया” को याद करें। राष्ट्रप्रेम वहां भी था, लेकिन वह मैत्री के नाम पर किसी से विद्वेष की कीमत पर नहीं आता है। अगर वहां राष्ट्रवाद और विभाजन के बाद पैदा सांप्रदायिकता का एक ”विक्टिमाइज्ड” कबीर खान है तो यहां भी विभाजन का ”विक्टिमाइज्ड” मिल्खा है। कबीर खान की उपलब्धि से मिल्खा की उपलब्धि को मिलाकर देखें, निर्देशक की बेईमानी साफ दिख जाएगी। मिल्खा सिंह इस ”पिक एंड चूज़” के आख्यान से पूरी तरह गायब हैं। अगर तथ्यों के उलटफेर में उनकी मौन सहमति है, तो इसे हम क्या समझें? संभव है निर्देशक का दबाव, या संभव है खुद उनका हिंदू राष्ट्रवाद?
बहरहाल, महिलाओं पर आते हैं। जिस प्रेम को याद कर के मिल्खा चुन्नी उड़ाते शहादरा के पुल पर पाए जाते हैं, उसे अचानक भूल कर अगले क्षण बीयर पीते हुए ऑस्ट्रेलियाई लड़की के साथ भी पाए जाते हैं। पता नहीं 1960 में ऐसा होता था या नहीं, हालांकि उन्होंने खुद दर्शकों में लोकप्रियता के नाम पर इसे निर्देशक का दबाव बताया तो है ही। फिर अचानक उन्हें ज्ञान होता है कि ऑस्ट्रेलियाई लड़की के कारण ही उनका प्रदर्शन खराब रहा है और वह अगले ही पल एक ”जलपरी” के प्रस्ताव पर उससे माफी मांगते दिखते हैं। क्या राकेश ओमप्रकाश मेहरा इन दो महिला पात्रों को सनातन भारतीय आख्यानों के हिसाब से ”नर्क का द्वार” मानते हैं जो विश्वामित्र की तपस्या भंग करने वाली अप्सरा से ज्यादा कोई मायने नहीं रखती हैं? क्या जिस लड़की से मिल्खा ने प्रेम किया था, उसकी जीवन स्थितियों को तीन घंटे में एक बार भी दिखाना वे ज़रूरी नहीं समझते? पता नहीं मिल्खा सिंह ने उसके बारे में कभी पता किया या नहीं, लेकिन वे खुद एक बात अपने साक्षात्कार में ज़रूर कहते हैं कि इन दृश्यों को दिखाने का मतलब यह संदेश देना था कि महिलाएं आपको अर्श से लेकर फर्श पर कहीं भी पहुंचा सकती हैं। बहरहाल…
 |
| फिल्म की इकलौती जान दिव्या दत्ता |
मिल्खा सिंह को पालने वाली उनकी एक बड़ी बहन है। दिव्या दत्ता अगर इस फिल्म में नहीं होतीं तो शायद भावबोध की जो न्यूनतम संभावना भी फिल्म में बची है, वह खत्म हो जाती। यह दिव्या के अभिनय का कमाल है। उनसे शायद ऐसा ”सबजुगेटेड” रोल करने को ही कहा गया रहा होगा और उन्होंने पूरा न्याय किया है। सवाल फिर निर्देशक पर है कि जब इतनी नाटकीयता उसे भरनी ही थी, तो उसने अपने ”सबजुगेशन” को पूरी तरह स्वीकार कर के खुश रह जाने वाली महिला का चरित्र क्यों गढ़ा? एक ओर ऐसी तीन महिलाएं जो पुरुष को फर्श पर गिरा रही हैं और दूसरी ओर ऐसी महिला जो खुद फुट भर धंसे रह कर पुरुष को झाड़ पर पर चढ़ाने का काम कर रही है? पचास के दशक में परिवारों के भीतर इतना तो मूल्यबोध रहा ही होगा कि बेटिकट यात्रा करने पर अपने लड़के की ज़मानत घर के बड़े-बूढ़े भले ही करवा लें, लेकिन बाद में उसे झाड़ते तो ज़रूर रहे होंगे। या, पता नहीं। आखिर क्या ज़रूरत थी कि शरणार्थी शिविर के भीतर मिल्खा की बहन और उसके पति के बीच अंतरंग कर्म को ध्वनि के माध्यम से ही सही, दिखाया गया? इससे मिल्खा के भीतर पैदा गुस्से को अगर दिखाने का उद्देश्य था, तो वह गुस्सा गया कहां? मैं जिस हॉल में यह फिल्म देख रहा था, वहां मेरे पड़ोस में बैठा एक बच्चा अपने पिता से लगातार पूछ रहा था कि पापा-पापा, यह आवाज़ कैसी है। पिता के मुंह से बदले में कोई आवाज़ ही नहीं निकली।
विभाजन कोई ऐसा आख्यान नहीं है जिसे रहस्य के आवरण में लपेट कर पेश किया जाय। बावजूद इसके राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने इस फिल्म में ऐसा ही किया है। शुरू से घोड़े और तलवार की तस्वीर देखकर बार-बार सत्तर के दशक की किसी फिल्म के पात्र की याद आती है जिसके पिता को डकैतों/माफियाओं ने अंधियारी रात उसके बचपन में मार गिराया था और वह सिर्फ उस माफिया को मार डालने के लिए बड़ा हुआ है। विभाजन के वक्त जो दंगे हुए, उनमें आम लोगों के बीच मारकाट हुई थी। सिख परिवार का डिफेंस पर होना और हत्यारों का काले नकाब पहनकर घोड़े पर आना- यह एक ऐसा कंट्रास्ट रचता है जहां विभाजन का स्वाभाविक दृश्य एक फिल्मी फिक्शन में बदल जाता है और आम लोगों के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को पावर डिसकोर्स में तब्दील कर दिया जाता है। बिल्कुल यही काम हवाई जहाज़ से परचे गिरवाकर मेहरा करते हैं। क्या कोई मानेगा कि पाकिस्तान की सरकार ने ऐसे परचे गिरवाए रहे होंगे? अगर नहीं, तो उस वक्त हवाई जहाज़ सरकार के अलावा और किसके पास था भाई? मिल्खा साक्षात्कार में कहते हैं कि लाहौर की सड़कों पर ”खालिक बनाम मिल्खा” के बैनर लगे थे और अखबारों में भी यही लिखा था। हवा से परचे गिराने में और मिल्खा सिंह की बात में ज़मीन-आसमान का अंतर है।
हुसैनीवाला चेकपोस्ट दिखाकर फिल्म ने तथ्यात्मक रूप से सही काम किया है, लेकिन मिल्खा सिंह ने अपने साक्षात्कार में वाघा सीमा का नाम लिया है। यहां मामला उलटा हो जाता है। हुसैनीवाला बॉर्डर पोस्ट 1970 में बंद हो गया था और वाघा सीमा इसके बाद कुछ दूरी पर उत्तर में खोली गई थी। लगता है मिल्खा सिंह ने साक्षात्कार में भी वैसा ही घालमेल किया है जैसा फिल्मकार को अपनी कहानी बताने में।
 |
| मिल्खा की आत्मकथा |
मिल्खा सिंह के इधर बीच आए साक्षात्कारों और खबरों को पढ़ें तो एक बात जो साफ होती है वो यह कि इस फिल्म के बनने को लेकर मिल्खा सिंह काफी उत्साहित और मुग्ध थे। ठीक वैसे ही इस फिल्म को बनाने के लिए राकेश ओमप्रकाश मेहरा भी उतने ही जोश में थे क्योंकि एक रुपया में हीरोइन और आत्मकथा दोनों मिल जाना किसी के लिए भी अच्छी डील है। बस गलती यह हो गई कि प्रसून जोशी ने मिल्खा सिंह पर अपने तईं ठीक से रिसर्च नहीं किया। लगता है या तो उन्होंने पूरी तरह मिल्खा सिंह की किताब को उतार दिया या फिर अतिरिक्त जानकारी के लिए मिल्खा सिंह से ही बात की। किसी ने कहा है कि आत्मकथाएं ईमानदार तो हो सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि सौ फीसदी सच्ची हों। ये ठीक है कि एक बायोपिक फिल्म बनाने में नाटकीयता के तत्व लाए जा सकते हैं, लेकिन एक जिंदा शख्स की कहानी को बेईमान बना देना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जैसा कि मैंने शुरू में कहा, किन्हीं दो व्यक्तियों के जीवन की तुलना अगर नहीं की जा सकती, तो उसी तर्ज पर उन दो व्यक्तियों के जीवन पर बनी फिल्मों की तुलना भी नहीं की जानी चाहिए। मैं ”पान सिंह तोमर” से ”भाग मिल्खा भाग” की तुलना कतई नहीं करूंगा। और ”चक दे इंडिया” से तो और भी नहीं क्योंकि (अकथित तौर पर मीर रंजन नेगी की कहानी पर बनी) यह फिक्शन तमाम मामलों कहीं ज्यादा स्वस्थ, राष्ट्रीय व खेल भावना से परिपूर्ण और पॉजिटिव है, चूंकि यहां कहानी किसी व्यक्ति पर नहीं लिखी गई थी और निर्देशक को अंधराष्ट्रवादी गंध मचाने की पूरी छूट थी फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। एक फिक्शन लिखने में बरती गई ईमानदारी और एक बायोपिक लिखने में बरती गई बेईमानी- यह फर्क है ”चक दे इंडिया” और ”भाग मिल्खा भाग” में। चूंकि मिल्खा देखने वाले बार-बार ”पान सिंह तोमर” को याद कर रहे हैं, इसलिए एक जि़ंदा शख्स के प्रति पूरे सम्मान के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों फिल्मों के बीच वही फर्क है जो दोनों व्यक्तियों के बीच है।
 |
| पान सिंह तोमर |
अब दोनों व्यक्तियों के बीच का फर्क समझना हो तो ध्यान करें कि मिल्खा सिंह ने अपने तमाम साक्षात्कारों में इधर बीच कहा है कि हर व्यक्ति के भीतर एक मिल्खा सिंह होता है और इस फिल्म से होने वाली कमाई को वे खिलाडि़यों के प्रशिक्षण वाले अपने फाउंडेशन में लगाना चाहेंगे जबकि एक तथ्य यह भी निकल कर आया है कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध गोल्फर बेटे जीव मिल्खा सिंह को खुद दौड़ने से रोका और गोल्फ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। दूसरा तथ्य यह है कि उन्होंने अर्जुन पुरस्कार भी यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि अयोग्य लोगों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके उलट पान सिंह तोमर ने तो अपने बेटों को भी फौज में ही भेजा, जबकि फौजियों की इज्जत करने वाले इस समाज में ”स्टीपल चेज़” की उपलब्धियों की धज्जी उड़ते वे खुद देख चुके थे। कहने का मतलब ये कि अकेले विभाजन की शुष्क सहानुभूति के दम पर आप व्यक्तित्व के परनालों से बहता मवाद नहीं सुखा सकते। उसके लिए एक मूल्यबोध ज़रूरी होता है जो व्यक्तित्व में मवाद को बनने नहीं देता। पान सिंह तोमर के व्यक्तित्व में और लिहाजा उन पर बनी फिल्म में भी यह मवाद नहीं है। मिल्खा सिंह चूंकि जिंदा हैं, ज्यादा प्रकट हैं, इसलिए उनका विश्लेषण तो होता ही रहेगा।
और आखिरी बात जो कतई मौलिक नहीं है। अंतत: निर्देशक ही फिल्म के लिए जिम्मेदार होता है। शरणार्थी शिविर के तंबू से आती आवाज़ पर सिनेमाहॉल का प्रश्नाकुल बच्चा, पाकिस्तान विरोधी सेंटिमेंट पर हुलसित पीवीआर की जनता, ऑस्ट्रेलियाई चुंबन पर हॉल में पड़ती सीटियां, उपलब्धि के पौरुष की छाया में चार ”सबजुगेटेड” महिला पात्रों का बिला जाना, एक बची-खुची महिला पात्र का दमन के आगे सविनय समर्पण, भारत-पाकिस्तान मैत्री खेल के परदे पर ट्रीटमेंट से निकलती अंधराष्ट्रवाद और विद्वेष की छाया- अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी की वास्तविक घटनाओं की ये सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं और प्रतिच्छवियां हैं, तो बुनियादी सवाल उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि निर्देशक पर ही खड़ा होता है। फिल्म तो मारियो पुज़ो के गॉडफादर पर भी बनती ही है, बस चुनना निर्देशक को होता है कि उसे ज़ख्मों से रिसता ताज़ा लाल खून दिखाना है या कि सड़ा हुआ मवाद।
Read more

.jpg)
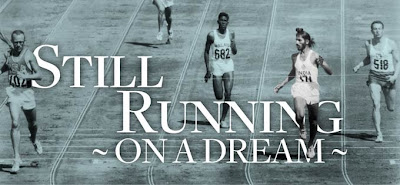



एक अलग पहलू
do baat: india ka kot milne ke baad ghar jane ka time aur suresh kumar wali baat par aapki rai kuch durust nahi hai.. baki baaton se sahmat..
इस बार साॅरी, अगली बार बाॅलीवुड के लोग आपसे पूछ कर फिल्म बनायेंगे। श्रीवास्तवजी आरएसएस व्यवस्था का विकल्प बनने का प्रयास मत किजिए।
मै आपसे सहमत नहीं हु मयंक जी . चीज़े स्वाभाविक न हो पर तथ्यगत होनी चाहियॆ. अगर फिल मिल्खा सिंह जी पर है तो वो तथ्यगत होनी चाहियॆ न की मिलावटी . मै इस सन्दर्भ में शहारुख खान द्वारा निर्मित फिल्म 'अशोक ' का उदाहरण देना चाहुङ्गा. अशोक जैसे वैभवशाली शाशक के ऊपर बनाने वाली फिल्म महज एक लड़की के आस पास ख़तम हो जाए ये बस भारत बर्ष में ही हो सकता है. तो मेरा मानना है के आप पुरे इमानदारी से आगे ही बोल दो की ये उनके जीवन के बारे में नहीं बस थोड़ा सा अवलम्बन लिया गया है. लेखक की ये बात भी मुझे पसंद आयी की फिल्म अगर खिलाड़ी के बारे में है तो बात खेल के बारे में हो तो ही अच्छा है
इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.
लेख में आधे से अधिक तथ्य बेबुनियाद समझ में आ रहे है
जाहिर सी बात है अगर इतना स्वाभाविक दिखाना होता तो फिल्म नहीं बल्कि धारावाहिक दिखाया जाता
एक फिल्म में जितना हो सकता था उसके लिहाज़ से फिल्म लाजवाब है
कुछ तथ्य विचारणीय हैं, जैसे बाघा बोर्डर वाली बात पर निर्देशक के शोध का फल शून्य है
किसी और फिल्म से या व्यक्ति से तुलना के मामले में कहना चाहूँगा कि सभी लोग और परिस्थितियां एक सी नहीं होती जरुरी नहीं कि जैसा पहले किसी महान व्यक्ति ने किया हो तो लोग उसी को दोहराए