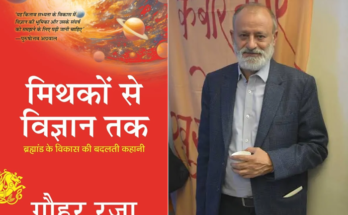कोविड-19 के प्रभाव ने हमारे सामने दुनिया को देखने का अलग नज़रिया दे दिया है। कहा यह भी जा सकता है कि उसने चीजों, स्थितियों और मनुष्यों के प्रति हमारे नज़रिये को बदलने को हमें मजबूर कर दिया है। समय न होने के पूंजीवादी मंत्र को उसने तहस-नहस कर दिया। मार्च से अब तक के लगभग पाँच महीनों में समय न होने का मिथक टूट गया है। संसद, न्यायपालिका सब कुछ ठप और कॉर्पोरेट भी चारों खाने चित।
उसने सबसे पहले अपनी जवाबदेहियों से पल्ला झाड़ा, फिर सामाजिक जिम्मेदारियों से भी। अपने लिए सुविधाजनक ‘वर्क फ्रॉम होम’ की गुंजाइश निकाली। कोविड ने दुनिया को घरों में समेट दिया। इसके अनेक भयावह पक्ष हैं जो समाज के अनेक संस्तरों पर अलग-अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव स्त्रियों पर पड़ा है। वे समाज के हरेक संस्तर पर शोषण, दमन और हिंसा का शिकार हुईं। कहीं उनके लिए रोजगार की समस्या खड़ी हुई तो कहीं पारिवारिक अत्याचार की। मध्यवर्ग की स्त्रियां भी इससे अछूती नहीं रहीं। इसी विषय को लेकर प्रख्यात अभिनेत्री नन्दिता दास ने सात मिनट की एक लघु फिल्म “लिसेन टु हर” (उसको सुनो) बनायी है।
फिल्म की कहानी कुल इतनी है कि नन्दिता दास कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। बीच में बच्चे को खेल और पढ़ाई संबंधी निर्देश देती रहती है। बच्चा माँ के साथ ही अधिक दिखता है। दूसरे कमरे में मौजूद पिता से उसका कोई खास सरोकार नहीं दिखता। कुरियरवाला आता है तब भी दरवाजा पत्नी खोलती है। पति अंदर से आदेश देता है। फिल्म का हुक पॉइंट यह है कि नन्दिता दास के फोन पर बार बार एक अन्य महिला का फोन आता है और उधर से पुरुष के डांटने-फटकारने-मारने की आवाज आती है और स्त्री बचने की कोशिश करते हुए चीखती है। वह फोन पर नन्दिता दास से सहायता की गुहार लगाती है। नन्दिता दास के सामने दोहरा संकट है। उस पर वर्क लोड है लेकिन वह संवेदनशील स्त्री है। झुंझलाहट के बावजूद फोन को इग्नोर करना उसके लिए असंभव है। लिहाजा वह न केवल फोन सुनती है बल्कि पुलिस को फोन करती है, जहां से उदासीन जवाब मिलता है और अधिक ज़ोर देने पर यह कहा जाता है कि पुलिस को अपनी ड्यूटी खूब पता है कि उसे क्या करना चाहिए। अंततः वह महिला को कॉलबैक करती है। फोन महिला का पति उठाता है और गुस्से में कहता है रांग नंबर। फिल्म खत्म हो जाती है।
वैसे यह कोई खास फिल्म नहीं है, फिर भी अपने विषय के कारण यह महत्वपूर्ण बन जाती है। बस एक मॉडल पर सिंगल लोकेशन पर फिल्माया गया दृश्य भर है जिसमें नन्दिता दास का थका हुआ चेहरा, झुंझलाहट, पति द्वारा अंदर से दरवाजा खोलने का आदेश और पत्नी का रुआँसा चेहरा घरेलू हिंसा की एक अलग ही इबारत लिखता प्रतीत होता है। असल में इसी कारण यह लघु फिल्म खास मायने बना लेती है। एक मध्यवर्गीय स्त्री इग्नोरेंस और उत्पीड़न की जीती-जागती मिसाल बन गयी है।
लिसेन टु हर फिल्म में दो स्त्रियों की समानांतर स्थिति दिखायी गयी है। दोनों कामकाजी हैं लेकिन अलग-अलग वर्ग से आती हैं और दोनों ही प्रताड़ना का शिकार हैं। नंदिता दास ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कामकाजी पति के होने के बाद भी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन स्वयं करती है क्योंकि वह पहले एक स्त्री ओर पत्नी है। फिल्म में नंदिता दास चिड़चिड़ाते या विरोध करते या नाराज़ होते हुए भी सहजता से वे सारे काम करती है क्योंकि उसे एक स्त्री के रूप में यही सिखाया गया है। दूसरी ओर फोन पर रोती स्त्री इस उम्मीद में उससे अपनी तकलीफ़ साझा करती है कि शायद कोई मदद मिल जाए और पति की मार से छुटकारा मिल जाए। पति उसे इसलिए मारता है क्योंकि वह उसके कहे अनुसार काम नहीं करती है। उसकी बात नहीं मानती है।
यानी आपका अपना कोई सोच-विचार या निर्णय है ही नहीं। नौकरी पर जाने वाली स्त्रियों को घर के पुरुष यह बताते हैं कि बॉस से कैसे बात करनी है और क्या नहीं। यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में सरपंच के चुनाव में यदि महिला प्रत्याशी है तो उसके पति के नाम के आगे लिखा जाता है सरपंच पति अमुक-अमुक। प्रख्यात नारीवादी चिंतक सीमोन द बोउवा ने जहां इसके अनेक जैविक आधारों की विवेचना की है वहीं जर्मेन ग्रीयर ने बधिया स्त्री को साहित्य की विधाओं, लोकगाथाओं और मिथकों में खोजा है।
महज सात मिनट की बहुत ही छोटी फिल्म में लॉकडाउन के बहाने ‘वर्क फ्रॉम होम’ में कामकाजी स्त्रियों की जो दशा चित्रित की गयी है वह केवल लॉकडाउन के समय की नहीं है, बल्कि सामान्य दिनों में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही होती है। हर काम के लिए पुरुष, स्त्री की ओर ताकता है कि वह उसे करे और स्त्रियां बिना शिकायत के करती हैं क्योंकि मना करने और रिएक्ट करने पर मनमुटाव या लड़ाई-झगड़ा-बहस की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे घर में अशांति होगी और इसी से बचने के कारण मन होने न होने, थके होने या शारीरिक कष्ट होने के बावजूद औरतें सब काम चुपचाप कर देती हैं। यही नंदिता दास ने फिल्म में किया। स्त्रियों के किसी भी काम को, चाहे वह घर का हो या ऑफिस का, दोयम दर्जे का गिना जाता रहा है जबकि कामकाजी स्त्रियां इस बात को लेकर ज्यादा सतर्क रहती हैं कि कहीं उन्हें यह न सुनने को मिल जाए कि नौकरी कर रही हो तो घर-परिवार को कम महत्त्व दे रही हो। फिल्म में नंदिता दास की ऑनलाइन मीटिंग में कई बार रुकावट आती है और वह बार-बार पति, बच्चे, डोरबेल और फोन का जवाब देती है, जबकि उसके खुद के फोन को छोड़कर बाकी काम उसके पति भी कर सकते थे। यह एक तरह से टॉर्चर करने का तरीका ही है। केवल मारपीट या गाली-गलौज ही हिंसा की श्रेणी में नहीं आते बल्कि किसी की इच्छाओं को रौंदकर अपनी बात मनवाना भी हिंसा है।
यह सब इतना सहज तरीके से होता है कि कहने और करने वाले दोनों को कुछ भी गलत नहीं लगता। सोसाइटी के हिसाब से मानसिक प्रताड़ना का तरीका अलग अलग हो सकता है। मारपीट दिखायी देती है इसीलिए उसे प्रत्यक्ष हिंसा कह सकते हैं, लेकिन नंदिता दास के साथ प्रताड़ना नहीं हो रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसके पति ने एक बार भी उससे अपशब्द नहीं कहा तब भी ये नहीं माना जा सकता कि वह प्रताड़ित नहीं हुई। यह कितनी विचित्र स्थिति है कि खुद बॉस होते हुए भी वह अपने काम को सौ प्रतिशत नहीं दे पाती क्योंकि किसी को परवाह ही नहीं है कि उसका काम बहुत जरूरी या महत्त्वपूर्ण है। ऐसा हमारे घरों में या हमारे आसपास रोज़ होता है और हम बेफिक्र रहते हैं कि हमारे साथ मारपीट नहीं हो रही है तो हम प्रताड़नामुक्त हैं। सच यह है कि सबसे ज्यादा स्त्रियाँ मौखिक प्रताड़ना का शिकार होती हैं।
लॉकडाउन के इन 5-6 माह में घर से ऑनलाइन काम करने वाली हर स्त्री ऐसे संकट से गुजर रही होगी और अब भी गुजर रही है। कई स्कूल टीचरों ने बातचीत में कई बार यह ज़रूर कहा कि कब स्कूल खुले तो वहां जाकर काम किया जाए। घर पर रहते हुए ऑनलाइन होना बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि अभी सब लोग घर पर हैं तो सबके हिसाब से काम करो। स्कूल जाने पर कम से कम पूरे तरीके से वहीं दिमाग रहता है तो काम का आउटपुट बेहतर होता है। यहां ऑनलाइन में बॉस और घर वालों दोनों का दबाव झेलना होता है जो बहुत मानसिक थकान देता है।
हम लोगों में से अधिकतर स्त्रियां वैसा ही जीवन जीती हैं जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है लेकिन कभी असहज महसूस नहीं करती हैं क्योंकि उनमें ऐसी आदत डाल दी जाती है। उनकी इस प्रकार कंडीशनिंग कर दी जाती है इसीलिए उन्हें ये सब बुरा नहीं लगता। इसके उलट कभी पुरुष द्वारा कोई काम कर दिये जाने पर हम बहुत खुश होते हैं और एप्रिशियेट करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि सुबह से लेकर रात तक खटने पर भी कोई सराहना नहीं मिलती बल्कि यही सुनने को मिलता है, ‘क्या करती हैं स्त्रियां सारे दिन घर पर रहकर? सिर्फ पकाना और खाना।’ जो घरेलू काम हम करते हैं उससे कोई अर्थोपार्जन नहीं होता है इसीलिए इसका महत्व नहीं होता। काम का दायरा तय कर दिया गया है और उसी दायरे में रहते हुए जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन आज के समय में स्त्रियां जब घर से बाहर निकल कर काम पर जा रही हैं, दो-दो जगह की जिम्मेदारियां उठा रही हैं, सफल भी हो रही हैं फिर भी उनको बहुत महत्व नहीं मिल रहा है। इस वजह से लिसेन टु हर फिल्म का विश्लेषण जरूरी है।
सिमोन ने कहा है कि स्त्रियां पैदा नहीं होतीं बल्कि बनायी जाती हैं। कहने का मतलब है कि स्त्री होने के लिए योनि का होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके दिमाग और सोच में ऐसी समझ डाली जाती है कि वे अपने चारों ओर तय की गयी बातों को अमल में ले आयें। इस प्रकार वे स्त्रियोचित गुणों से लबालब हो जाएं जैसे शर्म, लिहाज, झुकना, आज्ञाकारी होना, निर्णय लेने में पिता, पति, पुत्र या भाई की मदद लेना, स्वयं को अक्षम साबित करना, पिता-भाई के अनुसार पहनावा करना, दोस्ती पर घर से सहमति लेना, एक तय उम्र में घरेलू कामों में दक्ष हो जाना और परिवार में बच्चे और घरेलू कामों को प्राथमिकता देना । यही सब हम अपने घरों में माँ-दादी-चाची-दीदी को करते देखते हैं तब हमें ये कहीं असामान्य नहीं लगता ओर हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। कभी हमको अपने अधिकारों के लिए बोलना-लड़ना या छीनना सिखाया ही नहीं जाता है और यही कारण है कि सिमोन की कही बात साबित हो जाती है कि स्त्रियां पैदा नहीं होतीं बल्कि बनायी जाती हैं। सिमोन फ्रांस की स्त्रियों और खासकर अपने परिवार और समाज की स्त्रियों के बारे में लिखती हैं जिसमें स्त्रियों की दयनीयता का उल्लेख है और इसके बाद उन्होंने परिवार से विद्रोह किया। इसी विद्रोह ने उन्हें स्त्री विमर्श की महान लेखिका बनाया। सिमोन का उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि किसी भी स्त्री को बड़ा काम करने के लिए स्थितियां बनी-बनायी नहीं मिलती हैं बल्कि उसे खुद बनानी पड़ती है, जैसा सिमोन ने किया।
यह फिल्म जैसे हमारे समय के अंधेरे चेहरे पर आईने की रोशनी भर दिखाती है, लेकिन उस क्षणिक रोशनी में एक त्रासद, कंडीशंड और तकलीफ़ों से भरी दुनिया हठात हमारे सामने दिख जाती है जिसके कई आयाम और समानान्तर कथाएं हैं। एक सतत और घुटन भरे यथार्थ को समेटती हुई यह लघु फिल्म इसीलिए देर तक न सिर्फ जेहन में बची रहती है बल्कि अनेक स्तरों पर हमारे भीतर के घावों को हरा भी कर देती है!
अपर्णा छत्तीसगढ़ की रंगकर्मी हैं और गांव के लोग पत्रिका की प्रबंध संपादक हैं