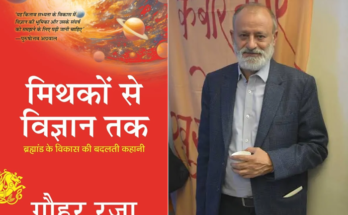जैविक व्यक्तित्व की तलाश करनी है तो गाँव की ओर जाना होगा। तलाश वहीं संभव है, चूंकि मानव जाति द्वारा निर्धारित सभ्यता के इतिहास में सबसे आत्मीय गाँव ही है। मनुष्य की देह को गांवों ने सहज रूप से प्रकृति के अनुकूल केन्द्रित होना सिखाया है। उसके द्वारा रचे-गढ़े संतुलन को मनुष्य आत्मसात कर ले तो इससे बेहतर सभ्यता स्थली नहीं हो सकती। और मुमकिन है, वह इसी के सहारे अपनी आत्मा को तलाशता रहता है। और इसके प्रतीक के रूप में हजारों वर्षों से ‘बिजूका’ को संभाले रखा है। इसी आत्मा के प्रतीक का एक रूपान्तरण ‘बिजूका’ शीर्षक से रची गई पेंटिंग है। ऐसा लग सकता है कि यह प्रतीक गाँव का ऐसा ‘लोक का प्रतीक और एक मनोबिम्ब मात्र है’।

मनोबिम्ब भी एक यथार्थ है। इसके कई रूप हो सकते हैं। याने लंबे इतिहास से जारी संघर्ष का संभावित सार है। यह परिकल्पित नहीं है। एक आदर्श है। आदर्श एक इकाई नहीं, यथार्थ भी है। इन दोनों के बीच लंबी और गहरी खाई है। तभी तो हम भारत के गांवों को देश और प्रकृति के सुनहरे आंचल की तरह देखते हैं। हमारा नजरिया वैज्ञानिक होना चाहिए। ताकि इस सुनहरे आंचल के भीतर के यथार्थ के संसार में प्रवेश कर सकें। इसीलिए शहरी जिंदगी के घुसपैठ के दौर में गांवों पर पूंजीवाद का विकृत चेहरा छा रहा है। गांवों की आत्मनिर्भर इकाई छिन्न-भिन्न हो रही है। यजमानी व्यवस्था खोखली होती जा रही है। रिश्तों में टूटन की दीवार खड़ी हो गई है। इसीलिए इस जैव-व्यक्तित्व के रूप में एक और पेंटिंग मेरे जहन के भीतर से फूटती है– ‘छोड़कर मत जाओ बिजूका’।

इस पेंटिंग में एक लड़की बिजूका को कसकर पकड़ती है। मानो वह बिजूका से गुहार लगा रही है – इस सुनहरे आंचल की जड़ में अमानवीय चेहरा पनपने लगा है। इस त्रासदी भरे समय में तुम ही तो जीवित हो, जो हजारों सालों से हमारे हर दुख-दर्द के साथी रहे हो। और रहोगे। यह देहाती लोगों की संभावनाओं का सार है।
हर बार इतिहास के प्रत्येक लम्हों में प्रकृति की मार को किसान सहता है। और जुट जाता है धरती माँ की छाती से अन्न उपजाने में। प्रकृति की पीड़ा से वह ग्रस्त है। पीड़ा झेल रहा है। उसे इस जकड़न का अहसास है और तथाकथित विकास के जकड़न के दड़बे में ही फँसता जा रहा है। लेकिन उसकी संवेदनशीलता पर कोई आंच नहीं आ रही है। इसी का बिम्ब एक पेंटिंग में उभरा– ‘मेहनतकश किसान’ के रूप में।

वह सपने संजोते रहता है कि माँ के सुनहरे आँचल में रंग-बिरंगे अंकुर अंकुरित होंगे और वह उस आँचल की छाँव में सुकून से आराम करेगा। इस तरह उसकी दुनिया लह-लहा उठेगी। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है – निरंतर प्रकृति की लूट-खसोट और जलवायु परिवर्तन की मार किसान ही झेल रहा है। साथ ही इसके सत्ता को संचालित करने वाली ताकतों याने कॉर्पोरेट घरानों के कृषि के काले कानूनों से भी। इसका प्रतिबिंब और एक पेंटिंग में ‘अब तो बरस पानी’ के रूप में खड़ा होता है।

ऊबड़-खाबड़ हो गए खेत में किसान गुहार लगा रहा है, ‘अब तो बरस पानी’। बाढ़ आई तो बरबादी, नहीं आई तो बरबादी। और तो और स्वच्छ पानी के लिए कॉर्पोरेट घरानों का जमीन के भीतर के पानी का दोहन भी है। बस इसी बरबादी के चलते एक नहीं अनेकों गाँवों में आत्महत्या का सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाकों में अन्य प्रथा की तरह एक और दस्तूर ‘आत्महत्या’ का भी बनता जा रहा है। सभी मौन हैं। इसी मौन का बिम्ब ‘किसानों की सामूहिक चिता’ पेंटिंग के रूप में उभरा।

विकास के हर दौर में किसानों को जकड़ने वाली ताक़तें लामबंंद होती रही हैं। चाहे वह प्रकृति की मार हो, प्राचीन काल की संकीर्णता हो, वर्ण-व्यवस्था की श्रेणीबद्धता, पितृसत्ता और मनुवाद का शिकंजा हो, यह आज भी मौजूद है। और लगातार इस कड़ी में जुड़ता चला गया – नियतिवाद, गरीबी, आत्मविश्वास और स्वाभिमान की कमी। इस कड़ी का और एक महत्वपूर्ण पहलू है ‘अशिक्षा’। इस संदर्भ में 1883 में महात्मा जोतिबा फुले का ‘किसानों का कोड़ा’ स्मृति पटल में उभरकर आ जाता है। कचोटता रहता है कि आज भी स्थिति जस की तस है। इस पुस्तक में फुले जी ने व्यक्त किया है, ‘विद्या के न होने से बुद्धि नहीं, बुद्धि के न होने से नैतिकता न रही, नैतिकता के होने से गतिमानता न आयी, गतिमानता के न होने से धन-दौलत न मिली, धन-दौलत न होने से शूद्रों का पतन हुआ। इतना अनर्थ एक अविद्या से हुआ।‘
इसी कसक की परिणिति स्वरूप न जाने कब इस सुनहरे आँचल की छाँव में फँसता गया। यह बिम्ब पेंटिंग ‘मकड़जाल में फँसता किसान’, ‘खेल-खेल में फँसता किसान’ और ‘मृत किसान का घर’ बड़ी सहजता से देहाती प्रतीक पेंटिंग में सायास ही उभरकर अपनी जगह बना ली। मसलन, हाथ में धागे का फांस बनाने का खेल, चव्वा-अट्ठे का खेल और किसान के दरवाजे पर मृत किसान का पैर और दरवाजे की चौखट पर धार्मिक अंध-विश्वासों के बिम्ब बहुत कुछ कह जाते हैं पेंटिंग में।

आज गाँव इस विकास प्रक्रिया में आत्मविहीन शहरीकरण के रूप में ठगा सा खड़ा है। किसानों ने बड़ी-बड़ी लड़ाई लड़ी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हाँ एक बात जरूर है – प्रत्येक किसान आंदोलन में किसान मज़हब, जाति से ऊपर उठ जाता है। वह केवल किसान ही होता है। जिस गांधी ने किसानों को देश की आत्मा कहा था, गांधी ने देहातों के अर्थशास्त्र के बारे में कहा था, ‘जब भी मैं किसी ग्रामीण की कुटिया में जाता हूँ तो एक डोर पर एक तेल-किट्ट बोतल लटकी नजर आती है। वह मजूर जब शाम को घर लौटता है तो डोर से बोतल निकालकर एक पैसे का खाने का तेल लेकर आता है। यह अर्थव्यवस्था बदलनी चाहिए। एक आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था अस्तित्व में आनी चाहिए।”

यह एक स्वप्न बनकर ही रह गया। बहुत दिनों तक यह प्रश्न सालता रहा और गांधीजी के सपनों के बीच से एक पेंटिंग – ‘यह किसान की नहीं, गांधी की हत्या है’, एक दुस्वप्न की तरह इस कड़ी में जुड़ गई।

वहीं इन हालात से जूझता, लड़ता-भिड़ता किसान थक-हारकर विवश हो जाता है। उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। इसी विवशता में ‘ये गाँव बेचना है’ की राह पकड़ लेता है। यह मार्मिक क्षण भी पेंटिंग में उभरकर आ गया।

लेकिन किसान आत्म-विभाजन के इस चौराहे पर खड़े होकर सोचता है – रास्ता है, सोचा जाय और उसकी इस भावना की झलक ‘उफ, सोचना पड़ेगा’, एक नया रूप अख़्तियार करती है।
एक अरसे पहले कवि लीलाधार जगूड़ी की कविता पढ़ी थी। सहसा इस घड़ी में वह कविता याद हो आयी –
ड्राईवर!
हम है तुम्हारे गाँव के लोग
जागो
ड्राईवर!
देखो, चीजों में अब भी स्वाद है
हमारे पास रोटी और साग है
खाओगे?
कुएं का जल है; पिओगे?
कहाँ जाना है?
ड्राईवर!
हमें राजधानी से अपना गाँव
छुड़ाकर लाना है।