अरूंधति रॉय के कई परिचय हैं। वे बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका हैं; एक निबंधकार हैं, जिनकी नवीनतम रचना ‘आजादी’ पिछले साल ही प्रकाशित हुई है; और वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। भारत में रहने वाली वह ऐसी लेखिका हैं जिन्हें पढ़कर पाठक अपना विचार बनाते हैं, चाहे वह भारत की राजनीति हो, भूमंडलीकरण हो या कोरोना वायरस की महामारी हो। अरुंधति रॉय ने इन सभी विषयों पर नैतिक स्पष्टता और उद्देश्यबोध के साथ लिखा है। शायद यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वह एक तरह का ही विचार रखती हैं- एक ऐसी शख्सियत जो बहुत साफगोई से अपने आसपास की दुनिया में घट रही घटनाओं को तरह-तरह से दिखाने की कोशिश करती हैं। न्यू स्टेट्समैन ने अरूंधति रॉय के साथ एक ई-मेल के ज़रिये साक्षात्कार लिया। न्यू स्टेट्समैन ने उनसे भारत, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, साहित्य और राजनीति पर सात सवाल पूछे। उन्होंने उन सातों सवालों के जवाब लिखकर वापस भेजे। इस साक्षात्कार का अनुवाद वरिष्ठ पत्रकार और जनपथ के स्तम्भकार जितेन्द्र कुमार ने किया है।
संपादक
मैं कुछ दिन पहले (शायद 2019 में) ‘’दि अल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस’’ पढ़ रही थी। आपने जो इसमें लिखा है वह हालांकि कोई दो दशक पहले की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने तब जो कहा और जिसके बारे में चेताया था, खासकर भारत की राजनीति के संदर्भ में, वह तो आज घटित हो रहा है। क्या भारतीय समाज के कुछ ऐसे भी आयाम हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि आप विशिष्ट रूप से भविष्यवाणी कर रही थीं उस वक्त?
मैं माफी चाहती हूं, लेकिन इसका जवाब इतना छोटा नहीं हो सकता है। अपने आपको भविष्यद्रष्टा कहना न सिर्फ अपना पीठ थपथपाना होगा, बल्कि बहुत से दूसरे लोगों को आसानी से बख्श देना भी होगा। खासकर जिन चीजों के बारे में मैं लिख रही थी उनमें से ज्यादातर हमारी आंखों के सामने घट रही थीं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में से लाखों-करोड़ों लोगों ने इसे जीया है, अनुभव किया है।
आपने जिस किताब का जिक्र किया है उसमें विभिन्न विषयों पर लेख हैं, उसमें भारत के परमाणु परीक्षण पर लेख है, बड़े बांधों और उसके खिलाफ नर्मदा घाटी के जन आंदोलन पर लेख है, पानी-बिजली और दूसरे बुनियादी ढांचे के निजीकरण, न्यायिक स्वतंत्रता, मीडिया और लोकतंत्र को बचाने वाली अन्य संस्थाओं में लगातार हो रहे क्षरण पर लेख हैं।
और हां, उसमें ‘’लोकतंत्र- किस चिड़िया का नाम है’’- शीर्षक से भी एक लेख है। यह लेख गुजरात में 2002 में दंगाई हिंदू भीड़ द्वारा किए गए मुस्लिमों के जनसंहार के बारे में है, जब नरेन्द्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। वह एक ऐसी घटना थी जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन (आरएसएस)- जो लगभग सौ साल के अपने काल में देश का सबसे ताकतवर संगठन बन चुका है- के एक अदना प्रचारक से प्रधानमंत्री के पद पर सत्तासीन करवा दिया। वे इसी घटना के कारण प्रधानमंत्री बने हैं, इसके बावजूद नहीं।

2002 का गुजरात नरसंहार भविष्यद्रष्टा वाले प्रश्न को जांचने-परखने का बढिया तरीका है। उस साल फरवरी और मार्च के दरमियानी हफ्ते में ट्रेन के एक डिब्बे में हुई आगजनी में 59 हिन्दू तीर्थयात्री मारे गए थे। इसके प्रतिशोध में गुजरात के गांवों और शहरों में हजार से अधिक मुसलमानों को संगठित भीड़ के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें जिंदा जला दिया गया, एक लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया गया। नरसंहार को राष्ट्रीय चैनलों पर लाइव कवर किया गया था। हम सबने मुख्यमंत्री मोदी के क्रूर और उत्तेजक भाषण सुने हैं। इसके बाद समाचार पत्रिका तहलका के लिए काम करने वाले पत्रकार आशीष खेतान ने अंडर कवर रहकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें कुछ हत्यारों और बलात्कारियों ने अपने अपराध को गर्वोक्ति के साथ स्वीकार किया। उस भयावह टेप को टीवी चैनल पर दिखाया गया, जिसे हम सबने देखा था। उनमें से अनेक हत्यारों ने खुले तौर पर अपने नए साहसी मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया था। अपनी हालिया किताब ‘’अंडर कवरः माइ जर्नी इन द डार्कनेस ऑफ हिन्दुत्व’’ में आशीष खेतान ने बहुत ही शांतचित्त होकर विस्तार से इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह ऊपर से नीचे तक पुलिस महकमे और कानूनी प्रक्रिया को अपराधियों की रक्षा के लिए बाध्य कर दिया गया था।
यही कारण है कि आज भारत में बड़े पैमाने पर न सिर्फ हत्यारे और बलात्कारी खुले आम घूम रहे हैं, बल्कि ऊंचे ओहदे पर भी बैठे हुए हैं जबकि बेहतरीन कार्यकर्ता, वकील, विद्यार्थी, ट्रेड यूनियन के नेता और दसियों हजारों आम लोग, मुसलमान, दलित और बड़ी संख्या में आदिवासी कई वर्षों से जेल की सजा काट रहे हैं। बिना किसी कारण के।
मेरे कहने का कुल आशय इतना है कि 2002 की गुजरात घटना के बाद यह समझने के लिए भविष्यवक्ता होने की जरूरत नहीं थी कि मोदी किस मिट्टी के बने हैं, आरएसएस किसका प्रतिनिधित्व करता है और अगर मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी देश के साथ क्या कर सकती है। इनमें से किसी को भी अपनी मंशा जाहिर करने में कोई शर्म नहीं थी, मोदी को तो बिलकुल भी नहीं। इसके बावजूद, नरसंहार के बाद भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उनका समर्थन किया। मीडिया ने तत्काल उन्हें ‘विकास करने वाले मुख्यमंत्री’ के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। कई उदारवादी बुद्धिजीवी मेरे जैसे लोगों के खिलाफ सिर्फ इसलिए हो गए क्योंकि हमने उनकी आलोचना करने से इंकार कर दिया था। जब उनकी बिछाई लाल कालीन पर चढ़कर मोदी दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुए, तब बड़े-बड़े संपादक, पत्रकार और बुद्धिजीवी आवेग में हर्षोन्माद करने लगे। अब उनमें से कई का अब मोहभंग हो चुका है और वे बड़े साहस के साथ उनके आलोचक बन गए हैं, लेकिन इससे यह बात छुप नहीं जाती कि कैसे इन लोगों ने गुजरात नरसंहार और उसमें मोदी की निभायी भूमिका को उस वक्त हज़म कर लिया था।
इसलिए मैं अपने तईं इसे भविष्यवाणी तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। यह तो राजनीति है। मूल बात ये है कि हम क्या देखना चाहते हैं और किसे हम नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। हमें अपने आप से कुछ गंभीर सवाल पूछने चाहिए- इसलिए नहीं कि हमें वैचारिक शुद्धता की खोज कर लेनी है या दोषरहित होकर काम करना है या फिर हमें कोई ऐसी विश्वदृष्टि अपना लेनी है जहां लोग या तो विशुद्ध शोषक हैं या विशुद्ध शोषित। बात इसके ठीक उलट है, क्योंकि वास्तविक जिंदगी इस स्थिति के लिए इजाजत ही नहीं देती है। लेकिन कम से कम हम उन जटिलताओं, उन अंतर्विरोधों के प्रति तो ईमानदार हो ही सकते हैं जिनके भीतर हम जीते हैं, काम करते हैं और सोचते हैं। जैसा कि जॉन बर्जर ने लिखा है- कोई भी कहानी दोबारा इस तरह नहीं सुनायी जा सकती है गोया वह इकलौती हो। इसलिए अब कुछ गंभीर सवाल।
मसलन, क्या मैं तुकबंदी करने वाली वह उपन्यासकार हूं जिसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जिस देश में वह रहता है वहां सामाजिक भेदभाव की सबसे क्रूर व्यवस्था काम करती है, जिसका नाम जाति है? क्या मैं भारत की वह मानवाधिकार कार्यकर्ता हूं जो कश्मीर के सैन्य कब्जे पर, वहां अनजान कब्रों की मौजूदगी पर और दसियों हजार जिंदगी खत्म कर दिए जाने पर चुप रहता है? या फिर ऐसा है कि मैं कश्मीर के लिए तो बोलती हूं लेकिन इंतेफादा की शुरुआत में वहां मारे गए हजारों कश्मीरी पंडितों से मुंह मोड़ लेती हूं या फिर बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए नरसंहार पर मौन साध लेती हूं? क्या मैं वह मार्क्सवादी हूं जो गुलाग को खारिज करता है? या फिर वह मुसलमान, जो होलोकॉस्ट से इंकार करता है? क्या मैं वह गांधीवादी हूं जो नस्ल और जाति पर गांधी के विचारों पर पर्दा डालता है? या फिर मैं उन लोगों में शामिल हूं जो वर्ग को तो देखते हैं लेकिन जाति को नहीं या इसका उलटा?
क्या मैं वह पत्रकार या जज हूं जो सत्ता के तलवे चाटता है और जनता को कचरा समझता है? क्या मैं जंगलों में आदिवासियों की हत्या में लिप्त खनन कंपनियों द्वारा पोषित साहित्य महोत्सवों की नियमित वक्ता हूं जो उनके मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राग अलापती हूं? या फिर मैं संतुलन साधने वाले उन उदारवादियों की तरह हूं जो बहुसंख्यकवादी फासिस्ट राजसत्ता द्वारा किए गए नरसंहार और प्रतिरोध आंदोलनों में गाहे-बगाहे होने वाली हिंसा के बीच समानता ढ़ूंढने की कोशिश करते हैं? क्या मैं हालिया किसान आंदोलन के दौरान उपजे उन मासूम समर्थकों की तरह हूं जो भूजल संकट, एकफसली खेती (मोनोकल्चर) के खतरों और खेती में तथाकथित हरित क्रांति के नतीजों के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते? क्या मैं उन नारीवादियों की तरह हूं जो मानते हैं कि अफगानिस्तान में बमबारी करके नारीवाद को खत्म किया जा सकता था?
अकेले हमारे राजनेता या राजनीतिक दल गुनहगार नहीं हैं। गुनाह अकेले हमारे मसीहाई नेताओं और उनके गुर्गों का भी नहीं है। यह तो सरलीकरण हो जाएगा। इसीलिए, आपके प्रश्न पर मेरा लंबा जवाब है कि नहीं, मैं नहीं मानती कि मैं भविष्यद्रष्टा थी।
क्या कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिन्होंने आपको अचंभित किया? मतलब आपने जैसा सोचा उसके मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी और तीव्रता से वे चीजें बदतर (या बेहतर) होती गयीं?
हां, जनता। लोगों ने दो बिलकुल अलहदा तरीकों से मुझे अचंभित किया है। एक तरफ, मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर कि जब नफरत के बीज बोये जा रहे थे तब हमारी जमीन कितनी उपजाऊ और सुग्राह्य थी कि देखते-देखते हमारे आसपास इतनी तेजी से घने जंगल उग आए। ऐसे में हमारा सहज अहसास तो यही होगा कि फासीवाद का यह विशिष्ट रूप भारतीय राजसत्ता और ‘जनसमूह’ की परस्पर साझेदारी का परिणाम है। यह समझदारी हालांकि टेक्सस में ‘हाउडी मोदी’ शो में जयजयकार करने वाली भीड़, मोदी/आरएसएस के तंत्र द्वारा तकरीबन पूरी तरह दुहे जा चुके मुख्यधारा के भारतीय मीडिया, नौकरशाही, न्यायपालिका, सुरक्षा बलों और चुनावी मशीनरी को संज्ञान से बाहर छोड़ देती है, जबकि ये सभी मिलकर सत्ता की सेवा में नतमस्तक हो चुके हैं। लिहाजा हम अब इस स्थिति में नहीं रह गए हैं जहां किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल की आलोचना हालात को समझने या उसे बदलने में पर्याप्त हो।
दूसरी ओर, विपक्षी राजनीतिक दलों और विभिन्न संस्थाओं ने लोकतंत्र में निगरानी और संतुलन की भूमिका निभाने की अपनी जिम्मेवारी से जब पल्ला झाड़ लिया हो, वैसे में आम लोगों ने उससे खाली हुई जगह को भरने का काम किया है। ऐन उस वक्त जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं रह गयी, प्रदर्शनकारियों की हिम्मत और कल्पनाशीलता ने मुझे हैरत में डाल दिया। मुस्लिम विरोधी नागरिकता कानून और अकेले असम में 20 लाख लोगों को नागरिकता से महरूम कर देने वाले नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ जैसा व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ अभी जो प्रदर्शन चल रहे हैं, वे एक उभरती हुई बग़ावत का संकेत देते हैं।
दो महीने से चल रहे किसान आंदोलन को समझने के लिए कुछ ज़रूरी बिन्दु
इन दोनों प्रदर्शनों को रोकने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों की परिणति उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मजदूर बहुल इलाकों में मुसलमानों के जनसंहार के रूप में हुई जिसके लिए खुद मुसलमानों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही आज दोषी ठहराया जा रहा है। सैकड़ों लोग जेल में बंद हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र-छात्राओं से पुलिस ने पूछताछ की है, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। बीजेपी के जिन नेताओं ने खुलेआम हिंसा का आह्वान किया उन्हें ईनाम-इकराम मिल रहा है। ये लोग अब अपने विभाजनकारी अभियान को असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में लेकर जा चुके हैं जहां परंपरागत रूप से इनकी पकड़ नहीं है। आगे क्या होता है यह तो देखने वाली बात होगी लेकिन चाहे जो भी हो, भारत अभी जिस खतरनाक परिस्थिति में पहुंच चुका है, मुझे नहीं लगता कि उसकी अतिरंजना संभव होगी। किसी नदी को आप विषमुक्त कैसे करते हैं? मेरे खयाल से, विष खुद-ब-खुद उसमें से निकल जाता है। बस, बहती हुई धारा अपने आप ऐसा कर देती है। हमें उस धारा का हिस्सा बने रहना होगा।
जहां मैं रहती हूं- अमेरिका- और जहां से न्यू स्टेट्समैन निकलता है- ब्रिटेन– उन दोनों जगहों के कुछ लोगों का कहना है कि दोनों देशों को भाजपा और भारत में अधिकारों के हनन के खिलाफ बोलना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन केवल पाखंड कर सकते हैं, लिहाजा किसी भी सूरत में जवाब तो हिन्दुस्तान के भीतर से ही आएगा। आप क्या मानती हैं?
मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके सवाल को ठीक से समझ पा रही हूं। जब आप कहती हैं कि अमेरिका और इंगलैंड को बोलना चाहिए तो क्या आप यह कहना चाहती हैं कि अमेरिका की सरकार और इंगलैंड की सरकार को बोलना चाहिए? निश्चित रूप से, अगर वे बोलते हैं तो उनके ऊपर पाखंडी होने का आरोप तो लगेगा ही, लेकिन उससे क्या? अंतराष्ट्रीय मामलों पर भारत सरकार की बयानबाज़ी में जाहिर पाखंड के कमोबेश बराबर ही तो होगा ये! हर सरकार की कथनी और करनी के बीच पाखंड होता है। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया द्वारा प्रसारित फर्जी खबरों के आधार पर इराक के ऊपर किया गया आक्रमण जानलेवा पाखंड नहीं तो और क्या था? यह तो बहुत ही अच्छा होगा अगर यूके और यूएस की सरकारें इस पर बोलें, लेकिन वे बोलेंगी नहीं। कम से कम स्पष्ट रूप से तो कतई नहीं बोलेंगी क्योंकि चीजें इस तरह चलती नहीं हैं। ऐसे रिश्ते आर्थिक, भू-राजनीतिक और उपयोगितावादी फायदों का एक जटिल संजाल होते हैं। माल और हथियारों की खरीद-फरोख़्त से लेकर अंतराष्ट्रीय बाजार में नैतिक लबादे में ढंका व्यापार- ये सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है। इस सब के बीच पाखंड तो बहुत मामूली चीज है। उसकी परवाह भला किसे है।
किसान आंदोलन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन स्वीकार, मेहंदीपुर और जींद में महापंचायत आयोजित: SKM
UP में किसान आंदोलन के समर्थकों पर राजकीय दमन के खिलाफ ICWI ने शुरू की ऑनलाइन पिटीशन
इन सब के बावजूद यह ज़रूरी है कि दुनिया भर की सरकारें कम से कम इतना संकेत अवश्य दें कि वे जानती हैं कि यहां चल क्या रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि इससे उन पत्रकारों को थोड़ी मजबूती और सुरक्षा मिलेगी जो कुछ ऑनलाइन मीडिया मंचों के लिए जोखिम उठाकर लिख रहे हैं; उन एक्टिविस्टों, फिल्मकारों, वकीलों और प्रदर्शनकारियों को राहत मिलेगी जो इस हुकूमत के खिलाफ खड़े होकर अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम नदी के जिस किनारे पर खड़े हैं, जिस ज़मीन पर खड़े हैं, वह बहुत तेज़ी से धंस रही है। हम बहने के कगार पर हैं।
आप लंबे समय से वैश्वीकरण के, पूंजीवाद के, पर्यावरण के मानवीय दुरूपयोग और राष्ट्रवाद की आलोचक रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है अंतत: इस बात की स्वीकारोक्ति हुई है कि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं? या अब भी हम चीज़ों को एक दूसरे से जोड़े बिना संबोधित कोशिश कर रहे हैं?
हां, कुछ हलकों में यह समझदारी विकसित तो हुई है। और यह कई व्यक्तियों द्वारा कई वर्षों के अथक प्रयास के चलते हो पाया है। लेकिन यह कहना ही पड़ेगा कि पर्यावरण का विनाश सोवियत संघ और चीन की सरकार ने भी बड़े पैमाने पर किया है। जब पर्यावरण के विनाश की बात आती है तो राजकीय पूंजीवाद और बाजार आधारित पूंजीवाद एक ही कल्पना से संचालित होते हैं- वे धरती को एक ऐसे संसाधन के रूप में देखते हैं जिसका दोहन मानव समाज आपसी वर्चस्व की लड़ाइयों में करता है, खुद को और अपने पर्यावास को नष्ट कर लेने की कीमत पर भी- यह जनसंहार के हथियारों के मूलभूत तर्क से मिलती-जुलती बात है।
अब पूंजीवाद स्वयं जनसंहार का हथियार बन चुका है। हम इस बात को जानते हैं, लेकिन यह तकरीबन एक सार्वभौमिक धर्म की शक्ल ले चुका है, देवों के देव महादेव की तरह। हम नहीं जानते कि इसकी वेदी पर मत्था टेकने को खुद को कैसे रोका जाए। उदाहरण के लिए, भारत एक प्रयोगशाला में तब्दील हो चुका है जहां साफ़ दिखता है कि एक प्रयोग के तहत धर्म, राष्ट्रवाद और पूंजीवाद को आपस में मिलकर एक मादक अर्क बनाया जा चुका है। इतिहास गवाह है कि यह मानना हमेशा सही नहीं होता कि लोग तार्किक होंगे और खुद अपने भौतिक हितों व वजूद की तलाश करेंगे। मैं अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को समझने की अब तक कोशिश कर रही हूं, जो मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं। मोदी की लायी नोटबंदी के दौरान अपनी नौकरी गंवाने के बाद और फिर कोविड के चलते लगाए गए अमानवीय लॉकडाउन के बावजूद वे मोदी के वफादार प्रशंसक बने रहे। पिछले हफ्ते जब उन्होंने फांसी लगायी, उससे एक दिन पहले तक वे अपने नायक मोदी की तारीफ कर रहे थे। वाकई, मरते दम तक वे भक्त बने रहे।
क्या साहित्य को ‘राजनीतिक’ होना चाहिए, इस विषय पर अमेरिका में पिछले साल एक संवाद हुआ था। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? चूंकि आप गल्प और निबंध दोनों लिखती हैं, तो क्या आपको लगता है कि दोनों एक ही राजनीतिक पायदान पर रखे जा सकते हैं या फिर गल्प व कथेतर के लिए अलग-अलग नियम हैं?
इस बहस में कुछ भी नया नहीं है। घूम-फिर कर वही बहस बार-बार आ जाती है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उद्धरण चिह्न में ‘राजनीतिक’ को इंगित किया है, क्योंकि यह बताने वाला कौन है कि क्या राजनीतिक है और क्या नहीं? आखिरकार, हम जो लिखते हैं उसमें अपने हिसाब से तमाम चीजें चुनते हैं- मसलन, हमें क्या प्रेरित करता है और क्या नहीं, क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, हमें किन चीजों को शामिल करना है और किन्हें छोड़ देना है… यही चीजें मिलकर हमारी राजनीति को उभारती हैं। यही बात प्रकाशकों पर भी लागू होती है। इस सवाल पर विचार करना तो बाद की बात है, इसे जायज़ मानने की सुविधा भी खाये पीये अघाये तबकों, जातियों, नस्लों और लिंग वाले लोग ही वहन कर सकते हैं अन्यथा बाकी के लिए तो कोई विकल्प ही नहीं है- चूंकि राजनीति हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में, यहां तक कि हमारे बिस्तर में और हमारी देह तक में घुसपैठ कर चुकी है।
इस पर गहराई से सोचने वाले किसी भी व्यक्ति को इमानी पेरी की जीवनी ‘’लुकिंग फॉर लॉरेन: दि रेडिएंट एंड रेडिकल लाइफ ऑफ लॉरेन हैंसबेरी’’ ज़रूर प़ढ़नी चाहिए। लॉरेन हैंसबेरी एक लेखिका थीं, अच्छी दोस्त थीं और जेम्स बाल्डिन की संरक्षक रही थीं। जहां तक आपका यह सवाल है कि गल्प और कथेतर के लिए अलग-अलग विधान होने चाहिए या नहीं- इस बारे में मैंने अपनी हालिया किताब ‘आजादी’ में थोड़ा विस्तार से लिखा है। कुल मिलाकर मैं केवल यह कह सकती हूं कि एक ही नियम हैः दोनों जितने बेहतर हों उतना बढि़या। खराब कला के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है- सही राजनीति भी नहीं।
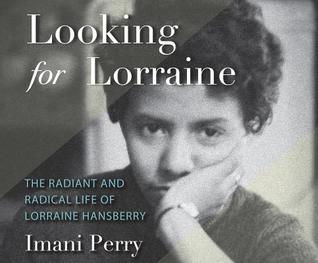
आपने पिछले साल इसी समय लिखा था कि महामारी एक पोर्टल है और यह कि “हम अपने पूर्वाग्रहों और नफरतों के पंजर, अपनी कृपणता, अपने डेटा बैंक और अपने मृत विचार, अपनी मरी हुई नदियों और धुंध भरे आकाश को पीछे छोड़ कर इसके साथ-साथ चलना चुन सकते हैं। या फिर हम हल्के कदमों से, थोड़े कम सामान के साथ, एक अलग दुनिया की कल्पना करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए लड़ने को तैयार रह सकते हैं।” मैं थोड़ा उत्सुक हूं इस बात को लेकर कि हमने (चाहे जैसे भी आप ‘हम’ को परिभाषित करें) अपने लिए इसमें से क्या चुना है? दूसरे तरीके से कहें तो, क्या आपको लगता है कि हमने महामारी से कुछ सीखा है?
हम अब भी उसी पोर्टल पर आगे बढ़ रहे हैं। हम वहां से बाहर नहीं निकले हैं। हम अभी तक यह नहीं जानते कि इस कहर का परिणाम क्या होगा। इसीलिए मैंने अपने निबंध में ‘हम’ शब्द का इस्तेमाल एक अलंकार के रूप में किया था- ‘हम’ का मतलब मानव जाति। यह महामारी एक एक्स-रे के जैसी है जिसने हमारी घनघोर अन्यायपूर्ण दुनिया की भयावह, सर्वांगिक, संस्थागत दरारों को उघाड़ कर रख दिया। मैं निश्चित रूप से मानती हूं कि उम्मीद अब भी बाकी है क्योंकि कोविड-19 के चलते मनुष्य को जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा झेलनी पड़ी है वह उसे अपने जीवन, मूल्यों, चाहतों और इच्छाओं का पुनर्मूल्यांकन करने को बाध्य करेगी। सरकारों, विशाल प्रौद्योगिकीय प्रतिष्ठानों या बैंकों के बारे में यह बात मैं नहीं कह सकती, लेकिन उपभोक्तावाद से अब तक संचालित होता आया मानव समाज अगर अचानक ठहरकर क्षण भर के लिए भी कुछ सोचता है, तो यह वास्तविक बदलाव को प्रेरित कर सकता है। दूसरा रास्ता यह होगा कि हम अमेजॉन ट्विटर की निगरानी वाली दुनिया में ज़ॉम्बी की तरह टहलते हुए चुपचाप प्रवेश कर जाएं।
और अंत में, भारत में रहते हुए (या कहीं भी) दूसरी दुनिया की कल्पना कैसी दिखती है?
हमें उसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। हमें उसकी तलाश करनी होगी क्योंकि वह दुनिया पहले से मौजूद है।
एमिली टैमकिन न्यू स्टेट्समैन यूएस की संपादक हैं। वे साप्ताहिक ग्लोबल अफेयर्स पॉडकास्ट वर्ल्ड रिव्यू की सह-प्रस्तोता हैं। कवर तस्वीर मूल लेख से साभार प्रकाशित है।




