 |
| व्यालोक |
हमारे समाज में एक बड़ी मजेदार बात है। दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक में फिल्म निहारने जाती ‘कूल’ जनता हो या दरभंगा के वीडियो हॉल नुमा सिनेमाघरों में जाने वाली ‘आम’ जनता, जेनरलाइजेशन इसका प्रिय शगल है। यही बात हाल ही में फिर दिखी, जब ‘तलाश’ देखने के लिए प्रतीक्षारत जनता पहले से ही निर्णय सुना रही थी- ‘आमिर के फिलिम हउ, त अच्छे होतइ…’, ‘तीन साल बाद आया है, बढ़िया फिल्म ही देगा…’, ‘आमिर कोई सलमान-शाहरुख-अजय-अक्षय थोड़े न है, फिल्म तो भाई बनाता है, क्लास की…’।
इन सारी टिप्पणियों को सुनने के बाद मैं जब फिल्म देखकर हॉल से निकला, तो ऊपर उल्लिखित जनता-जनार्दन से पूछने की इच्छा हुई, ‘भाई लोग, नाम का इतना खौफ किसलिए? आमिर भी आखिर इंसान हैं, वह भी सहम सकते हैं, फेल (हिंदी के असफल में वह मज़ा नहीं आयेगा) हो सकते हैं।’ इतनी भूमिका के बाद ‘तलाश’ के बारे में मैं एक समीक्षक की बात से बिल्कुल सहमति जताऊंगा कि क्या हम इसे थ्रिलर मान भी सकते हैं? बारहां, तो यह धीमी, लचर, बोर और ऊंघने की दिशा में ले जाती दिखी।
हालांकि, मैं यहां जो बात कहने जा रहा हूं, वह ‘तलाश’ के बहाने दरअसल मुंबइया/हिंदी/बॉलीवुड फिल्मों की दशकों पुरानी रवायत है, जहां स्टीरियोटाइपही मौलिकता है, दोहराव ही अनूठापन है और क्लिशे ही हीरोइक है।
‘तलाश’ बनाने वाली टीम को देखें। इसमें सभी नव-समृद्ध, नव-सांस्कृतिक, पश्चिमी तरीके में पूरी तरह रंगे- और उससे आक्रांत भी- अंग्रेजीदां लोग हैं- रीमा कागती, ज़ोया अख्तर, फ़रहान अख्तर, आमिर खान वगैरह। इन सबको एक भ्रम भी है- अपनी पहचान को लेकर- और ये सभी खुद को अचानक ही सांस्कृतिक और बौद्धिक जगत के अलमबरदार, पहरुए और स्वयं को जागृत तौर पर अलहदा और अनूठा मानते हैं। पर ‘हा हुसैन हम न हुए’ की तर्ज पर अगर कहें, तो इन सबकी बुनियादी दिक्कत यही है कि एक सीमा से निकलने के बाद इनको भी back to square one ही होना है। जोखिम की हद तक ये जोखिम कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनकी जड़ें हैं ही नहीं। ये अभिशप्त हैं, क्योंकि इनके पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं है।
बात को ज़रा सा खोलकर कहूं।
 ‘तलाश’ बुनियादी तौर पर ‘द सिक्स्थ सेंस’, ‘द किड’ और कुछ ऐसी ही अन्य हॉलीवुड की फिल्मों के साथ ही ‘एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस’ नामक उपन्यास पर आधारित एक ढीली-ढाली फिल्म है। हालांकि, रीमा कागती इसे नहीं मानेंगी, लेकिन क्या हिमेश रेशमिया, प्रीतम जैसों ने माना है कि वे सर्जनात्मक चोरी करते हैं?
‘तलाश’ बुनियादी तौर पर ‘द सिक्स्थ सेंस’, ‘द किड’ और कुछ ऐसी ही अन्य हॉलीवुड की फिल्मों के साथ ही ‘एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस’ नामक उपन्यास पर आधारित एक ढीली-ढाली फिल्म है। हालांकि, रीमा कागती इसे नहीं मानेंगी, लेकिन क्या हिमेश रेशमिया, प्रीतम जैसों ने माना है कि वे सर्जनात्मक चोरी करते हैं? बहरहाल, यहां सवाल रीमा कागती के आखिरकार फॉर्मूले की शरण में जाने और आमिर के घुटने टेकने का है। भूत-प्रेत और आत्मा का जादू जगाने वाली यह फिल्म उसका लॉजिकल कन्क्लूजन नहीं दे पाती। रीमा जिस स्कूल की देन हैं, वह मोटे तौर पर अमेरिकी नव-पूंजीवाद का उत्पाद है, वहां मनोरोगों को कोई भी ‘एट हिज/हर स्ट्राइड’ लेता है। मनोचिकित्सक के पास जाना कोई बहुत बड़ा अपराध या चौंकाऊ घटना नहीं मानी जाती, वह एक आम घटना है। वहीं, भारत में अब भी बहुत पढ़े-लिखे और तथाकथित आधुनिक तबके में भी अगर कोई मनोचिकित्सक के यहां कदम भी रख देता है, तो उसे पागल घोषित करते देर नहीं लगती, मिर्गी का दौरा आने या यूं ही बेहोशी आने पर भी जूता सुंघाने की कवायद की जाती है। यह एक सामाजिक तथ्य है, सोशल कंस्ट्रक्शन है और रीमा को यह सच्चाई पता है। आखिर, अंग्रेजी में हगने-मूतने और सोचने वाला यह तबका खाता तो हिंदी और हिंदी-पट्टी की अंडरबेली की ही है, इसलिए कुछ सच्चाइय़ां तल्ख होते हुए भी इसे पता हैं।
यही वजह है कि ‘द किड’ में ब्रूस विलिस के किरदार को जहां एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या दी जाती है, वहीं ‘द सिक्स्थ सेंस’ में निर्देशक पूरी तरह आत्मा-परमात्मा का ही आख्यान करता है- ऑल-आउट ऑफेंसिव, कोई टट्टी ओट शिकार नहीं। रीमा को मुंबइया फिल्म इंडस्ट्री के बंधे-बंधाए नियमों के छिलके पर ही फिसलना पड़ता है और वह (साथ में आमिर, द परफेक्शनिस्ट भी) आत्मा की दुहाई देने लगती हैं, कोई मनोवैज्ञानिक तर्क या संगति नहीं दे पातीं।
यहां उद्देश्य रीमा के इंस्पिरेशन या भटकाव की कलात्मक व्याख्या नहीं है। मसला, यहां उस पूरे रचना-विधान और कौशल का है, जो किसी भी तरह की मौलिकता और सर्जनात्मकता को सिरे से खारिज करती है। बंधे-बंधाए फॉर्मूलों और अंधविश्वासों की फुटेज पर जब सामूहिक ऑर्गी में व्यस्त हों, तो रचनात्मकता का शीघ्रपतन बहुत ही लाजिमी है। वैसे भी, आज जो भी है, सब कल (यस्टरडे) का दुहराव ही तो है। आपके साहित्य से लेकर फिल्म नॉयर तक। तो फिर, काहे का मर्सिया और काहे का हा, हुसैन!!!
Read more

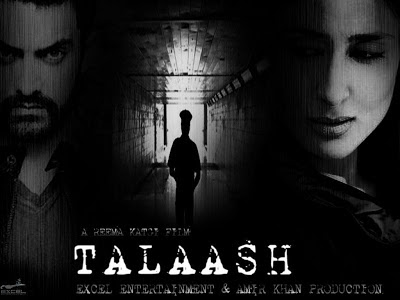



मुझे तो फिल्म अच्छी लगी… बाकी सबका अपना अपना नजरिया… 🙂 3.5/5.0
बढ़िया लिखा व्यालोक भाई।।।
अभिषेक जी. आप की बातों से पूर्ण सहमत हूँ. पर जोड़ना चाहूँगा की तीनो मुख्य कलाकार ने अभिनय में कोई कसर नहीं छोड़ी है.