विश्वप्रसिद्ध रचना ‘रॉबिन्सन क्रूसो’ के लेखक डैनियल डेफो, (1660 -1731) बहुआयामी किस्म के व्यक्ति थे, व्यापारी थे, पत्रकार थे, लेखक थे, पर्चे भी लिखते थे। लंदन के निवासी रहे डैफो ने उनके जमाने में आए प्लेग की महामारी – जिसमें हजारों लोग मर गए थे – पर बाकायदा एक लम्बा पर्चा लिखा है- ‘ए जर्नल आफ द इयर आफ द प्लेग’, जो वर्ष 1722 में प्रकाशित हुआ था।
महामारी के दिनों में लोगों का व्यवहार, सामाजिक व्यवहार तथा प्रशासन के स्तर पर कैसे चीजे़ं चलती हैं, इसके बारे में वह अपना अवलोकन प्रस्तुत करते हैं वह अपने आप में दिलचस्प है। सरकारें किस तरह असली स्थिति से लोगों को अवगत कराने से बचती हैं, गलत आंकड़ें पेश करती हैं, इसका भी वह वर्णन करते हैं, किस तरह बीमारी के लिए ‘अन्य’ को जिम्मेदार ठहराती हैं, इसकी भी वह बात करते हैं।
इस रिपोर्ट के अंश को पलटते हुए बरबस कोविड महामारी से निपटने में सरकारी प्रयासों की खामियों की याद आना स्वाभाविक है।
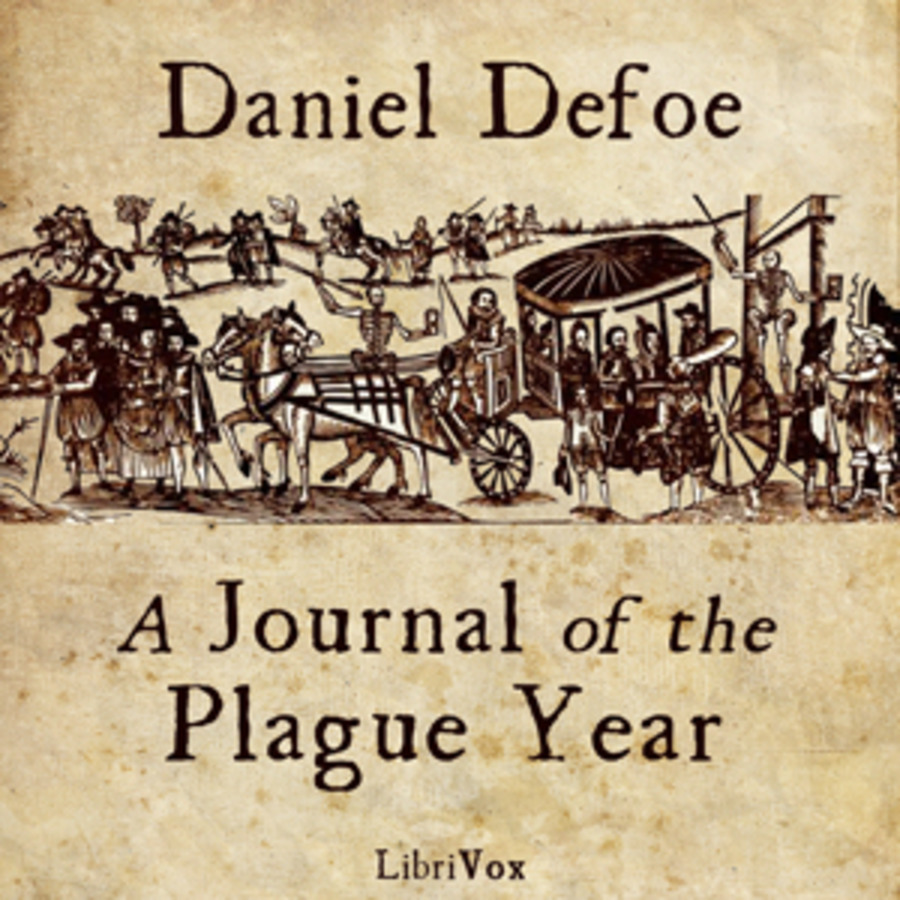
फिलवक्त़ यह तो पता नहीं कि क्या 17वीं सदी के ब्रिटेन में भी ऐसे ‘अन्य’ कहे गए लोगों पर – समुदायों पर मुकदमे चलाए गए थे या नहीं या उन्हें निशाना बना कर प्रताडि़त किया गया था नहीं, लेकिन 21वीं सदी के भारत में तो कोविड महामारी ने ऐसे नज़ारों को बहुत देखा, जब समुदाय विशेष पर इसका लांछन लगाया गया, उससे जुड़े लोगों को प्रताड़ना का शिकार बनाया गया।
तबलीगी जमात को कोविड महामारी के सुपर स्प्रेडर के तौर पर चिन्हित करने की चंद माह पहले चली उस बहस की ओर मुड़ कर देखें, जब किस कदर लोगों के एक हिस्से को निशाना बनाया गया और अब वह समूची बहस इतिहास का हिस्सा बना दी गयी है।
यह उसी उदासी का ही प्रतिबिम्बन है कि तबलीगी जमात के सम्मेलन में शामिल होने आए छत्तीस विदेशियों को रिहा करते हुए दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मैजिस्टेट ने दिल्ली पुलिस के बारे में जो तीखी बातें कहीं उस पर मौन ही बना रहा। मालूम हो कि दिल्ली में तबलीगी जमात के सम्मेलन में आए इन विदेशियों पर कोविड के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था और संक्रमण में विस्फोट के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था।
फैसला देते हुए मैजिस्ट्रेट ने इस संभावना को रेखांकित किया कि मुमकिन हो कि “पुलिस ने इन लोगों को दुर्भावना से प्रेरित होकर पकड़ा हो तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत फंसाना चाहा हो।’’
[p]olice picking up these individuals with the malicious intention of implicating them under the directions of the Union home ministry.
निश्चित ही यह कोई पहला मौका नहीं था कि अदालतों ने कोरोना संक्रमण के लिए संस्था विशेष या समुदाय विशेष से जुड़े लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाने को लेकर अपनी घोर असहमति प्रकट की हो।
समुदाय केन्द्रित कोरोना मैपिंग का प्रश्न? नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट!
मुंबई उच्च अदालत की औरंगाबाद पीठ ने तो ऐसे मसले पर सरकार की बुरी तरह भर्त्सना की :
‘‘एक राजनीतिक सरकार ने बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जब एक महामारी या आपदा चल रही थी और परिस्थितियां बता रही हैं कि ऐसी संभावना है कि इन विदेशियों को इसके लिए चुना गया’’
A political government tries to find a scapegoat when there is pandemic or calamity and the circumstances show that there is probability that these foreigners were chosen to make them scapegoats,
सवाल उठता है कि क्या एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने में उनकी कथित भूमिका को लेकर तथा उनके हाशियाकरण को लेकर कभी हुक्मरानों को या उनसे संबंधित तंजीमों को कभी जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा? क्या वह अपने इन कारनामों को लेकर कभी जनता से माफी मांगेंगे?
क्या मीडिया का एक बड़ा हिस्सा- जो इस घृणित मुहिम में शामिल था और जिसने भारत के समावेशी सामाजिक तानेबाने को नुकसान पहुंचाने की काफी कोशिश की, क्या उसे कभी अपनी इन हरकतों के लिए तथा इसके चलते अल्पसंख्यक समुदायों के अधिक हाशियाकरण को मुमकिन बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा?
निश्चित ही नहीं, कम से कम आने वाले भविष्य में।
यह ऐसा वक्त़ है कि विशिष्ट समुदाय के इस खुल्लमखुल्ला ‘अन्यीकरण’ को, किसी धार्मिक संस्था के दानवीकरण को रफ़्ता रफ़्ता सामान्यीकृत किया जा रहा है और इस पर कोई सवाल भी नहीं उठ रहे हैं।
आज आलम यह है कि यह लांछनीकरण, जो पहले विशिष्ट समुदायों तक या समाज के तबकों तक सीमित था या असहमति रखनेवाले विद्वानों एक्टिविस्टों तक सीमित था, वह सिलसिला अब व्यापक जनान्दोलनों तक भी पहुंच गया है जिन्होंने हुकूमत द्वारा पेश किए जा रहे वर्चस्ववादी आख्यान को चुनौती दी है।
राजनैतिक बंदियों की रिहाई तो किसान आंदोलन के माँगपत्र का हिस्सा है, फिर हल्ला किस बात का?
तीन दमनकारी फार्म बिलों के विरोध में खड़े ऐतिहासिक किसान आन्दोलन को देखें।

एक माह से अधिक वक्त़ बीत गया जब लाखों किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे हैं ताकि इन दमनकारी कानूनों को सरकार वापस लें, जिनके जरिये उन्हें लगता है कि इस हुकूमत ने एक तरह से उनकी तबाही और बरबादी के वॉरंट पर दस्तख़त किए हैं। किसानों के इस शांतिपूर्ण आन्दोलन को देशभर में भी समर्थन मिल रहा है। देश के कोने कोने में इस मसले पर किसान और उनकी मित्र शक्तियां संघर्षरत हैं।
सरकार के अपने जो भी दावे हों कि यह तीनों कानून – जिन्हें महामारी के दिनों में पहले अध्यादेश के जरिये जारी किया गया था और जिन्हें तमाम जनतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रखते हुए संसद में पास किया गया- किसानों की भलाई के लिए हैं, लेकिन यह सभी के लिए साफ हो रहा है कि इनके जरिये राज्य द्वारा अनाज की खरीद की प्रणाली को समाप्त करने और इस तरह बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए ठेका आधारित खेती का रास्ता सुगम करने, उन्हें आवश्यक खाद्य सामग्री की बड़ी मात्रा में जमाखोरी करने के रास्ते सुगम किए जा रहे हैं। लोगों के लिए यह भी साफ है कि यह महज किसानों का सवाल नहीं है बल्कि इसके जरिये करोड़ों मेहनतकश अवाम के लिए अनाज की असुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो रहा है।
इसके बजाय कि सरकार इन आंदोलनरत किसानों के साथ एक सार्थक वार्ता करे उसकी तरफ से इस आन्दोलन के दमन तथा उसके विकृतिकरण की तमाम कोशिशें चल रही हैं। एक दिन भी नहीं बीतता जब इस आन्दोलन को बदनाम करने के लिए सरकार की तरफ से कोई नया शिगूफा, कोई नयी गाली नहीं उछाली जाती। किसानों को ‘खालिस्तान समर्थक’, माओवादी से लेकर ‘अर्बन नक्सल’ और राष्ट्रद्रोही या फर्जी किसान क्या-क्या नहीं कहा जा रहा है।
दरअसल, यह इस आंदोलन की अंदरूनी ताकत थी और न केवल भारत के स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर उसे मिले व्यापक समर्थन का मसला था कि यह तमाम गालियां, यह विकृतिकरण तूल नहीं पकड़ पाया और हुकूमत को अपनी जुबां बदलनी पड़ी। अब उसकी तरफ से एक नया शिगूफा और छोड़ा गया है कि यह दरअसल विपक्ष द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। यह अलग बात है कि किसानों के साझे मोर्चे ने बार बार साफ किया है कि किसी भी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है।
आर्टिकल 19: मुंह छुपाये गिद्धभोज की ताक में मीडिया और सरकार की छाती पर रोटी दलता किसान
अपनी उन पुरानी रणनीतियों को असफल होते देख कर – जिसका इस्तेमाल उन्होंने सीएए विरोधी आन्दोलन के दमन के लिए किया था – और इस बात को मददेनज़र रखते हुए कि देश की उच्चतम अदालत ने भी शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करने के लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों पर जोर दिया है, सरकार अपने आप को एक दुविधा की स्थिति में देख रही है।
और इस मसले पर राष्ट्रव्यापी चर्चा को रोकने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, वह अधिक चिन्तनीय है। उन्होंने कोविड के नाम पर संसद के शीतसत्र को रद्द किया है। इसके लिए जो तर्क उन्होंने दिया है वह कम विवादास्पद नहीं है।
यह सही ही पूछा जा रहा है कि अगर कोविड महामारी के दिनों में सरकार विधानसभा के चुनावों को तथा अन्य स्थानों पर स्थानीय चुनावों को इजाज़त दे सकी, तो फिर संसद सत्र बुलाने में उसे अचानक आपत्ति क्यों दिखी? गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनावों की जब चर्चा चल पड़ी थी तब प्रमुख विपक्षी पार्टी की तरफ से उन दिनों यह मांग की गयी थी कि कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए चुनाव को टाला जाए, लेकिन सरकार ने चुनावों को होने दिया था।
नागरिकों को ही ‘विपक्ष’ का विपक्षी बनाया जा रहा है!
एक तरफ सरकार यह दावा करती है कि जीवन सामान्य हो चला है, सितम्बर माह में – कोविड के बावजूद उसने संसद सत्र का आयोजन किया (उसे छोटा किया गया और सवाल जवाब का सत्र भी समाप्त किया गया) – तब दिसम्बर माह में संसद सत्र को रद्द किया जाना इसी बात को दर्शाता है कि वह किसानों के ऐतिहासिक किस्म के जनान्दोलन से उठी चर्चाओं से बचना चाहती है। याद रहे विगत एक माह से जारी इस आन्दोलन ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पश्चिमी मुल्कों में भी समर्थन की एक लहर पैदा की है, केन्द्र सरकार के तमाम सहयोगी दलों में भी सरकार के इस अडियल रवैये को देख कर बेचैनी पैदा की है तथा कुछ पार्टियों ने उसका साथ भी छोड़ा है।
यह भी पूछा जा रहा है कि महामारी के दिनों में अध्यादेश के तौर पर जारी कृषि विधेयकों पर चूंकि संसद की मुहर लगानी थी इसलिए सितम्बर में सत्र आयोजित किया गया और आज की तारीख में जब इन बिलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आक्रोश उमड़ पड़ा है, सरकार ने इयीलिए संसद सत्र को टाल दिया है ताकि वह उससे उभरे सवालों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होने से बचे।
मालूम हो कि कृषि बिलों के बहाने यह धारणा जनसाधारण में बलवती हो रही है कि सरकार को अपने खासम खास गिने चुने पूंजीपतियों की – अडानियों और अंबानियों की ही फिक्र है और उसे मेहनतकश जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को इस बात का भी अंदाज़ा रहा होगा कि अगर संसद सत्र होता तो उसे चीन के मुद्दे पर भी असहज होना पड़ता।
आर्टिकल 19: क्या आप जानते हैं कि भारत ने ‘लोकतंत्र’ के रूप में अपनी स्थिति लगभग खो दी है?
याद रहे कि पड़ोसी मुल्क चीन द्वारा देश के सीमावर्ती इलाकों में कथित तौर पर की गयी घुसपैठ की जो ख़बरें आ रही हैं, ऐसी ख़बरें जिन्हें मुख्यधारा के मीडिया के एक हिस्से में भी जगह मिली है, उसे लेकर भारत सरकार की एक किस्म की उदास प्रतिक्रिया का मुद्दा भी संसद के शीतकालीन सत्र में जोरदार ढंग से उभरता।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपने एक व्याख्यान में जनतंत्र के तीन ‘डी’ की बात की थी। उनके मुताबिक डिबेट (बहस मुबाहिसा, डिसेन्शन (असहमति) और डिसीजन (निर्णय) लोकतंत्र के तीन ‘डी’ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बहस मुबाहिसा, असहमति और निर्णय, यह तीनों जनतंत्र की आत्मा हैं।
सवाल उठता है कि उस जनतंत्र का क्या स्वरूप बचता है जब बहस मुबाहिसे को सचेतन तौर पर स्थगित किया जाता है, असहमति पर अधिकाधिक लांछन लगाया जाता है और निर्णयों को अधिकाधिक केन्द्रीकृत किया जाता है?
बात बोलेगी: ‘ज़रूरत से ज्यादा लोकतंत्र’ के बीच फंसा एक सरकारी ‘स्पेशल पर्पज़ वेहिकल’!
‘नीति आयोग’ के सीईओ अमिताभ कांत के उस विवादास्पद वक्तव्य, कि भारत में ‘‘अत्यधिक जनतंत्र है’’ के विपरीत यही देखने में आ रहा है कि हम जनतंत्र के अधिकाधिक संकुचन की दिशा में, भारत के ‘‘कम जनतंत्र’’ होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं।
मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से भारत के ‘नए इंडिया’ में प्रवेश की बात का ढिंढोरा अक्सर पीटा जाता है। अब यही कहना मुनासिब होगा कि यह ‘नया इंडिया’ जनतंत्र के अधिकाधिक संकुचन की और रफ़्ता-रफ़्ता अधिनायकतंत्र की तरफ उन्मुख होने की यात्रा का प्रत्यक्षदर्शी बनता दिख रहा है।





