कुमार अम्बुज हाल में कुसुमाग्रज सम्मान से सम्मानित हुए हैं। कुसुमाग्रज मराठी भाषा के बहुत बड़े कवि और उससे कहीं बड़े मनुष्य थे। बंगाल में जैसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर, गुजराती में मकरंद भाई दवे और कुंदनिका बहन, मराठी में कुसुमाग्रज आदि प्रसिद्ध लेखकों ने साहित्य सृजन के साथ आंदोलनकारी और सामाजिक क्रांति में सहभाग करने की भूमिका भी निभायी। हिन्दी में भी अवश्य ही ऐसे उदाहरण होंगे लेकिन ऐसा कम ही सुनने में आया है। उम्मीद करते हैं कि हिन्दी में भी नवजागरण की वह अवस्था जल्द आएगी, जब हिन्दी के साहित्यकार, कलाकार भी उस वैकल्पिक समाज के उपकरण तैयार करने में भागीदारी करते दिखेंगे जिस वैकल्पिक समाज का हम स्वप्न देखते हैं।
लेकिन तब तक जो समाज है, उसकी वस्तुगत दृष्टि से निर्मम पड़ताल करने का कार्यभार एक महत्त्वपूर्ण दायित्व है जो हिन्दी के साहित्यिक – सांस्कृतिक समुदाय पर है। हम हिंदी के पाठक और रचनाकार इस बात के लिए ख़ुश हो सकते हैं कि हमारे पास नागार्जुन, रघुवीर सहाय, विष्णु खरे और चंद्रकांत देवताले आदि कवियों की धरोहर है और वर्तमान में हमारे पास कुमार अम्बुज जैसे कवि हैं, जिन्होंने अपने इस सांस्कृतिक-सामाजिक दायित्व को कभी अनदेखा नहीं किया।
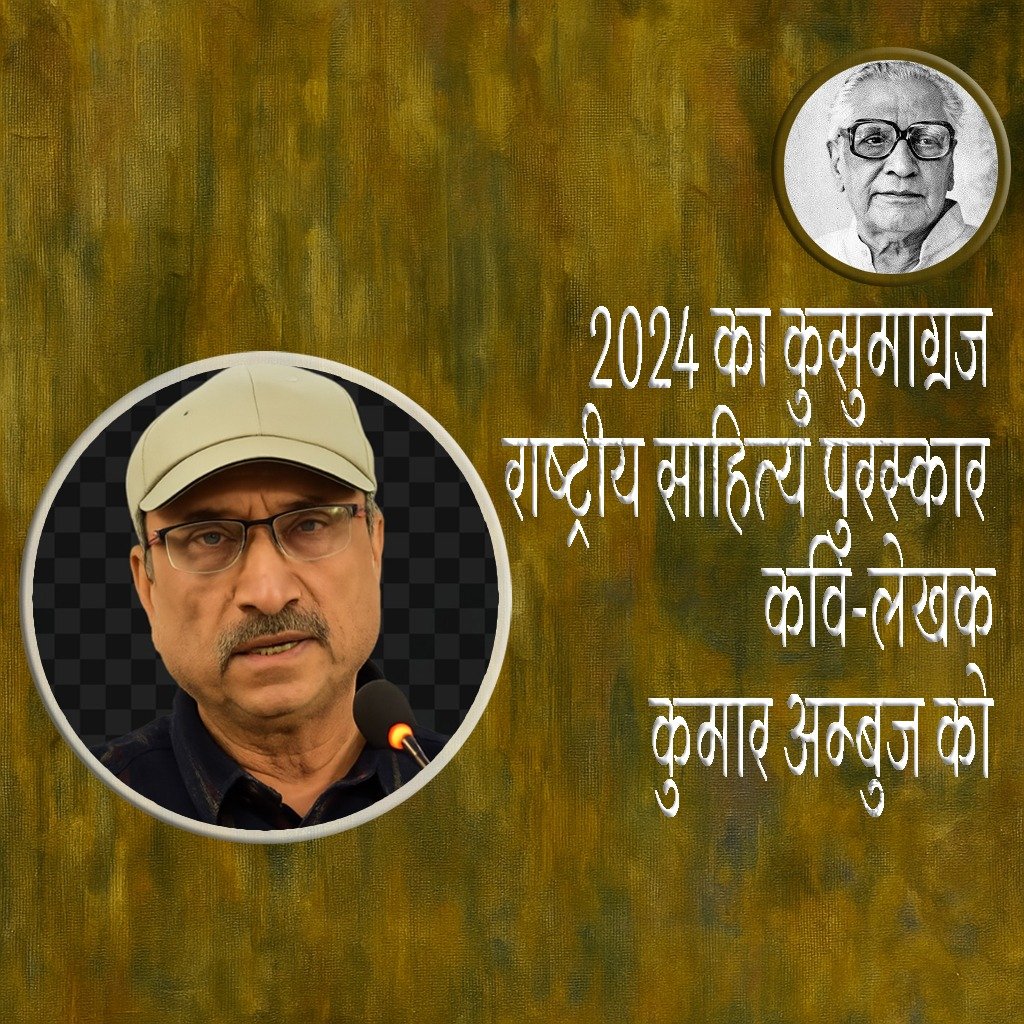
कुमार अंबुज के अब तक “किवाड़”, “क्रूरता”, “अनंतिम”, “अतिक्रमण”, “अमीरी रेखा” शीर्षक से कविता संग्रह, “इच्छाएँ” और “मज़ाक़” शीर्षक से कहानी संग्रह और दो किताबें कथेतर गद्य की आयी हैं। केरल के विश्वविद्यालयों में उनकी कविताएँ पाठ्यक्रम में हैं। उनकी अनेक कविताओं के अनुवाद भी अनेक हिंदीतर भारतीय भाषाओं में और अन्य विदेशी भाषाओं में हुए हैं। हिन्दी के भीतर भी उनका एक व्यापक, संलग्न और उत्सुक पाठकवर्ग है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय और विदेशी फ़िल्मों के एक सजग दर्शक और पाठक के तौर पर अनेक लेख लिखे हैं। उनकी भी पुस्तक आने वाली है। एक लेखक के तौर पर उन्होंने परिमाण में और गुणवत्ता में उल्लेखनीय लिखा है। बहैसियत प्रगतिशील लेखक संघ के संगठक भी उनका कार्य उल्लेखनीय है। अभी भी वे आधुनिक हिन्दी कविता को समझने-समझाने के शिविरों में उत्सुकता और तैयारी के साथ शामिल होते हैं और नयी जानकारियों और दृष्टिकोणों का खुले दिल से स्वागत भी करते हैं।
उनके रचनात्मक जीवन का एक भाग इंदौर में भी बीता है और बाद में वे भोपाल में रह रहे हैं। एक महानगर बनते शहर में घुटती जाने वाली बारीक ध्वनियों को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में दर्ज किया है। महानगरों में छा जाने वाले अकेलेपन को तोड़ने के प्रयास भी उनके सांस्कृतिक कर्म का अविभाज्य हिस्सा हैं। वे जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ सामूहिकता, आत्मीयता, दोस्तियाँ और परस्पर सम्मान रोज़मर्रा के जीवन के भी लगभग अनिवार्य हिस्से होते हैं और रचनात्मकता के भी। उन्होंने लिखना जब शुरू किया तब इन सब अनिवार्यताओं पर संकट की छाया गहराने लगी थी। हर तरह का कुहासा बढ़ने लगा था – राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सभी तरह का। ऐसे में संस्कृतिकर्मी, एक कवि जो कर सकता था, वह उन्होंने भी किया।
उन्होंने रेल की पटरी पर कान धरकर सुनने की कोशिश की कि वेगवान समय कितनी दूर है और और उतनी देर में सजग लोग क्या तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुराने किवाड़ अब और धक्का मज़बूत नहीं कर सकेंगे इसलिए लड़ने की व्यूह रचना होनी होगी। जब देश-समाज और उसकी राजनीति अगले चरण में दाखिल हुई तो उन्होंने और उनके अग्रजों और समकालीन कवियों ने उस क्रूरता की भी पहचान की जो धीरे-धीरे बिना पहचान के हममें से एक बनकर हममें से हर एक में शामिल होती जा रही थी और जिसका पता देर तक लगने वाला नहीं था। पहले ही जातियों में विभक्त समाज को मंदिर-मस्जिद के आधार पर और ज़्यादा विभाजित करने वाली घटनाओं ने जब विस्फोटों की शक्ल अख्तियार कर ली तब कुमार अम्बुज ने फिर से अपने समाज को याद दिलाया कि यह दिखने वाला विभाजन कोई वास्तविक सांप्रदायिक या धार्मिक पहचानों का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी हुई है एक अमीरी रेखा जो तीखी धार वाली तलवार की तरह समाज को तहस-नहस करती जा रही है।
एक पाठक के तौर पर मैं यह कहने की भी छूट लेना चाहता हूँ कि कुमार अम्बुज की शुरुआत की कविताओं के पढ़ते हुए मुझे एक शांत जीवन वाले गाँव में जहाँ नीम और बरगद के पेड़ों की छाँह और बाज़ दफ़ा बनैले पशु भी दिख जाते हैं, वहीं उनकी बाद की कविताएँ तेज़ रफ़्तार भागते जीवन में मोबाइल, इंटरनेट और सूचनाओं के तमाम घटाटोप के बाद भी किसी को हाथ पकड़कर पास बिठा लेने की, थोड़ी बात करने की और इस अकारण रफ़्तार के ख़िलाफ़ थोड़ा ठहरकर सोचने के लिए, एक गिलास पानी पीने के लिए, एक कविता सुनने के लिए, पेड़ का हरापन देखने के लिए, चिड़िया की आवाज़ सुनने के लिए और इस तरह थोड़ा ख़ुद के साथ समय बिताने की अभ्यर्थना भी हैं।
लेकिन इस सबको करते हुए जो चीज़ उनके जीवन और कविता में अपने आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ी मिलती है – वह है विचारधारा। वह अलग से पहचानी जा सकने वाली चीज़ नहीं, वह कोई नारा नहीं, चीत्कार, आर्तनाद भी नहीं, वह अक्षरों की स्याही में मौजूद काला रंग है और वह कविता के आयतन से बची पन्ने की जगह का सफ़ेद भाग है। उसे हम आकाश, अवकाश या ज़रूरी खाली जगह भी कह सकते हैं। वह इतनी वाचाल भी नहीं कि जगह-जगह अनचाहे सुर की तरह खटके और इतनी अदृश्य भी नहीं कि अपने होने का स्पष्ट भान न करा सके। इसलिए यह कविताएँ दो स्तरों पर आवश्यक हैं उन सभी के लिए जो संस्कृति को एक महत्त्वपूर्ण अन्विति मानते हैं और जो यह मानते हैं कि एक बेहतर दुनिया के लिए बेहतर राजनीति ज़रूरी है और बेहतर राजनीति के लिए बेहतर संस्कृति। मैं यहाँ एक ही उदाहरण देना उचित समझता हूँ कि जैसे धूमिल की मोचीराम कविता पढ़ते हुए पाठक को अलग से यह बताने की जरूरत नहीं रह जाती है कि श्रम का सम्मान करना चाहिए और जातिवाद को तोड़ना चाहिए। वैसे ही कुमार अंबुज की अनेक कविताएँ पढ़ने के बाद पाठक को पूँजीवाद, सांप्रदायिकता, उपभोक्तावाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद आदि के बारे में अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं या कम रह जाती है। लेकिन यह तो उपयोगितवादी दृष्टि हुई। कुमार अंबुज की कविताएँ उससे ज़्यादा बड़ा काम करती हैं: वे हमें बताती हैं कि अभी भी हम कहाँ और बेहतर मनुष्य बन सकते हैं, केवल कविता और साहित्य में नहीं, अपनी नज़रों में भी।
इस लिहाज से भी उनकी उपस्थिति महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें इस बारे में संशय नहीं रहता कि यहाँ जाना ठीक है और यहाँ नहीं जाना चाहिए। यह भी नहीं कि मैं लोकप्रिय मंच या श्रोताओं, पाठकों की विशाल संख्या को देखकर सोचूँ कि मेरे विचार को अधिक प्रभावी बनाने में अमुक स्थान का उपयोग करने में कोई हर्ज नहीं। उनके पास प्रतिबद्धता एक शब्द नहीं, जीवन की शर्त है और विचारधारा का आग्रह बाहर से चस्पा ज़िद नहीं, सहज विनम्रता का पर्याय है।
ग़लती उनसे भी हो सकती है लेकिन वह उसे वैधता दिलाने की कोशिश नहीं करते जो अक्सर भोलेपन के आवरण में सुविधा को छिपाने की कोशिश से पैदा होती है। वे जानते हैं कि सब उन्हें कवि की अकड़ और चुनाव की वजह से नहीं करते हैं प्यार, लेकिन कुछ इस वजह से भी करते हैं उन्हें प्यार, और किस् प्यार का करना चाहिए सम्मान, यह वह जानते हैं। और उनके बिना किये और बिना चाहे भी उनका जीवन किसी के लिए कुहासे को चीरती रोशनी की लकीर बन जाता है, तो किसी के लिए असुविधाजनक अवरोध।
तो ऐसे कवि और बहुत प्यारे दोस्त कुमार अम्बुज को कुसुमाग्रज सम्मान मिलने की बहुत बधाई। और मराठी के सदाशयी साहित्यिक समाज को भी बहुत बधाई, जिन्होंने ग़ैर मराठी भाषायी कवियों के लिए यह पुरस्कार स्थापित कर भाषा की पुल की भूमिका को सुदृढ किया है। ऐसा हिंदी एवं अन्य भाषाओं में भी किया जाना चाहिए।
इस अवसर पर मेरी पसंद की उनकी एक कविता का अंश:
“कवि की अकड़”
एक वही है जो इस वक़्त में भी अकड़ रहा है
जब चुम्मियों की तरह दिए जा रहे हैं पुरस्कार
जैसे देती हैं अकादेमियाँ और पिताओं के स्मृति-न्यास नाना-प्रकार
जैसे देते हैं वे लोग जिनका कविता से न कोई लेना-देना न कोई प्यार
तो परिषदों, संयोजकों, जलसाघरों के नहीं हैं कोई नियम
और मुसीबजदा होते जाते कवियों का भी नहीं कोई नियम
लेकिन वही है जो कहता है कि आपके देने के हैं कुछ नियम,
तो जनाब,
मेरे लेने के भी हैं कुछ नियम।
…..
आख़िर में कहना चाहता हूँ कि यदि उसकी कविता में
हम सबकी कविता मिलाने से कुछ बेहतरी हो तो मिला दी जाए
यदि बदतरी होती हो तो हम सबकी कविता मिटा दी जाए
लेकिन एक कवि की ठसक को रहने दिया जाए
कि वही तो है जो बिलकुल ठीक अकड़ता है
कि वही तो है जिसके पास कोई अध्यादेश लाने की ताक़त नहीं
कोई वर्दी या कुर्सी नहीं और मौक़े-बेमौक़े के लिए लाठी तक नहीं
फिर भी एक वही तो है जो बता रहा है
कि अकड़ना चाहिए कवियों को भी
इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वह
कविता की बची-खुची अकड़ है
जीवन पर निर्बल की सच्ची पकड़ है।

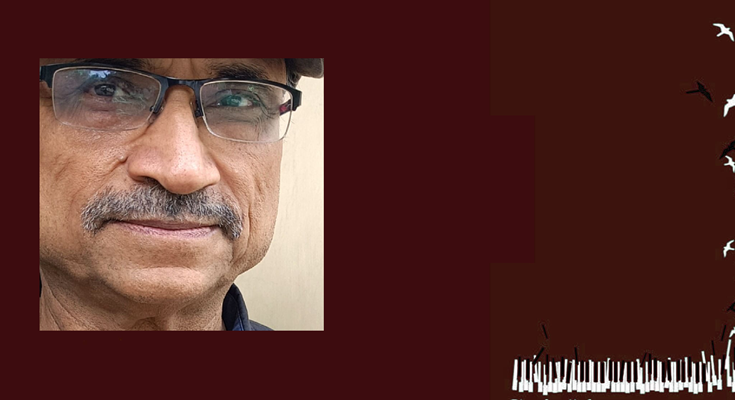



Saw 7700bet777 advertised somewhere. Gave it a quick look. Pretty much what you’d expect. Worth a shot if you’re bored. Head over to 7700bet777.
Всё о камерах видеонаблюдения — полное руководство!
Приветствуем вас, уважаемые форумчане! Сегодня мы подробно поговорим обо всём, что касается видеокамер наблюдения. Мы поможем вам разобраться в огромном разнообразии предложений рынка и сделать правильный выбор оборудования для защиты вашего имущества и безопасности вашей семьи.
Почему важно установить систему видеонаблюдения?
Камеры видеонаблюдения становятся всё популярнее среди владельцев домов, офисов и коммерческих помещений. Они обеспечивают защиту имущества, предотвращают преступления и помогают контролировать происходящее даже дистанционно. Давайте рассмотрим самые важные аспекты выбора камеры и её установки.
Какие бывают виды камер видеонаблюдения?
Вы можете выбрать камеру исходя из ваших потребностей и условий эксплуатации:
– **Уличные** — предназначены для наружной установки, защищены от влаги и пыли.
– **Домашние** — компактные модели для внутренней установки.
– **IP-камеры** — позволяют подключаться к сети Интернет и просматривать записи онлайн.
– **Wi-Fi камеры** — удобны благодаря беспроводному соединению.
– **Камеры с SIM-картой** — работают независимо от интернета, передавая сигнал через мобильную сеть.
– **Миниатюрные камеры** — незаметны и подходят для скрытого наблюдения.
– **Поворотные камеры** — способны охватывать большие площади, поворачиваясь на 360 градусов.
– **Ночные камеры** — оснащены инфракрасной подсветкой для съёмки в темноте.
—
Как правильно выбрать камеру видеонаблюдения?
Перед покупкой обратите внимание на следующие характеристики:
– Разрешение камеры — HD/FullHD/UHD обеспечит чёткое изображение.
– Угол обзора — широкий угол позволяет видеть больше пространства.
– Наличие микрофона и динамика — возможность двусторонней связи.
– Датчик движения — экономия памяти устройства путём включения записи только при обнаружении активности.
– Питание — проверьте совместимость с вашим источником питания.
– Возможность удалённого доступа — управление камерой через смартфон или компьютер.
—
Установка и подключение камеры видеонаблюдения
Правильная установка и настройка камеры позволят вам эффективно пользоваться всеми возможностями системы видеонаблюдения. Рассмотрим ключевые моменты:
– Выберите оптимальное место для размещения камеры, обеспечивающее максимальный обзор охраняемой территории.
– Убедитесь, что камера защищена от погодных воздействий, если устанавливается снаружи здания.
– Настройте Wi-Fi соединение или кабельную линию подключения.
– Установите приложение для просмотра записей и управления камерой через мобильное устройство.
—
Где лучше всего приобрести камеру видеонаблюдения?
При покупке обращайте внимание на проверенные магазины и бренды. Рекомендуем выбирать оборудование известных производителей, предлагающих гарантии качества и поддержку клиентов. Обратите внимание на предложения крупных торговых площадок, таких как Ozon, Wildberries и специализированные магазины электроники.
—
Советы по установке камер видеонаблюдения:
– Изучите правила установки камер видеонаблюдения перед началом монтажа.
– Получите согласие жильцов многоквартирных домов на установку камер в подъездах и местах общего пользования.
– Позаботьтесь о защите личной жизни соседей, устанавливая камеры таким образом, чтобы избежать нарушения частной собственности.
—
Поделитесь своим опытом!
Расскажите нам о вашем опыте покупки и установки камер видеонаблюдения. Может быть, у вас есть советы или рекомендации для новичков? А может, вы столкнулись с проблемами при выборе или настройке оборудования? Оставляйте комментарии ниже, давайте делиться полезными советами вместе!
Автор:
Система видеонаблюдения
*Данная статья носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей.*