अहमदाबाद के जमालपुर के पास स्थित बसन्त-रजब चौक को कितनों ने देखा है? देखा भी होगा और वहां से रोज गुजरते भी होंगे, तब भी ऐसे लोग उंगली पर गिनने लायक ही मिलेंगे जिन्होंने चौराहे के इस नामकरण का इतिहास जानने की कोशिश की होगी। मुमकिन है कि यहां से गुजरने वालों में अधिकतर ने आज के इस इकहरे वक्त़ में- जबकि मनुष्य होने के बजाय उसकी खास सामुदायिक पहचान अहम बनायी जा रही है- इस ‘विचित्र’ नामकरण को लेकर नाक भौं भी सिकोड़ी होगी।
वह जून 1946 का वक्त़ था जब आज़ादी करीब थी, मगर साम्प्रदायिक ताकतों की सक्रियता में भी अचानक तेजी आ गयी थी। उन्हीं दिनों दो युवा साम्प्रदायिक ताकतों से जूझते हुए मारे गये थे- वसंत राव हेगिश्ते और रजब अली लाखानी। वसंत का जन्म अहमदाबाद के एक मराठी परिवार में 1906 में हुआ था और एक खोजा मुस्लिम परिवार से आने वाले रजब अली लाखानी 27 जुलाई 1919 को कराची में पैदा हुए थे। बाद में उनका परिवार अहमदाबाद आकर बस गया था।
हमेशा की तरह उस साल रथयात्रा निकली थी और उसी बहाने समूचे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो चला था। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता रहे इन जिगरी दोस्तों ने अपने ऊपर यह जिम्मा लिया कि वे अपने-अपने समुदायों को समझाएंगे कि वे उन्मादी न बनें।

इसी काम में वे जी जान से जुटे थे। छोटी-छोटी बैठकें कर रहे थे। लोगों को समझा रहे थे। आज ही के दिन यानि 1 जुलाई को खांड नी शेरी के पास जूनूनी हो चुकी उग्र भीड़ ने इन दोनों को अपने रास्ते से हटने को कहा। उनके इनकार करने पर दोनों को वहीं ढेर कर दिया गया।
गुजराती के चर्चित कवि जवेरचंद मेघाणी ने 1947 में वसंत-रजब की याद में एक संस्मरणात्मक खंड का प्रकाशन किया था, जिसमें कई लोगों ने इन दोनों के बारे में लिखा था। वसंत की छोटी बहन हेमलता ने लिखा था कि उनकी दोस्ती इतनी अटूट थी कि “उन्हें मौत ही जुदा कर सकी, जब कांग्रेस कार्यालय से उनकी अर्थी साथ उठी।“

विगत कुछ वर्षों से उनकी शहादत के दिन छोटे-मोटे संगठन ‘सांप्रदायिक सद्भाव दिवस’ मनाते आ रहे हैं। गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में रायखण्ड के पास स्थित गायकवाड हवेली कैम्पस के पुलिस म्यूजियम में उनकी मूल तस्वीरों के साथ उनसे जुड़ी कुछ अन्य चीजों को प्रदर्शित किया है और इसे ‘बंधुत्व स्मारक’ घोषित किया है।
उनकी इस साझी शहादत को इस साल 74 साल पूरे हो रहे हैं।
विडम्बना ही है कि स्वाधीनता संग्राम के दो महान क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खान की दोस्ती एवं शहादत को याद दिलाती इस युवा जोड़ी की स्मृतियों को लेकर कोई खास सरगर्मी शेष मुल्क में नहीं दिख रही है। इसकी वजहें साफ हैं।
दरअसल, इनके बलिदान को याद करने का यह सफ़र हमें अपने इतिहास के ऐसे पन्नों को पलटने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो आज की तारीख में धुंधले हो चले हैं। मिसाल के तौर पर, स्वतंत्रता सेनानी और प्रबुद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी को आज की तारीख में कितने लोग जानते हैं? आजीवन जिस धार्मिक कट्टरता और उन्माद के खिलाफ वह आवाज उठाते रहे. वही धार्मिक उन्माद उनकी जिंदगी लील गया।

23 मार्च, 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिये जाने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गयी थी। कानपुर भी इससे बचा हुआ नहीं था। इस घटना के ठीक तीसरे ही दिन यानी 25 मार्च को शहर में हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच मनमुटाव ने एक बड़े दंगे का रूप ले लिया। दोनों समुदायों के लोग एक-दूसरे की जान लेने पर आमादा थे। ऐसे माहौल में भी गणेश शंकर विद्यार्थी लोगों के उन्माद को शांत करने के लिए घर से निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने कई लोगों की जान बचायी, लेकिन आखिर में उन्हें इन्हीं उन्मादी लोगों के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी (25 मार्च 1931)।
यह वही विद्यार्थी थे जिन्होंने हमेशा राजनीति और धर्म के मेल की मुखालिफत की थी। खिलाफत आंदोलन की लामबन्दी को लेकर उन्होंने लिखा था कि “देश की आजादी के लिए वह दिन बहुत ही बुरा था जिस दिन आजादी के आंदोलन में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया.”
‘धर्म की आड़’ नामक अन्य लेख में उन्होंने स्पष्ट किया था कि किस तरह ‘देश में धर्म की धूम है। उत्पात किये जाते हैं, तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है, तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जानें या न जानें, परंतु उसके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं।’
हम पंडित सुंदरलाल को याद कर सकते हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गदर पार्टी की मिलिटेंट कार्रवाइयों से की थी और बाद में गांधीजी के सच्चे अनुयायी बने थे। चालीस से अधिक किताबों के लेखक पंडित सुंदरलाल की चार खंडों में प्रकाशित ‘भारत में अंग्रेजी राज’ शीर्षक किताब प्रकाशित होते ही (1929) ब्रिटिशों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गयी थी। वर्ष 1941 में उन्होंने गीता और कुरान को एक साथ हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित किया था। इनके साथ जुड़ा एक संस्मरण बार-बार दोहराने लायक है, जहां बम्बई में तनाव के दिनों में- जबकि मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता कांग्रेस की जनसभा में कुछ हंगामा करने पर आमादा थे और उनकी अपनी जान को खतरा था- इन्होंने भरी जनसभा में अपने भाषण से माहौल को अपने पक्ष में कर लिया था।
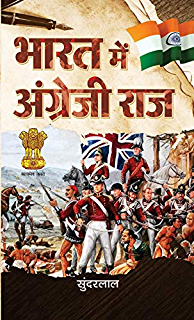
हम महात्मा गांधी को याद कर सकते हैं जिन्होंने हिन्दू कट्टरपंथियों के खिलाफ ही नहीं, मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ भी अपनी मुहिम को उन दिनों में भी जारी रखा जब बंटवारे के बाद मुल्क में हवाएं उल्टी बहने लगी थीं और अपने उसूलों पर अडिग रहने की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकायी थी।
सवाल है कि इन्सानी एकता को मजबूत रखने के लिए, वक्त़ पड़ने पर अपने आप को जोखिम में डालने के लिए क्या सिर्फ चर्चित अग्रणी ही तैयार रहते हैं? दरअसल, इसकी बुनियाद आम लोगों की ऐसी सक्रियताओं पर टिकी होती है। ऐसी कई मिसालें हमें देखने को मिलती हैं।
कुछ अरसा पहले एक संस्था ने बसन्त-रजब की शहादत के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा था जिसमें चन्द मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव साझा किये थे। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने दिल्ली की अपनी उस मौसी का किस्सा सुनाया, जिन्होंने 1984 के सिख विरोधी संहार के दिनों में- जबकि अकेले दिल्ली में ही आधिकारिक तौर पर एक हजार के करीब सिख मार दिये गये थे- अपने पड़ोसी सिख परिवार को अपने घर में शरण दी थी, जबकि उन दिनों ऐसे लोगों को ढूंढ रही हत्यारी भीड़ कभी भी उनके घर को तथा उनके तीनों बच्चों को निशाना बना सकती थी।
एक लेखक/कार्यकर्ता ने 2002 के गुजरात के झंझावाती दिनों का वह किस्सा सुनाया, जब तत्कालीन राज्य सरकार की शह पर सूबे में अल्पसंख्यकों के खिलाफ खूनी अभियान चला था, जिसे हिन्दुत्व के वर्चस्ववादी संगठनों के कारिन्दों ने अंजाम दिया था। उनके मुताबिक अहमदाबाद के पास के एक गांव (कुहल) के एक साधारण किसान ने अपने ही गांव के कई मुस्लिम परिवारों को, उनके बाल बच्चों के साथ, दस दिन तक अपने यहां शरण दी थी। इसके लिए उन्होंने न केवल अपने आप को बल्कि अपने सारे करीबियों को जोखिम में डाल दिया था। यह संख्या 110 थी।
वसन्त-रजब की साझी शहादत को याद करने की यह चर्चा उस प्रसंग के बिना अधूरी रह जाएगी, जो रजब अली के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है।

वर्ष 2015 की 1 जुलाई को बंधुत्व स्मारक का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया। इस कार्यक्रम में सिर्फ वसंत राव हेगिश्ते के परिवार के सदस्य शामिल हो सके। और लाखानी परिवार? इनके परिवार का एक भी सदस्य वहां उपस्थित नहीं था। वे सभी अमेरिका और कनाडा बस गये थे।
विडम्बना ही कहेंगे कि आज़ादी के बाद अहमदाबाद में हुए दंगों में लाखानी परिवार के सदस्य बार-बार हमलों का शिकार होते रहे। शायद सांप्रदायिक शक्तियां- जो रजब अली की सक्रियताओं से उद्वेलित थीं- उनके वारिसों से बदला चुकाना चाह रही थीं। आलम यहां तक आ पहुंचा कि उनके परिवार वालों ने हिन्दू धर्म अपना लिया और इस कदर गुमनामी में चले गये कि रजब अली लाखानी के साथ अपना कोई रिश्ता बताने से भी डरते रहे।
क्या ऐसे ही मुल्क की तस्वीर के लिए इन वीरों ने अपनी जान कुरबान की थी?





