याद कीजिए, इमैनुएल मैक्रां के फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने पर यहां की तथाकथित लिबरल-सेकुलर, वाम ताकतों ने किस तरह हर्ष-विगलित स्वर में मानवता के बच जाने की बात कही थी और भारत के लिए भी एक मैक्रां जैसे नेता की दुआ की थी। आज महज तीन साल के भीतर तस्वीर उल्टी हो गयी है। सिर्फ इसलिए, कि फ्रांस में एक इस्लामिक जिहादी के हाथों एक स्कूल टीचर की हत्या के बाद मैक्रां ने अपनी अनुभूत सच्चाई बयान कर दी। उन्होंने इस घटना को बेलाग-लपेट ‘इस्लामी आतंकवाद’ कहा।
अब ज़रा इस कथित सेकुलर-लिबरल लॉबी का खेल देखिए। मुद्दा क्या होना चाहिए था और क्या है? मुद्दा था कि इस्लाम के नाम पर फ्रांस में एक और हत्या हुई। यह तमाम हत्याओं की फेहरिस्त में एक और हत्या मात्र है और कम से कम अब इस्लाम के ऊपर बात होनी चाहिए। यह लेकिन मुद्दा नहीं बना। मसला इस बात को बनाया गया कि मैक्रां ने इस्लाम के ऊपर टिप्पणी की है (जो उन्होंने बिल्कुल की है) और वह एक हत्यारे के बहाने ‘इस्लामोफोबिया’ को बढ़ावा दे रहे हैं। बात हत्यारे पर, उसकी प्रेरणा पर होनी थी। मुद्दा बन गया उस पर बात करने वाला। आइए, ज़रा बिंदुवार इस पूरे घटनाक्रम को समझें।

फ्रांस की घटना के बाद पूरी दुनिया में मुस्लिमों ने समवेत् स्वर में फिर से अपना ‘राग विक्टिम’ शुरू कर दिया है। इस राग का आरोह हालांकि कोमल नहीं है, मद्धम भी नहीं। पर्याप्त आक्रामक है। इमैनुएमल मैक्रां को ईरान ने ‘डेमन ऑफ पेरिस’ कहा, तो पाकिस्तान अपने नये पाये खुदा तुर्की के साथ फ्रांस के खिलाफ जेहाद की बोली ही बोलने लगा। मजे की बात यह है कि आधिकारिक तौर पर भारत ने फ्रांस के साथ खड़ा रहने की बात की है, लेकिन यहां के शांतिप्रिय मुस्लिम इस कोरोना काल में भी सड़कों पर आ गए हैं और मैक्रां के पोस्टर लगाकर उसकी मज़म्मत कर रहे हैं।
इस पूरे काल में किसी भी मुस्लिम नेता, मौलवी, लिबरल पोस्टर ब्वॉय, चिंतक, बुद्धिजीवी, सेकुलर सरदार ने इस बात की कोई चर्चा नहीं की है कि पेरिस में टीचर की हत्या के बाद नीस में चर्च पर भी एक हमला हुआ है और दोनों हमले रिफ्यूजी मुस्लिमों ने ही किये हैं।
आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस बात पर एक मिनट अटकें। इस्लाम के नाम पर जब भी कोई हत्या की जाती है, तो दो तर्क होते हैं: या तो यह कहा जाता है कि यह ‘सही वाला इस्लाम’ नहीं है या फिर इसे किसी सिरफिरे के ‘वन ऑफ’ कृत्य की तरह ले लिया जाता है। ये सवाल बहुत दिनों से अनुत्तरित पड़ा हुआ है कि इस दुनिया में ‘असली इस्लाम’ का पता कब और कैसे चलेगा। दूसरे धर्मों के ‘अच्छे’ या ‘बुरे’ संस्करणों पर भी बात हो सकती है, लेकिन यहां उनका संदर्भ नहीं है। क्यों नहीं मौलानाओं ने, बुद्धिजीवियों ने, इकट्ठा होकर ऐसा एक ‘सही इस्लाम’ बताया जिसको पूरी दुनिया समझ सके? क्यों नहीं कुरान की उन आयतों पर चर्चा हुई (मैं सिर्फ चर्चा की बात कर रहा हूं) जिसमें काफिरों को वाजिबुल-कत्ल बताया गया है और उनकी जगह ‘सच्ची और सही इस्लामिक आयतें’ क्यों नहीं बतायी गयीं?
यह समस्या पूरी दुनिया की है। भारत और फ्रांस भी इस मामले में एक हैं। दोनों ही जगहों पर धर्मनिरपेक्षता के मायने भी एक हैं (पश्चिमी आधुनिकता द्वारा परिभाषित), भले दोनों के आधुनिक राष्ट्र-राज्य बनने की तारीख में पांच दशक की दूरी हो। फ्रांस के अख़बार चार्ली हेब्डो ने 30 मार्च 2016 के अंक में अपने संपादकीय का शीर्षक एक सवाल को बनाया था, ‘’हाउ डिड वी एंड अप हियर’’? यानी हम यहां तक कैसे पहुंच गए। ज़ाहिर है, ‘यहां’ से आशय फ्रांस के सेकुलर समाज के धार्मिक कट्टरता की स्थिति तक पहुंच जाने से है। इस संपादकीय में अखबार ने इसके कारणों की पड़ताल करते हुए लिबरल समाजों को कठघरे में खड़ा किया था।
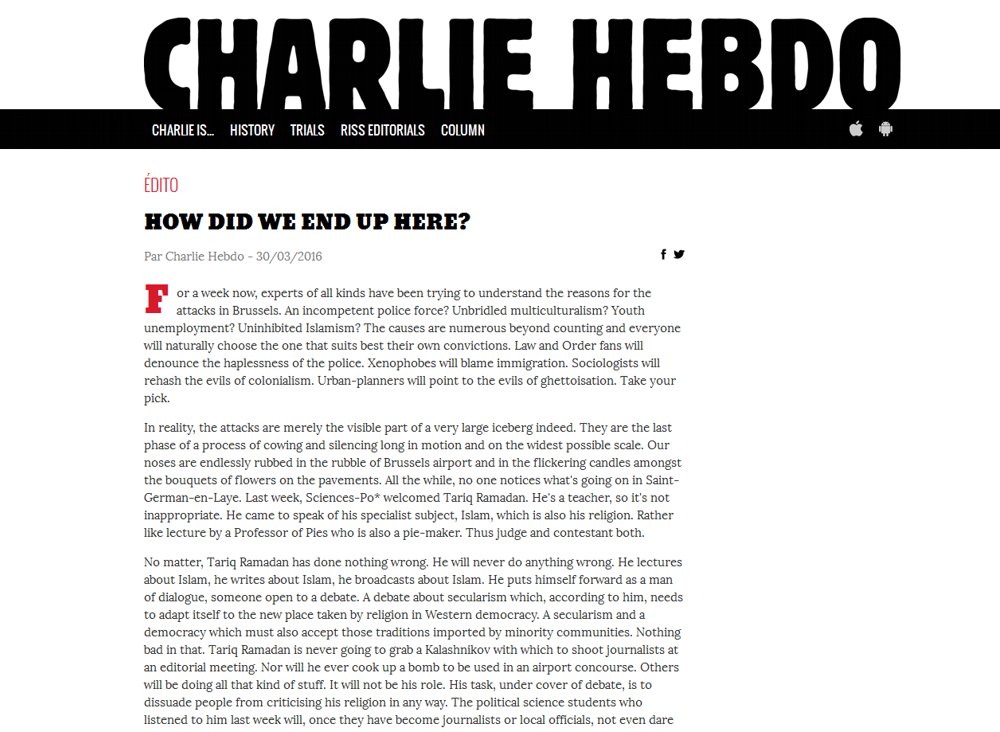
युनिवर्सिटी ऑफ हूस्टन में इतिहास के प्रोफेसर रॉबर्ट ज़ारेत्सकी इस संपादकीय का हवाला देते हुए एक लेख में पूछते हैं कि क्या फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति पर हुए हमलों के प्रति फ्रांस की ‘उदासीनता’ ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या एक स्थानीय मुसलमान बेकर- जो वैसे तो बहुत शांत, सज्जन, सदव्यवहार वाला शख्स है लेकिन बस एक दिक्कत है कि वह हैम और बेकन के सैंडविच नहीं बेचता- की समाज में सहज स्वीकार्यता इस्लामिज़्म के साथ गलबहियां करना नहीं हुआ?
यह टिप्पणी तारिक रमदान के एक लेक्चर के जिक्र से शुरू होती है और बताती है कि सेकुलरिज्म के मूल्य के तहत समाज अपनी पसंद का सामान न बेचने वाले बेकर को जैसे ही स्वीकार्यता देता है, वहीं बेकर की भूमिका पूरी हो जाती है। इस तरह कई अप्रिय चीजों को पचाते हुए समाज एक अनजाने भय में घिर जाता है- मुंह खोलने का भय। तारिक रमदान जैसे इस्लामिक स्कॉलरों की यही भूमिका है- वे आपके सेकुलरिज्म में हलका से ‘डेन्ट’ मार देते हैं और आप इस भय से मुंह बंद कर लेते हैं कि आपके कहे को इस्लामोफोबिया न समझ लिया जाए।
इससे जो समूचा दर्शन बनता है, किसी बम का धमाका या किसी की गला रेत कर की गयी हत्या उसकी तार्किक परिणति होती है। ऐसे कृत्य ‘वन ऑफ’ नहीं होते। एक सिलसिला होता है जिसमें इस्लामिज्म के खिलाफ सेकुलरिज्म अपना मुंह बंद रखता है। इस्लाम पर मुंह खोलने, चर्चा करने का मतलब ये नहीं कि हम मुसलमानों को विक्टिम बना रहे हैं। हकीकत तो यह है कि इस्लाम का कोई विपक्ष है ही नहीं- न हिंदू धर्म, न ईसाइयत, न यहूदी धर्म। इस्लाम का इकलौता विपक्ष वही है जो बाकी सब धर्मों का विपक्ष है यानी सेकुलरिज्म। विडम्बना देखिए कि सेकुलरिज्म ने इस्लाम पर बोलने के किसी अदृश्य भय से मुंह बंद कर लिया था। ठीक उस वक्त चार कदम पीछे हट गया था जब उसे विपक्ष की भूमिका निभानी थी। ऐसा कर के सेकुलरिज्म के वाहकों ने दरअसल उसकी मूल अवधारणा को ही डाइल्यूट कर दिया।
भारत में इस भय और इससे उपजे गिल्ट का खेल ही गज़ब है। सीधा सिर के बल खड़ा कर दिया गया है यहां तथ्यों को। आप एक बार ‘शिंडलर्स लिस्ट’ देख लीजिए। दो-दो महायुद्धों और होलोकॉस्ट जैसी त्रासदियों के बाद यूरोप अगर विकसित हो सका तो इसलिए कि उसने अपने इतिहास को रद्दी कालीन के नीचे नहीं बुहारा। उसने अपने घाव को गंदी पट्टियों से नहीं छिपाया, जिससे घाव की चिकित्सा हो सकी। यहां आप बाकी बातें रहने दीजिए, 1947 में जो भयावह नरसंहार हुआ उसी पर कितना साहित्य, फिल्म या नाटक, गीत पाते हैं हम? उल्टा एक वायवीय बात हमें फीड की गयी है कि जो मुसलमान यहां रहे, उन्होंने चुना इस देश को। भुला दिया जाता है कि चुनाव में तो 95 फीसदी मुस्लिम आबादी ‘मुस्लिम लीग’ के साथ थी, डायरेक्ट एक्शन डे के साथ थी, मोपला के साथ थी, तुर्की खलीफा के साथ थी। आप जब तक इतिहास का बोध नहीं कराएंगे, तो कोई भी समाज भला कैसे स्वस्थ होगा? फ्रांस में अगर इस पर चर्चा चल रही है, तो सिर्फ इसलिए कि वहां दबाने या छुपाने की परंपरा नहीं रही है। लोग एक हद के बाद बहस करना भूले नहीं हैं।
इसका मतलब यह नहीं कि फ्रांस या मैक्रां ‘इस्लामोफोबिया’ को बढ़ावा दे रहे हैं। इस्लामोफोबिया का क्या मतलब है, भाई? फोबिया का मतलब है- वह भय, जिसकी कोई तुक न हो, जो यथार्थ न हो। इस्लाम से भय के कारण तो प्रत्यक्ष हैं। इस्लाम पर चर्चा न करने का क्या कारण है? वह कौन सा भय है जिसके चलते लिबरल-सेकुलर लोग बिरयानी खा लेने या बना लेने, चंद गज़लें रट लेने या उर्दू-फारसी के चंद अशआर जान लेने, ईद पर मुबारक-मुबारक कह देने या विदा होते वक्त खुदा-हाफिज (आजकल अल्लाह हाफिज) कह देने भर से समझते हैं कि वे इस्लाम को जान गए, इसलिए और चीजों पर मुंह बंद रखते हैं?
यह इतना आसान नहीं है। एक जबर्दस्त सामाजिक एके वाले मजहब, जिसकी किताब में संशोधन तो दूर, उसकी बात तक करने पर जान पर बन आती है, ऐतिहासिक तथ्यों तक को मात्र कह देने से लोग कत्ल हो जाते हैं, उसको आप मीठी खीर और कुर्बानी का मांस खाकर नहीं जान सकते, जनाब। इस्लाम को जानने के लिए उसकी सुन्नतों, आयतों, पांच कर्तव्यों, सामाजिक संरचना और सबसे बढ़कर मजहबी दखल या एकाधिकार को जानना होगा। उस डर पर बात करनी होगी जो एक आम मुसलमान से लेकर एक अभिजात्य बुद्धिजीवी को एक ही जुबान बोलने पर मजबूर कर देता है।
आपको यह समझना होगा कि मुसलमानों को क्यों पिछड़ेपन की किसी भी निशानी, किसी भी परंपरा पर बात करना तक नहीं पसंद। सुधार की तो बात छोड़ दीजिए, सवाल यह है कि जब भारत में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि लगभग टेक्स्टबुक का हिस्सा बन चुके हैं ऐसे में हलाला, तीन तलाक, लड़कियों का खतना, कम उम्र में शादी, आदि-इत्यादि कुप्रथाओं को परदा-दर-परदा ढंक कर क्यों रखा जाता है? क्यों श्रीमान अमिताभ बच्चन राजस्थान की पुरातन ड्रेस में आयी एक महिला की तो मजम्मत कर सकते हैं, पर बुर्कानशीं किसी मोहतरमा की नहीं?
ये प्रश्न दाहक हैं, समाज को इनसे दो-चार होना ही होगा, जैसे आज फ्रांस हो रहा है। आप इन सवालों को संघी, ट्रोल, इस्लामोफोबिक कहकर जितना अधिक कालीन के नीचे बुहारते रहेंगे, आग उतनी ही अधिक भड़कती रहेगी। एक अंतिम बात ये है कि भारत के मुसलमानों का अगर किसी ने सबसे अधिक नुकसान किया है, तो यहां की तथाकथित लिबरल-सेकुलर, वाम लॉबी ने किया है।





