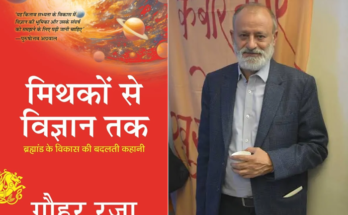लगता है ‘पठान’ अब एक फिल्म से ज़्यादा हिन्दी सिनेमा के लिए ‘बाउंस बैक’ मोमेंट बनने जा रहा है। सिनेमाघरों में, टिकट की बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद जिस तरह लोग उमड़ रहे हैं वो कोविड के बाद पहली दफा देखा जा रहा है। फिल्म के ‘बायकॉट’ की धमकी भरी अपीलों ने जैसे दर्शकों में एक अलग तरह का रोमांच भी पैदा किया है। यह फिल्म कई वजहों से करिश्माई बतलायी जा रही है।
यह फ़िल्म क्यों खास है?
इसके लिए फ़िल्म से पहले इसके खिलाफ बनाए गए माहौल से बात शुरू की जानी चाहिए। इस फ़िल्म का जितना तीव्र विरोध महज एक गाने के कुछ सेकेंड की क्लिप से हुआ वह ‘नए भारत’ में अब नयी परिघटना तो नहीं रह गयी है लेकिन इस विरोध के मानी स्पष्ट थे। ये विरोध ‘बेशर्म रंग’ में इस्तेमाल हुए भगवा रंग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ तो कतई न था।
विरोध का स्पष्ट लक्ष्य शाहरुख खान थे। दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण लक्ष्य दीपिका पादुकोण थीं। हम सब जानते हैं कि ये दोनों फ़िल्म जगत की ऐसी शख्सियतें हैं जो अपनी खामोश मौजूदगी से ‘नए बहुसंख्यक, हिन्दुत्व सम्पन्न भारत’ की परियोजना पर प्रहार करते रहे हैं। अपने खिलाफ हो रहे तमाम तरह के सरकारी और गैर-सरकारी उत्पीड़न के बावजूद खुद को ‘सरेंडर’ नहीं करते। दीपिका ने जहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के संघर्ष में अपनी खामोश मौजूदगी दर्ज़ कराकर इस नए भारत के लाभार्थियों को अपने खिलाफ कर लिया वहीं शाहरुख खान जिनके नाम का दूसरा हिस्सा ही हालांकि विरोध का पर्याप्त मजबूत कारण है लेकिन उससे भी बढ़कर अपने बेटे के खिलाफ चली पूरी षड़यंत्रकारी मुहिम का मजबूती से सामना किया और खुद को बहुसंख्यकों के भगवान के सामने नत-मस्तक नहीं किया।
शाहरुख और दीपिका उस पुराने भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां कलाकारों को उनके हुनर से पहचाने जाने की रवायत रही है न कि उनकी जाति, धर्म या विचारधारा से। ऐसे में महज कुछ सेकेंड की एक क्लिप से बिना पूरी फ़िल्म देखे जिस कदर व्यापक विरोध हुआ और ऐसे असंवैधानिक विरोध होने दिये गए उससे यह स्पष्ट होता है कि इस आलोकतांत्रिक विरोध के पीछे केवल कुछ संगठन ही नहीं थे बल्कि नए भारत की परियोजना में शामिल पूरा तंत्र शामिल था।
क्या फिल्म को मिल रहा समर्थन उसे मिले विरोध का विरोध है?
इस फ़िल्म को मिल रही सफलता को देखकर एकबारगी तो यही लगता है कि यह संगठित ढंग से एक खास विचारधारा के लोगों द्वारा किए गए विरोध का अहिंसक विरोध है। खबरें आ रही हैं कि कई सिनेमाघरों ने इस फिल्म के लिए अतिरिक्त शो शुरू किए हैं, अमूमन हर शो हाउसफुल जा रहा है, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर जो लंबे समय से अपने खुलने की बाट जोह रहे थे और इस फ़िल्म के साथ उनमें बहारें लौटी हैं और सिनेमाघरों के अंदर दर्शकों के झूमने, सीटी बजाने की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे तमाम दृश्य सोशल मीडिया पर मंज़र-ए- आम हो रहे हैं।
ऐसा भी लगता है कि देश के आम दर्शक इस तरह के बेजा विरोध और एक खास विचारधारा के लोगों की संविधानेतर बायकॉट की धमकियों से आजिज़ आ चुके हैं। ये धमकियाँ ज़रूर एक खास मकसद से दी जाती हैं लेकिन इन धमकियों के आगे निरंतर झुकने से जैसे आम सिनेप्रेमी ने इस बार तौबा कर ली है। आखिर यह एक आम दर्शक के विवेक पर हमला ही है जो उसकी तरफ से किसी और को ये हक़ देने जैसा है कि वो कोई फिल्म देखे या न देखे। हिन्दी सिनेमा, निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और एक फिल्म के निर्माण में शामिल उन तमाम लोगों के अलावा अंतत: आम दर्शक की होती है जो उस फिल्म की नियति तय करता है। इसलिए किसी फिल्म का विरोध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस दर्शक के विवेक का ही विरोध होता है। दर्शक के इस नितांत मौलिक अधिकार की रक्षा करना तमाम संवैधानिक संस्थाओं का कर्तव्य है लेकिन अफसोस कि धमकियों के सामने सबसे पहले यही संस्थाएं हथियार डालते नज़र आ रही हैं।
क्या देशभक्ति ही इस फिल्म की सफलता का राज़ है?
कहा जा रहा है कि यह फिल्म देशभक्ति से परिपूर्ण एक मसाला फिल्म है और इसलिए इस फिल्म का विरोध भी थम गया और इसे सामाजिक स्वीकृति भी मिल गयी। ऐसी फिल्में बनाने के मामले में अभिनेता अक्षय कुमार शाहरुख खान से कहीं आगे हैं जो देशभक्ति से थोड़ा आगे बढ़कर हिन्दुत्व के आख्यान से रची-बसी फिल्में भी एक सप्ताह सिनेमाघरों में टिका पाने में असफल हुए जा रहे हैं। हाल ही में आयी उनकी ‘रामसेतु’ फिल्म बुरी तरह पिट गयी। इसी तर्ज़ पर अजय देवगन की ‘कच्छ’ भी बुरी तरह पिटी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज के दौर में केवल देशभक्ति से ओत-प्रोत होने को ही किसी फिल्म की सफलता की गारंटी कहा जा सकता है? पठान फिल्म देखते हुए ऐसा लगेगा कि यह फिल्म अंतत: देशभक्ति ही स्थापित करती है लेकिन यह फिल्म इससे कहीं ज़्यादा आम इंसान को बचाने के मिशन में तब्दील होती दिखलाई पड़ती है। अगर मानवता को बचाने के लिए संघर्ष का नाम देशभक्ति है तो इससे अच्छी देशभक्ति की परिभाषा शायद कुछ और नहीं हो सकती।
यह फिल्म जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ भारत की अंतहीन दिखती दुश्मनी को स्थापित करती है और उसकी एजेंसी आइएसआइ को सालों से चले आ रहे छल-कपट के सुविधाजनक आवरण में लपेट कर पेश करती है तो उसी एजेंसी की एक एजेंट (दीपिका पादुकोण) में भी उसी इंसानियत को खोज लाती है जिसके लिए भारत की उसी के समकक्ष एजेंसी का एक एजेंट संघर्ष कर रहा है। यहाँ आकर दोनों देशों के एजेन्टों के बीच मानवता को बचाने के लिए संघर्ष की तड़प एक जैसी दिखलाई पड़ती है। इस लिहाज से यह फिल्म देशभक्ति के कुछ नए प्रतिमान रचती है।
‘पठान’ होना इस फिल्म में शाहरुख खान की जन्मजात नियति नहीं है और इसलिए यह कह देना एक मुसलमान होने के नाते असल में शाहरुख खान ने उस मुख्य धारा के आख्यान का पालन किया है जिसके तहत एक आदर्श मुसलमान वही हो सकता है जो अपने देश (हिंदुस्तान) के लिए मर मिटे। शाहरुख पठान की अपनी पहचान के मामले में दीपिका पादुकोण द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वो मुसलमान है? बताते हैं कि ‘उसे नहीं पता। उसके माँ-बाप उसे बचपन में एक सिनेमाहॉल में छोड़ गए थे, फिर वो अनाथालय में बड़ा हुआ, फिर किसी जुवेनाइल होम में रहा। उसे देश ने सब कुछ दिया। देश का कर्ज़ लौटाने के लिए वो सेना में भर्ती हुआ। एक दफा अफगानिस्तान के एक गाँव को मिसाइल के हमले से बचाया। वो गाँव पठानों का था। उसी गाँव ने पठान नाम दिया’।
शाहरुख खान का यह संवाद कई मायनों में उस लीक को तोड़ देता है जिसके तहत एक आदर्श हिन्दुस्तानी मुसलमान का चेहरा गढ़ने की कोशिश की जाती है। शाहरुख यहाँ ईमान से, जुबान से ‘पठान’ है लेकिन वह आत्मा से एक हिन्दुस्तानी है जिसे अपना पैदाइशी मजहब, जाति कुछ नहीं पता है और जिसका पालन-पोषण इस देश की लोकतान्त्रिक संस्थाओं ने किया है। इस लिहाज से फिल्म को देखें तो हमें भारतीयता की रूढ़ परिभाषा से इतर एक नये जनतान्त्रिक हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत की परिभाषा कहीं व्यापक और उदार रूप में हासिल होती है।
फिल्म में ताज़ा क्या है?
पठान फिल्म एक मनोरंजक फिल्म है। मनोरंजक होना किसी भी कला का पहला मकसद है। यह फिल्म हिन्दी सिनेमा में तकनीकी के इस्तेमाल के मामले में नया कदम साबित होगी हालांकि जिन्हें ‘मार्वेल’ सीरीज की हॉलीवुड फिल्में देखने का अभ्यास है उनके लिए यह हिन्दी सिनेमा में नयी आमद जैसा है। पूरे तौर पर नहीं लेकिन कुछ हद तक ऐसे दृश्य रचने की कोशिश हुई है जो हिन्दी सिनेमा के दर्शकों के लिए मनोरंजन के साथ साथ अलग ‘स्पेस’ का तसव्वुर दे सके।
हवा में करतब हो या लड़ाई, जमी हुई बर्फ पर मोटरसाइकिलों का तेज़ गति से भागना हो, अत्यंत उन्नत तकनीकी से लैस तालों को खोलना हो और ये सब दुनिया के तमाम देशों के इर्द-गिर्द रचा गया फलक हो, ये फिल्म हर मामले में ग्राह्य तो लगती है। ये फिल्म दर्शक को यह याद दिलाती रहती है कि वो सिनेमा देख रहा है। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
संगीत सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिहाज से मुफीद है। संवाद सुने जाने और याद रखे जाने लायक है। अभिनय के मामले में जॉन इब्राहिम किरदार के मुताबिक वो तल्खी अपने चेहरे पर नहीं ला नहीं सके। दीपिका पादुकोण का अभिनय अच्छा रहा। शाहरुख ने जैसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पूरी शिद्दत से अपने किरदार को जिया है। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा के कसे हुए अभिनय के बिना यह फिल्म ऐसी नहीं बनती जैसी बन पड़ी है।
कश्मीर बीच में आ गया क्या?
इस मामले में फिल्म कमजोर पटकथा से गुज़री है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान की कश्मकश समझ में आती है लेकिन उसका प्रतिकार किसी सुपारी किलर को कांट्रैक्ट देकर किया जाना नितांत अहमकाना लगा। दिलचस्प ढंग से कश्मीर के मामले का हल केवल पाकिस्तान का सेना प्रमुख ढूँढने निकल पड़ता है। बिना किसी राजनैतिक नेतृत्व और दिशानिर्देश के। यह इस फिल्म का सबसे कमजोर पहलू लगा और ऐसा भी लगा कि इसे जबरन फिल्म को सामयिक बनाने की कोशिश के चलते हुआ है। कोरोना का हवाला भी इस फिल्म में दिया गया बल्कि उससे भी खतरनाक वायरस बनाने की कोशिश को एक तरह नकारात्मक प्रेरणा के तौर पर दिखाया गया है। यह कल्पना अपने आप में काफी ध्वंसक है जिसे चाहे-अनचाहे इस फिल्म में शामिल किया गया है।
अंत में
फिल्म एक दफा ज़रूर देखे जाने लायक है। शाहरुख के लिए, दीपिका के लिए और इन दोनों के खिलाफ चले विरोध अभियान के खिलाफ भी। एक मज़ेदार, मनोरंजक सिनेमा का बढ़िया लुत्फ सिनेमा घर में जाकर ही उठाया जा सकता है।
(लेखक लंबे समय से सामाजिक मुद्दों पर लिख रहे हैं)