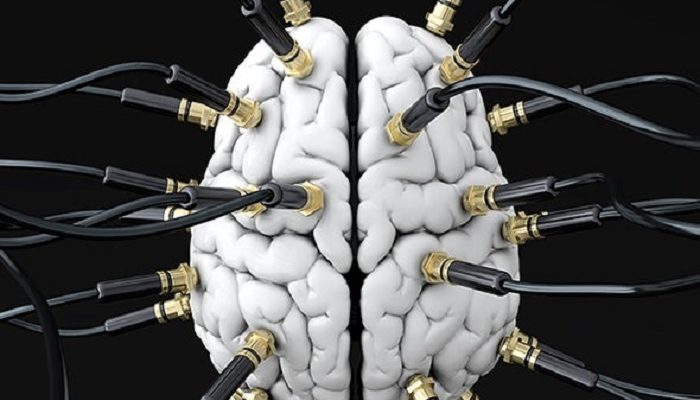अपने पसंदीदा स्तम्भ को एक अंतराल के बाद फिर से लिख रहा हूं। इस बीच मन को शांत करने का अभ्यास किया। लोगों को केवल और केवल सुना। उन्हें टोका नहीं। जिनसे भी इस बीच संवाद हुआ उन्होंने मेरे इस बदले हुए आचरण को लक्षित किया। पूछा भी, कि ठीक तो हो? पलटकर कहना चाहा कि यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, लेकिन टोकने से तौबा की थी इसलिए नहीं पूछा। हालांकि मेरे इस स्तंभ के न आने से कायनात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बीच में एकाध दफा शमशान और कब्रिस्तान याद आए जहां एक से एक दानिशमंद सोये हुए हैं। और जिनके सोये रहने से भी इस कायनात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे फ़र्क पड़ा। क्या इतना काफी नहीं?
बड़ी तेज़ी से हम एक समाज के तौर पर स्मृतिहीन समाज में तब्दील होते जा रहे हैं। सूचना जब एक उद्योग बन जाय और निरंतर बिना रुके, बिना थमे, सूचनाओं का उत्पादन चौबीस गुणा सात होने लगे और अन्य किसी उद्योग जैसा यह उद्योग भी भारी मुनाफा कमाने लगे तब सूचनाएं उत्पाद के तौर पर हमारे आसपास बहुतायत में यूं ही बिखरी पड़ी हैं जैसे बहुत सारा अनुपयोगी सामान, जो किसी ‘मेगा सेल’ से खरीद के लाया गया हो।
इन बहुत सूचनाओं ने हमारे दिल-दिमाग को इस कदर भर दिया है कि उसमें सब कुछ केवल समाया जा रहा है। किसी सूचना का कोई विशिष्ट महत्व नहीं बच रहा है। मौजूदा हिंदुस्तान एक घटना प्रधान हिंदुस्तान बन गया है। इसमें घटनाएं हैं और केवल घटनाएं हैं। जब घटनाएं हैं तो उनकी सूचनाएं हैं। सूचनाएं हैं तो उनकी मनमाफिक व्याख्याएं भी हैं। व्याख्याएं हैं तो उसमें मत-विमत हैं। मत-विमत हैं तो वाद-विवाद हैं और वाद-विवाद हैं तो जीतने-हारने की कोशिशें भी हैं। पक्ष-विपक्ष अब केवल सत्ता के प्रांगण की शब्दावली नहीं रही बल्कि अब वह कटुता का एक नया रूप लेकर उसी खम के साथ एकल परिवारों से लेकर संयुक्त परिवारों, पड़ोस से लेकर मोहल्ले और मोहल्ले से लेकर गाँव तक बसेरा करती जा रही है।
ऐसे में लोकतंत्र की सबसे सतही और सबसे भ्रामक व्याख्या ‘बहुमत’ इतिहास के सबसे गौरवशाली लेकिन विद्रूप समय में अपना स्वरूप चहुंओर पूरी ठसक के साथ फैला रहा है बल्कि हर इंच जगह को अपने दैत्याकार बाहुपाश में क़ैद करते जा रहा है। बिना किसी इतिहासबोध के बनता हुआ यह समाज खुद समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहा है।
जिस समाज को सिविल होना था और एक साथ एक उन्नत किस्म की सिविल सोसायटी यानी नागरिक समाज का निर्माण करना है या ऐसे कहें कि खुद को कुनबों, गोत्रों, जातियों, मज़हबों और क्षेत्रों से ऊपर उठाकर एक नागरिक के तौर पर प्रतिष्ठित करना था वो अब ऐसी बहसों में मुब्तिला हो चुका है जहां कुछ भी बोलकर कोई भी निकल जा रहा है। और समाज उसे एक घटना, सूचना, व्याख्या, पक्ष-विपक्ष, वाद-विवाद के एक मीठे घोल के मानिंद पीते जा रहा है। समाज में कोई जुंबिश अब जैसे किसी बात पर नहीं हो रही है क्योंकि उसके दिल-दिमाग में अब एक छोटी सी जुंबिश के लिए रिक्त स्थान नहीं बचा है।
जिस सिविल सोसायटी बनने की राह पर समाज को आगे बढ़ना था और गढ़ना था एक खूबसूरत लोकतंत्र- न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास और दूर-दूर बसे अपने हमवतनों के लिए- उस सिविल सोसायटी को एक रहस्यमयी इंसान बाहरी शक्तियों से भी ज़्यादा खतरनाक बता रहा है और उससे युद्ध किये जाने की ज़रूरत पर बल दे रहा है। वह पुलिस सेवा के लोगों को इनसे निपटने के लिए सतर्क कर रहा है। इस इंसान को ज़ाहिर है सिविल सोसायटी की कोई ज़रूरत नहीं है और यह उसके दिये बयान के बाद उसके लिए आश्वस्ति ही है कि कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई जुंबिश नहीं!
बात बोलेगी: एक ‘सिविल सोसायटी’ के राज में दूसरे का ‘वध’ और तीसरे का मौन
कोई आता है और आज़ादी को धता बताकर चला जाता है। जब वह आज़ादी को धता बता रहा है तब वह उसी आज़ादी का इस्तेमाल भी कर रहा है, हालांकि कालक्रम के हिसाब से जब वह इन अपचनीय गरिष्ठ पदार्थों का वमन कर रहा है तब वह सन 2021 है और उसे इस तरह बदबूदार वमन करने की आज़ादी हासिल हुए महज़ सात साल ही हुए हैं इसलिए वह अपने कहने में सही है कि देश को असली आज़ादी 2014 के बाद ही मिली है।
वह यह भी कहने की कोशिश कर रहा है कि 2014 से पहले अगर आज़ादी का इस्तेमाल किया जाता तो उसके साथ न्यूनतम ज़िम्मेदारी का एक बोध साथ रखना होता, न्यूनतम मर्यादा का पालन करना होता क्योंकि उसके अनुसार यह आज़ादी भीख में मिली थी इसलिए भीख की लाज रखने के वास्ते ही सही आंशिक रूप से कृतज्ञ होने की ज़रूरत हर शख्स को होती। 2014 के बाद अगर किसी मूल्य या बोध का सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है तो वह है कृतज्ञता। इस क्षरण को अगर वो शख्स आज़ादी ही समझता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बहुत लोग कृतज्ञता के साथ जीवन नहीं जी पाते। उन्हें थोड़ी सी सफलता के बाद यही सबसे बड़ा बोझ लगने लगता है जिसे वो जल्दी से जल्दी अपने सर माथे से उतार देना चाहते हैं। 2014 के बाद के नरेंद्र मोदी के भाषण इस बात की तसदीक करते हैं। इस इंसान ने अब तक के बने हिंदुस्तान के प्रति एक लफ्ज़ गलती से भी अगर इस्तेमाल नहीं किया है तो वो है कृतज्ञता। आभार। धन्यवाद। शुक्रिया। क्या अपने पूर्वजों या अपने से पहले आए लोगों के किए कामों के प्रति कृतज्ञ होना वाकई इतना बुरा है?
बहरहाल, बात एक स्मृतिहीन समाज से शुरू हुई थी तो क्या कृतज्ञता से मुक्ति का यह अभियान इसी स्मृतिहीन होते समाज की बुनियाद पर चलाया जा रहा है? एक समाज जो एक निजी चैनल के भव्य मंच के समक्ष बैठकर इस वमन को आचार समझकर चटखारे लेकर खाने ही लगे तब इस समाज में इसके खिलाफ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। बोलने से बचना एक बात है, बोलने का साहस करना या न करना एक अलग तरह का निर्णय और चुनाव है लेकिन इस इतिहासबोध के खिलाफ चटखारे लेकर तालियां पीटना एक ऐसा सोचा-समझा अभियान है जो बहुत जल्द अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आतुर है और बहुत जल्द वाकई यह अभियान समग्रता में सफल होगा। इस देश में यह अभियान नया नहीं है बल्कि इसके गठन के साथ ही शुरू हो चुका था। मंच पर बैठे शख्स और उसके सामने बैठे संभ्रांत लोगों ने इस अभियान का सार्वजनिक मुजाहिरा बस किया है।
एक इंसान आता है और वह बताकर चला जाता है कि अब से पहले की सरकारों ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। उसकी सरकार ने मुफ्त राशन दिया। वह शख्स आदिवासियों के लिए किये गए उन कामों से डरता है जो पिछली सरकारों ने किये थे। कृतज्ञता से मुक्त यह इंसान अपने साथ-साथ पूरे देश को इस जंजाल से मुक्ति दिलाने के अभियान में सरपट दौड़ा जा रहा है। इसे इल्म है कि वह सूचना दे रहा है। उसे ये भी इल्म है कि वह झूठी सूचना दे रहा है, लेकिन उसे यह भी इल्म है कि सूचना एक उपभोग की वस्तु है। सूचना, जिसके ग्राहक बिना सोचे-समझे इसका उपभोग करने के लिए तैयार किए जा चुके हैं। सूचना, जिसके सारे के सारे मंच उसके अधीन हैं। सूचना जिसके जरिये वह दिन को रात कहने की चालाक सलाहियत अर्जित कर चुका है। उसे यह भरोसा है कि उसकी सांसें इन्हीं सूचनाओं में बसती हैं और इस पर उसका पूरा का पूरा नियंत्रण है।
एक इंसान आता है जो अपने और प्रधानमंत्री के बीच हुई बात को सुहागरात पर हुई पति-पत्नी के बीच बात बताकर तालियां बटोर कर चला जाता है। इस बात पर भी कोई जुंबिश नहीं होती जबकि लोग इस देश में प्रधानमंत्री की घनघोर रूप से भयंकर इज्ज़त करते हैं। प्रधानमंत्री से उस शख्स के बीच के रिश्ते के बारे में पूछने के वजाय लोगों और उस शख्स के बीच पूछने को मन करता है। हम देख रहे हैं कि कैसे राष्ट्रवाद का रूपान्तरण झुनझुनवालावाद में हो रहा है। ये सब कमाल इन सूचनाओं की बहुतायत की वजह से हो रहा है या भंडारघर में ठूंस-ठूंस कर भरी गयी सूचनाओं की वजह से या इंसान की सबसे बड़ी नेमत स्मृति से विहीन होने की वजह से हो रहा है या इन सभी वजहों से हो रहा है कहना मुश्किल है, लेकिन अगर भारतवासियों के पास स्मृति बची रह जाएगी और सूचनाएं, सूचनाओं की शक्ल धारण कर लेंगी, तब ज़रूर इन कारणों की युक्तियुक्त पड़ताल होगी।

धरती के बढ़ते हुए तापमान से केवल पर्यावरण पर ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है बल्कि वह इंसान की सबसे बुनियादी प्रकृति यानी याद रखे जाने की क्षमता को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इन दो बातों के बीच सीधा-सीधा कोई रिश्ता वैज्ञानिकों ने नहीं बताया है लेकिन अब विज्ञान जानने के लिए क्या वाकई किसी वैज्ञानिक की तरफ देखने की ज़रूरत रह गयी है? जैसे इतिहास जानने के लिए इतिहासविद की तरफ या अर्थशास्त्र जानने के लिए किसी अर्थशास्त्री की तरफ या राजनीति समझने के लिए किसी राजनैतिज्ञ की तरफ? हालांकि यह बाद वाली प्रजाति लगभग विलुप्त होने की कगार पर है लेकिन बाकी लोग तो पेशेवर हैं। बचे हुए हैं। देश में नहीं तो कहीं और भी।
महज़ सात साल में ऐसे कितने इंसान आकर कुछ भी बता जा रहे हैं। जिसको जो मन आ रहा है वह बोलकर चला जा रहा है और सबसे पहले उसके ठीक सामने बैठे इंसान तालियों से उसके कहे को मान्यता दे रहे हैं, इसके बाद जब वह अवसर सूचना में बदलकर समाज और देश के बाकी लोगों तक पहुँच रहा है वो उसे अपने दिल दिमाग के किसी कोने में एडजस्ट करके उसके लिए भी जगह बना ले रहे हैं। और इस तरह एक बेसिर पैर की सूचना, ज्ञान का रूप लेकर दिल-दिमाग के भंडारघर में ठूंस दी जा रही है। वक़्त मौके पर भंडारघर से ऐसे ही सूचनाएं निकालकर घर-परिवार के परिसर में पक्ष-विपक्ष की पैंतरेबाजी अमर्यादित और कृतघ्नता के आवरण में अठखेलियाँ कर रही हैं।
दिलचस्प मामला यह है कि जो लोगों पर सीधे तौर पर बीती लोग उसे अब पूरी तरह भूल चुके हैं। जो कभी नहीं बीता उसे गठान बांधे बैठे हैं। कोरोना ने कितने घरों को बे-चिराग किया है इस दिवाली पर लेकिन लोगों को आज भी चिंता 2030 या 2050 में मुसलमानों की काल्पनिक रूप से बढ़ जाने वाली आबादी की है। ऐसे लोग जो बेचिरागों को रहनुमा बना चुके थे सात साल पहले, अब उसी राह पर हैं। उन्हें वो दर्द-ओ-गम भूल गया है जो कुछ महीनों पहले उन्होंने झेला था बल्कि उन्हें अब भी यही लगता है ठीक है, कुछ न होगा तो कम से कम मुसलमान ही टाइट कर दिए जाएंगे।
बात बोलेगी: स्मृतियाँ जब हिसाब मांगेंगीं…
यह समझना मुश्किल नहीं है कि बेतहाशा सूचनाओं ने समाज को इस कदर आत्मघाती बना दिया है या आत्मघाती समाज ने ऐसी सूचनाओं का उत्पादन किया है। जो हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को लीलने को आतुर हैं। और इसी कोशिश में दोनों ज़िंदा हैं। यही मूर्छित अवस्था का जिंदापन आज के लोकतंत्र का वाहक है और सूचनाओं की गाहक है।
लोग परेशान हैं। हैरान हैं। दुखी हैं। हताश हैं। फिर भी उनके पास कुछ ऐसा है जिसे देख-सुन कर वो अपने रंज-ओ-गम से बेखबर हुए जा रहे हैं। इस ऐसे कुछ की सप्लाई सातों दिन और चौबीसों घंटे जारी है। जैसे इस देश के समाज को खत्म कर लेने की ललक जारी है। जैसे सरकारों के प्रचार जारी हैं। जैसे हमारी स्मृतियों का क्षरण होना जारी है। जैसे सब कुछ जारी है।