तकनीक अद्भुत चीज़ है। 1990-91 में हमारे घरों में ‘लाइव’ युद्ध उतर आया था। केबल टी.वी. के जरिये। इराक में ‘ऑपरेशन डेज़र्ट स्टॉर्म’ चल रहा था और सीएनएन-बीबीसी के जरिये हमारे-आपके ड्रॉइंग रूम में युद्ध उतर आया था। कॉफी और चाय के साथ लड़ाई की खौफनाक तस्वीरों को हम हंसी और मज़ाक के जरिये भीतर उतार रहे थे। इसी दौर के बाद इस देश में धीरे-धीरे 24 घंटे के न्यूज़ चैनल नाम की मूर्खता का दिव्य विस्फोट हुआ था, जो आज डिजिटल प्रहसन में बदल चुका है।
खाड़ी युद्ध में फिर भी हम बचे रहे थे। मीलों की दूरी थी, नस्ल और जात, देश और समूह का भी अंतर था, यह दीगर बात है कि उस समय भी बच्चों का नाम सद्दाम रखने वाले लोग मौजूद थे और उनके समर्थन में भारत की गलियों में भी पोस्टरबाजी हो रही थी। करगिल के समय 24 घंटे चलने वाली मूर्खता हमारे देश में उरूज पर पहुंची और चूंकि मामला देश का था, इसलिए ‘देशभक्ति’ और ‘खून का उबाल’ चरम पर था। युद्ध हमारे ‘एंटरटेनमेंट’ का सामान था और ताबूतों में घर लौटते सैनिक महज एक नंबर, एक आंकड़ा।
इस बार कोरोना की दूसरी लहर में सोशल मीडिया पर ‘लाइव मौत’ चल रही है। फेसबुक हो या ट्विटर, टाइमलाइन जैसे मौत का बुलेटिन बन चुकी है। कल एक वाट्सएप ग्रुप में एक दोस्त की गंभीर बीमारी की सूचना दी गयी, साथ ही बचाने की गुहार भी लगायी गयी। पूरे चार घंटों तक उस समूह में बुद्धि-विलास होता रहा, तमाम नंबर्स और उपाय शेयर हुए- काढ़ा से लेकर प्रोन ब्रीदिंग तक के तरीके बताए गए। नहीं हुआ, तो किसी भले आदमी द्वारा नोएडा जाकर पीड़ित के साथ खड़ा होना नहीं हुआ। यह बात एक बदलते समाज और भविष्य के तौर पर रेखांकित करने योग्य है।
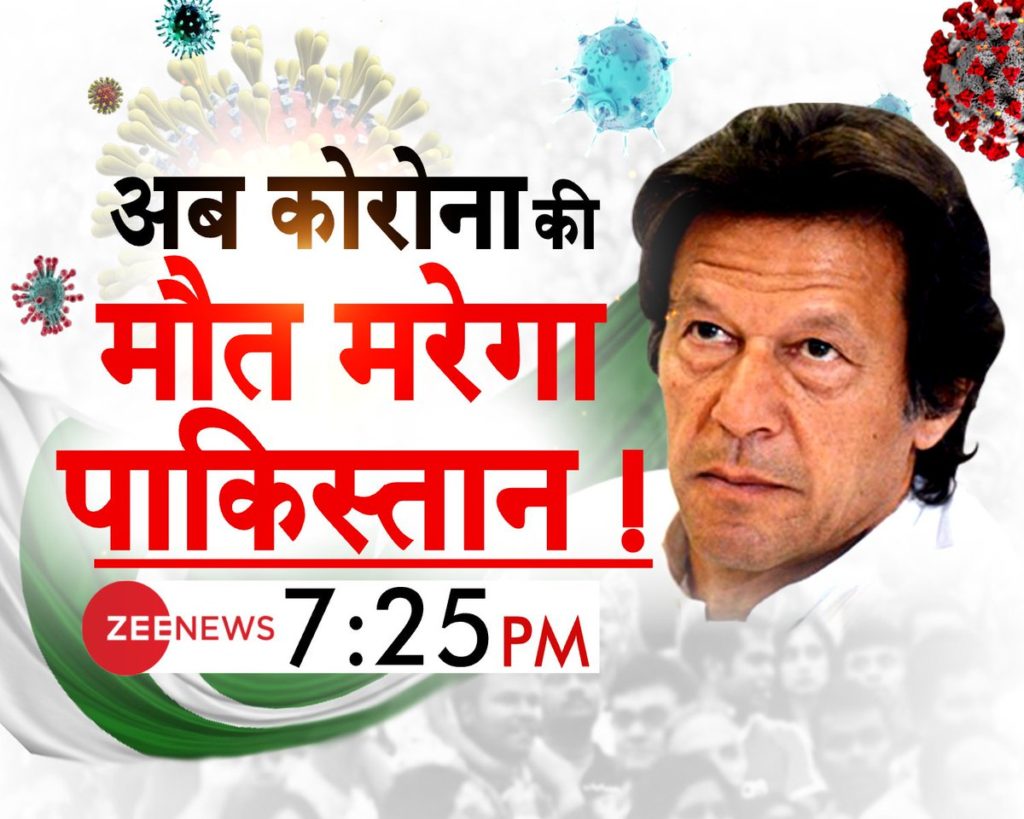
महामारी के इस दौर में न्यूज़ चैनल्स का रवैया देखकर पत्रकारिता के पतन को भी आप पारिभाषित नहीं कर सकते हैं। तकनीक की अबाध और सुगम पहुंच ने घर-घर में इन 24 घंटे चलने वाली ‘थियेट्रिक्स’ की दुकानों को तो पहुंचा दिया, लेकिन पत्रकारिता के सबसे जरूरी आयाम ‘ख़बर’ की ही भ्रूण-हत्या कर दी गयी। अब कहीं भी कुछ भी बचा है, तो वो है प्रोपैगैंडा, फेक न्यूज़ और कम से कम ‘व्यूज़’। समाचार कहीं नहीं हैं, विचार के नाम पर कुछ भी गलीज़ परोसा जा रहा है।
हमारी पत्रकारिता बिल्कुल हमारे उस नागरिक की तरह हो गयी है, जो मास्क लगाने को कहने पर अपने ‘यूपीएससी मेंस लिखने’ का हवाला देती है, जिसको अधिकार तो अबाध चाहिए, लेकिन कर्तव्यों के नाम पर उसका माथा फिर जाता है, जिसके लिए पत्रकारिता का मतलब ‘पास’ का जुगाड़ करना और संबंधों की धौंस जमाना है।
वस्तुनिष्ठता एक मिथ भले हो, लेकिन पत्रकारिता का आदर्श ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग ही है, वह जितना भी संभव हो सके। तथ्यों के संप्रेषण और वस्तुस्थिति की सही जानकारी देना एक पत्रकार का कर्तव्य है, इसमें दो राय नहीं हो सकते, किंतु उसके नाम पर इस महामारी की स्थिति में ‘पैनिक’ फैलाना और ‘फेक न्यूज़’ परोसना कौन सी पत्रकारिता है? वैसे तो दर्जनों उदाहरण हैं, लेकिन महज कुछ उदाहरण देकर इसको और साफ किया जा सकता है।
एक दिन पहले शशि थरूर ने लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ‘ताई’ को मार दिया, उन्हें अपने ट्वीट में श्रद्धांजलि दे दी। अखबारों और चैनल्स ने कागा के नकबेसर लेकर भागने के पीछे दौड़ लगायी और कुछ ही देर में ताई ट्रेंड कर रही थीं, राष्ट्रीय ख़बर थीं। किसी भी अभागे जर्नलिस्ट ने इस ख़बर को कंफर्म करने की जहमत नहीं उठायी। बाद में, सुमित्रा ताई ने जो खंडन किया है, उसे सुनने के बाद आपको लगता है कि जब उन जैसी ताकतवर महिला का इस देश में तथाकथित पत्रकारिता यह हाल कर सकती है, तो बाकी का क्या हाल होगा?
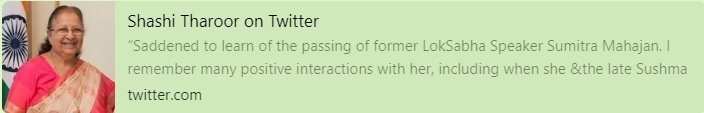
गंगाराम अस्पताल में दर्जनों मरीजों के बिना ऑक्सीजन मौत की ख़बर जब कई मीडिया-संस्थानों ने चला दी, तो खुद अस्पताल के चेयरमैन को एएनआइ को बाइट देकर उसका खंडन करना पड़ा। थरूर ने अभी अपनी ट्वीट हटा ली, मीडिया संस्थानों ने ख़बर हटाई भी हो तो उनको सज़ा क्या मिली, पता नहीं।

महामारी और आपाताकाल के इस दौर में हरेक नागरिक से उच्चतर और संयत व्यवहार की अपेक्षा है। पत्रकार भी प्रथमतः और अंततः नागरिक ही तो हैं। हो इसका उल्टा रहा है। अराजकता, अफरातफरी और आपराधिक लापरवाही के ही हमें यत्र-तत्र-सर्वत्र दर्शन हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि पत्रकारों को कभी अनैतिक पत्रकारिता के लिए दंडित नहीं किया गया। इनमें से कुछ ने तो संस्थागत पत्रकारिता छोड़ के अपनी स्वतंत्र राह पकड़ ली और आज जो पत्रकारिता वे कर रहे हैं, ऐसा लगता है उनके अतीत का रेचनकर्म है। इन्हीं में एक हैं ‘राडिया टेप फ़ेम’ बरखा दत्त, जो सूरत से लेकर गाजियाबाद तक के श्मशानों से लाइव पत्रकारिता कर रही हैं जबकि उनकी टीम के चार लोग खुद कोविड पाज़िटिव निकल चुके हैं और खुद उनके पिता अस्पताल में भर्ती हैं।
दूसरी ओर ज्यादातर अनैतिकता की राह पर आगे बढ़ते रहे और जेल होकर भी आ गए। ऐसे पत्रकारों को समाज और पत्रकार बिरादरी अस्वीकार कर देती ऐसा तो कभी नहीं हुआ, उलटे वसूलीबाज़, जेल रिटर्न पत्रकारों को गोयनका दिया जाता रहा जिससे वे नवतुरियों के आदर्श बनते रहे। जिन्हें पत्रकारिता के पुरस्कार लायक नहीं समझा गया लेकिन स्वामिभक्ति के चलते पुरस्कार देना अनिवार्यता थी, उन्हें साहित्यकार बना दिया गया। इसका इकलौता उदाहरण आलोक मेहता हैं, जिनका एक ट्वीट आजकल चौतरफा गाली खा रहा है।
पत्रकारिता की दुकान चला रहे लोगों को पता है कि वे कुछ भी (मतलब, कुछ भी) लिख, बोल सकते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिम्मेदारी और कर्तव्यबोध का सख्त अभाव और अनैतिकता पर दंड की कमी इस बीमारी को और गंभीर बना रही है। ऊपर से कुछ पत्रकारों की सत्ताजनित अहंम्मन्यता ने जिस तरह संस्थानों का कबाड़ा किया है, उसका कोई सानी समकालीन दुनिया में खोजना मुश्किल है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सर्वोच्च अदालत प्राथमिकता के आधार पर अरनब गोस्वामी की ज़मानत पर सुनवाई कर लेती है लेकिन देश भर में तांडव मचा रही ऑक्सीजन की कमी का मसला हफ्ते भर के लिए टाल दिया जाता है?
हॉलीवुड की एक फिल्म है, ‘ट्रुथ’। यह 2004 में सीबीएस (न्यूज चैनल) के एक कार्यक्रम ‘सिक्सटी मिनट्स’ में बुश के मिलिट्री ड्यूटी न करने का समाचार प्रसारित करने और फिर उसके परिणामों के बारे में है। बुश ने वियतनाम दौरे से बचने के लिए पैरवी के जरिये अपनी ड्यूटी नेशनल गार्ड्स में लगवा ली थी, जैसा उस समय अमेरिका के कई रसूखदार घरों ने किया था, ऐसा सिक्सटी मिनट्स में दिखाया गया है (वैसे, राजीव गांधी के बारे में भी आरोप है कि भारत-पाक युद्ध के समय सेना में पायलट की ड्यूटी से बचने के लिए उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस पर कोई बात भारत में नहीं होती है)। फिल्म में यही दिखाया गया है कि एक सूत्र पर आधारित ख़बर को जब कई तरह से ‘वेरिफाई’ नहीं किया गया, तो शो की प्रोड्यूसर ‘मेरी मेप्स’ और एंकर ‘डैन रादर’ को अपने करियर खोने पड़े थे। ध्यान रखिएगा कि ये मेरी मेप्स वही हैं, जिन्होंने अबू गरीब के जेलों की रिपोर्ट को दुनिया के सामने उजागर किया था और उससे कितना हंगामा मचा था।
फिल्म में तथ्यों और पत्रकारिता का जो तानाबाना है, उसमें डैन रादर की भूमिका निभा रहे रॉबर्ट रेडफोर्ड का एक डायलॉग खासा भारी है, ‘सवाल यह नहीं कि तुम्हें और मुझे क्या लगता है, सवाल यह है कि तथ्य क्या हैं’? तथ्य पवित्र हैं, इनका घालमेल कभी भी भावनाओं, विचारों और पूर्वग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए और यही पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा है। भारत में शायद यह रेखा कभी रही ही नहीं और अगर कभी रही, तो आज तो उसकी धज्जियां बिखेर दी गयी हैं।
पिछले एक साल में कोविड से निबटने के लिए तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने क्या किया, कहां कमियां रहीं, कहां क्या उपाय रहे, इन सभी पर ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग वक्त की मांग है। दुर्भाग्य से हमारे देश में जिन भी हाथों ने माइक या की-बोर्ड संभाल रखा है, वे सभी किसी न किसी के भोंपू हैं और पत्रकारिता के बुनियादी सबक से भी महरूम हैं।
रवीश कुमार के शो में माइम-आर्टिस्ट की मौजूदगी से लेकर रिपब्लिक चैनल के एंकर के सड़कों पर नाचने और बरखा दत्त के श्मशान में बैठने तक, पत्रकारिता अब केवल थियेट्रिक्स और ड्रामैटिक्स का पंचमेल बनकर रह गयी है। इसका स्मृति-लेख कब का लिखा जा चुका है।

कवर तस्वीर बरखा दत्त की ट्विटर टाइमलाइन से साभार प्रकाशित है




