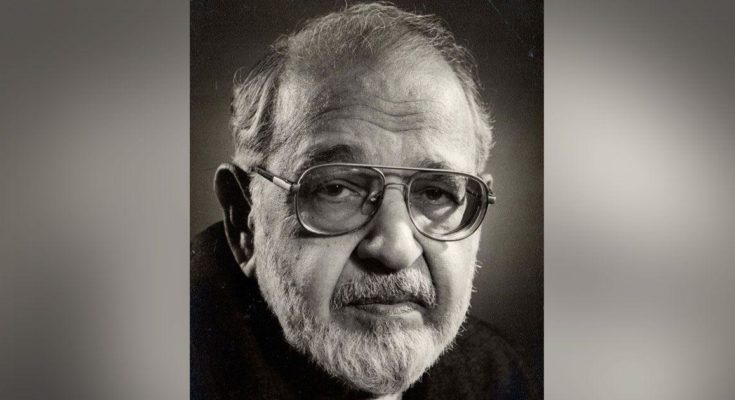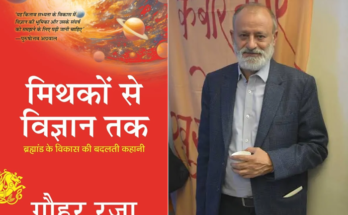हम लोगों ने साहित्य-संसार में जब आँखें खोलीं तब अज्ञेयजी (7 मार्च 1911- 4 अप्रैल 1987) इसके दैदीप्यमान नक्षत्र थे। हाई स्कूल में इनकी एक कहानी मैंने पढ़ी थी, शीर्षक था- ‘शत्रु’। हमारे हिन्दी शिक्षक पर अज्ञेय का इतना अधिक प्रभाव था कि कहानी के बहाने वह उनके कृतित्व पर एक लम्बा भाषण दे गए, जिसमें उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘शेखर: एक जीवनी’ का सार-संक्षेप भी शामिल था। हमारे शिक्षक को यह पता था कि वह जो कह रहे हैं, इन विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का शायद नहीं है, लेकिन वह किंचित अपने ही सुख के लिए कहे जा रहे थे। मेरे गुरु की मान्यता थी कि शिक्षक का काम पढ़ाना इसी अर्थ में है कि वह छात्रों को विषय के प्रति जिज्ञासु बना दे। कम-से-कम मैं अज्ञेय के प्रति जिज्ञासु हो चुका था।
अज्ञेय से मेरा प्रथम परिचय इसी तरह हुआ था। गुरु-मन्त्र द्वारा। शीघ्र ही मैंने उनकी कुछ किताबें ढूँढ लीं और मैट्रिक की परीक्षा देने के कुछ ही समय बाद उनके उपन्यास “शेखर: एक जीवनी” का पारायण-पाठ कर गया। किसी भी कृति का पहला पाठ उसके मूल्यांकन का समृद्ध आधार नहीं हो सकता। मैंने कितना समझा, नहीं समझा, यह भी नहीं कह सकता; लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं इस नतीजे पर अवश्य आया कि यह लेखक कुछ अलग है।
उन्हीं दिनों मैथिलीशरण गुप्त के भाई सियारामशरण गुप्त द्वारा सम्पादित कवि सीरीज़ की पुस्तिकाओं में से अज्ञेय पर केंद्रित पुस्तिका मेरे हाथ लगी और उनके कवि-कर्म या कविताओं पर भी कुछ जान सका। मैं साइंस का छात्र था। स्नातक स्तर पर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मेरे विषय थे। किसी भाषा के साहित्य से मेरा विश्वविद्यालयी रिश्ता नहीं था। इसलिए साहित्य को मेरी हॉबी ही कह सकते हैं। ऐसे में मैंने जब यह जाना कि अज्ञेय स्वयं साइंस के ही छात्र थे, तब मेरा स्वयं पर भरोसा हुआ कि मैं भी लेखक हो सकता हूँ। यह उनसे एक अतिरिक्त लगाव का कारण था। मेरे मन पर अज्ञेय की सतरंगी छतरी तन चुकी थी; इसकी अनुभूति मुझे हो न हो, उनके प्रति एक आकर्षण, जिसे मैं ललक कहना पसंद करूँगा, मेरे भीतर अवश्य विकसित हो चुकी थी। इसी ट्रांस में उनकी सभी प्रमुख किताबें पढ़ गया। “नदी के द्वीप”, “अपने-अपने अजनबी” तार-सप्तक की चार में से तीन जिल्दें और कुछ कविता संकलन।

लेकिन वह जमाना प्रगतिवादी था। पटना आया तब प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा और उसकी गतिविधियों में भाग लेने लगा। पटना उन दिनों आज की तरह खाली-खाली नहीं था। रेणु, नागार्जुन, प्रफुलचन्द्र ओझा मुक्त, कन्हैया जैसे लोग यहां रहते थे। सबके इर्द-गिर्द एक-एक साहित्यिक घेरा था और फिर सब मिलकर एक बड़ी उपस्थिति बनती थी। तब साहित्य आज जितना अप्रासंगिक भी नहीं हुआ था। बड़े-बड़े लेखक यहां आते रहते थे और छोटी-बड़ी साहित्यिक गोष्ठियों का सिलसिला बना रहता था। लेकिन यह सच्चाई थी कि प्रगतिवादी समूह थोड़ी अकड़ में होते थे। उन्हें महसूस होता था हमारा सच दूसरे के सच से अधिक खरा है, अतएव हम ही समाज के उन्नायक हैं। जो हमसे पृथक हैं वे दक्षिणपंथी और विचारों से कमतर लोग हैं। जैसे आज दक्षिणपंथी शक्तियां जवाहरलाल नेहरू और कम्युनिस्टों आदि के बारे में अनाप-शनाप किस्से गढ़ती रहती हैं, वैसे ही उन दिनों अज्ञेय के बारे में प्रगतिवादी खेमे के लोग किस्से गढ़ते रहते थे। मानो अज्ञेय भारत में अमेरिका और दुनिया भर के पूंजीवादियों के सांस्कृतिक जासूस हों। अज्ञेय का विराट-मौन इन सब धारणाओं को पुष्ट करता था। अब महसूस होता है वह इनका आनंद लेते थे।
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यानी वैचारिक शीतयुद्ध के ज़माने में कहा जाता था कि विचारों की पूरी दुनिया दो भागों में बँटी है। या तो लोग मार्क्सवादी हैं या फिर मार्क्सवाद विरोधी। हिंदी साहित्य में उन दिनों यह कहा जा सकता था कि या तो आप अज्ञेय के पक्ष में हैं या फिर उनके विरोध में। प्रगतिवादियों के पास जितना अपने पक्ष में कहने के लिए था, उससे अधिक अज्ञेय के विरोध में कहने के लिए था। जो जितना अज्ञेय के विरुद्ध है, वह उतना ही प्रगतिशील है, ऐसी मान्यता थी। ऐसे माहौल में एक मूक-मौन साधक की तरह अज्ञेय चुपचाप काम करते रहे। वह किस मानसिकता में जीते होंगे, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। एक बड़े और सक्रिय साहित्यिक समूह के इस इकतरफा विरोध को उन्होंने पूँजी नहीं बनाई, बस एक ‘सात्विक-उपेक्षा’ से नजरअंदाज भर करने की भरसक कोशिश की। उन्होंने अपने लेखन और व्यक्तित्व को प्रतिक्रियावादी कुंठा के गिरफ्त में आने से लम्बे समय तक रोका, लेकिन यह भी सच था कि आखिरी दिनों में उनके पास एक दकियानूसी घेरा घिर आया था। जिस अज्ञेय के इर्द -गिर्द कभी हिंदी साहित्य और समाज का श्रेष्ठ हुआ करता था, अब कुछ ऐसे लोग थे जिनका साहित्य में कोई खास अवदान नहीं था, हालांकि मान-सम्मान और पुरस्कारों की उन्हें कभी कोई कमी नहीं हुई और चर्चा से भी कभी विलग नहीं किये जा सके। सब मिला कर एक किंवदंती-पुरुष बने रहे, लेकिन कहीं कोई रिक्तता उन्होंने अवश्य महसूस की होगी जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने अपने इर्द-गिर्द एक ‘भीड़’ विकसित करने की कोशिश की। हमारे समाज में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत नहीं हुई है। जब यह होगा, इन कारणों की समीक्षा संभव होगी।
मैं कभी उनके निकट नहीं हो सका। दो अनमोल मुलाकातें जरूर हैं। एक तो पटना के डाकबंगला चौराहे पर अकस्मात और दूसरा दिल्ली में कवि रघुवीर सहाय जी के साथ। केवल दो मुलाकातों से किसी की तस्वीर बनाना मुश्किल है, लेकिन इतना कह सकता हूँ वह भीड़ की भाषा और फैसलों के विरुद्ध रहते थे। तब भी जब वह अपने ही द्वारा सृजित भीड़ से घिरे होते थे। इसीलिए उन्हें समझना मुश्किल होता था। उन्होंने कभी इस या उस की टिप्पणियों या आलोचना की परवाह नहीं की। इसीलिए उन्हें साहित्यिक मठों के समर्थन की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें यह पता था कि वह क्या करने आये हैं और उनके लिए साहित्य का मकसद क्या है। दुनिया भर में साहित्य ने सूक्ष्म से विराट की यात्रा की है और साहित्य का जनतंत्र इसी अर्थ में अजूबा है कि उसे भीड़ और वोट की दरकार नहीं होती। एक सच्चा लेखक मनुष्य की आज़ादी का पहरेदार होता है, उसकी आज़ादी के फलसफे का प्रस्तावक भी। जब वह भीड़ की भाषा या मिजाज अपनाता है, तब अनैतिक हो जाता है। अज्ञेय इससे भरसक बचते रहे। यही उनकी विशिष्टता थी, पहचान भी।

अज्ञेय हिंदी के लेखक थे और उनकी सांस्कृतिक पहचान की जड़ें उत्तर भारत में थीं। गंगा, गीता और गौ माता से घिरे उस आर्यावर्त में, जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन घनीभूत था और स्वयं अज्ञेय भी जुझारू राष्ट्रवाद की उस धारा से जुड़े थे जो एक समय बम-बारूद के ढाँचे पर खड़ा था। इस धारा से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वह निकलते हैं। वह रेनेसां की उस धारा से जुड़ते हैं जिसकी पहचान हिंदी में बहुत कम थी। इसीलिए न वह छायावादी-उत्तरछायावादी चेतना से जुड़े दीखते हैं, न प्रगतिवादी चेतना से। कबीर की तरह शहर बाहर मवास पर बसे-टिके दीखते हैं। सबसे अलग-थलग।
यूरोपीय रेनेसां का मुख्य चरित्र ज्ञान से विज्ञान की ओर संचरण रहा है। यह शास्त्र और समाज की मान्यताओं का निषेध करता रहा है। भारतीय समाज में नवजागरण के उन्नायक राजा राममोहन राय ने भी यही किया। उन्होंने भीड़ की आवाज नहीं सुनी, शास्त्रीय मान्यताओं, प्रचलनों और देव-वाणियों का निषेध किया। पीड़ित स्त्रियों की पीड़ा सुनी और तमाम विरोधों के होते उनके पक्ष में अकेले खड़े हो गए। जोतिबा फुले ने स्त्रियों के साथ अद्विजों-दलितों, किसानों और दस्तकारों को जोड़ा। उनके पक्ष में सभी शास्त्रों, देवी-देवताओं के विरुद्ध तन कर खड़े हो गए। रानाडे, आंबेडकर, नायकर आदि यही करते रहे। आधुनिक साहित्य में रवीन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, जैनेन्द्र आदि ने इस चेतना को रेखांकित किया। सबसे ऊपर मनुष्य का सत्य है, इससे ऊपर कुछ नहीं। भक्तिकालीन संत चंडीदास का उद्घोष आधुनिक साहित्य का मुख्य स्वर हो गया। अज्ञेय इसी धारा से जुड़े। यह धारा प्रगतिवादी खेमे की भी थी, लेकिन उनसे अलग अज्ञेय की यह विशिष्टता रही कि इसमें मार्क्सवादी बैनर नहीं लगने दिया, हालांकि वैचारिक रूप से ऐसे तो अवश्य ही रहे कि मानवेंद्रनाथ राय और जयप्रकाश नारायण जैसे धुरंधर मार्क्सवादियों से उनकी निकटता रही।
उनका लिखना उस दौर में शुरू हुआ जब यहां राष्ट्रीय आंदोलन घनीभूत था, लेकिन इसका कोहराम उनकी रचनाओं में कम ही मिलता है। उनके उपन्यास ‘शेखर: एक जीवनी’ का शेखर नास्तिक है, वह मुल्क की आज़ादी के लिए नहीं अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। सब कुछ उसके विरुद्ध है। परम्परा, घर, रिवाज और सामाजिक ढांचे के विरुद्ध वह इंकलाब करना चाहता है। उसकी यह आज़ादी मुल्क की आज़ादी से कहीं गंभीर और महत्वपूर्ण है। जब यह उपन्यास लिखा जा रहा था तब मुल्क के नौजवान अपने दिलों में भगत सिंह की यादें लिए राजनैतिक आज़ादी के फलसफे लिख रहे थे, लेकिन अज्ञेय का नायक शेखर अपने ही अभिजात ब्राह्मणवादी संस्कारों से जूझ रहा है। उसका संघर्ष बाहर का नहीं, अंदर का है। अज्ञेय जानते थे असली आज़ादी समाज और व्यक्ति की है। संविधान आत्मसात करते वक़्त संविधान सभा में आंबेडकर ने अपने भाषण में इसी भाव को व्यक्त किया था।
अज्ञेय को हिंदी साहित्य के प्रचलित मुहावरों में समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। वह राष्ट्र तो उनके यहां पूरी तरह अनुपस्थित है, जिसे लेकर हिंदी काव्य साहित्य में अतिरिक्त सतर्कता बरती गयी। प्रगतिवादी दौर में इतना ही अंतर आया कि राष्ट्र परिवर्तित अथवा विस्तृत होकर जन बन गया। राष्ट्र और जन दो ऐसे आधुनिक रक्तपिपासु देवता बने जिसके नाम पर किसी भी देवता से अधिक बलिदान हुए। इन दोनों में किसी को विरोधाभास दिख सकता है, किन्तु अज्ञेय इनके अन्तर्सम्बन्धों को पहचान रहे होते हैं। 1909 ई. में लिखे अपने एक उपन्यास “गोरा” में रवीन्द्रनाथ टैगोर का नायक गोरा इस समस्या से जूझ रहा होता है। राष्ट्र की कामना में वह लगातार संकीर्ण और संवेदनहीन बनता गया है। पवित्र और शुद्ध की तलाश में वह निरंतर अपवित्र और अपावन होता गया है। उसमें अपने राष्ट्र और जाति (जन्म-कुक्षि) का अभिमान विकसित होता है। इसी जात्याभिमान के केन्द्राभिसारी स्वरूप में उसका व्यक्तित्व भी विकसित हो रहा है। स्वयं पर अभिमान और अन्य से घृणा की पूँजी पर विकसित हो रहे विचार पवित्रता और घृणा का निरंतर उद्घोष कर रहे होते हैं। अंततः उसे ज्ञात होता है कि वह तो जन्म से ही म्लेच्छ है। जन्मना अपवित्र और अपावन है। और उसी रोज उसे अपने पवित्रतावादी संस्कारों से मुक्ति मिलती है। उसकी म्लेच्छता उसके लिए हर एक का द्वार खोल देती है, उसे सम्पूर्ण रूप से पावन बना। देती है। अब उसे जात-पात और विधर्म भाव से मुक्ति मिल गयी है।

अज्ञेय का शेखर इसी तरह कुछ भिन्न अर्थों में मुक्त होता है। वह आत्मसंघर्ष करता है क्योंकि बड़ी गुलामी उसके मन के भीतर है। उसे इन संस्कारों से आज़ादी चाहिए। ये संस्कार ब्राह्मणत्व के भी हैं और पुरुष के भी, इन आडम्बरों को उतार फेंकना उसकी प्राथमिकता होती है। यह अकारण नहीं है कि अज्ञेय ने टैगोर के ‘गोरा’ का बंगला से हिंदी और जैनेन्द्र कुमार के ‘त्यागपत्र’ का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इनके अनुवाद उन्होंने जीविका के लिए नहीं किये थे। ये दोनों उपन्यास अज्ञेय को पसंद हैं तो इसके आधार हैं। ‘गोरा’, ‘त्यागपत्र’ और ‘शेखर: एक जीवनी’ की एक त्रयी बन सकती है। गौरचंद्र मुखर्जी, शेखर और मृणाल एक ही पीड़ा से जुड़े हैं। उनका संघर्ष अपनी निजता के लिए है। राष्ट्र, समाज और परिवार की पवित्रता और अस्मिता की वेदी पर उनकी गुलामी के फलसफे लिखे जा रहे हैं। इसकी बेड़ियाँ तोडना एक पारम्परिक समाज में मुश्किल है। इसलिए ये तीनों परंपरा से एक मौन-विद्रोह करते हैं, लेकिन उनके विद्रोह इतने सकारात्मक हैं कि अंततः वही परंपरा के परिष्कार अथवा विकास भी बन जाते हैं।
अज्ञेय ने आत्मकथा नहीं लिखी। उन्होंने राजी सेठ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है- ‘आत्मकथा में झूठ लिखना ज्यादा आसान है, उपन्यास में सच लिखना ज्यादा आसान है।’ अपने उपन्यास ‘शेखर: एक जीवनी’ में उन्होंने आसानी से अपने सच को रखा है। उनके आत्मसंघर्ष को यहाँ समझा जा सकता है, हालांकि उनका सच साहित्य का एक जटिल प्रश्न बन गया जिसके उत्तर आज भी तलाशे जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि शेखर और अज्ञेय एक ही हैं या यह आत्मकथात्मक उपन्यास है। मैं साहित्यिक कृतियों के इतने सरलीकरण के पक्ष में नहीं होना चाहूँगा, लेकिन एक तथ्य तो है ही कि अज्ञेय का अपना जीवन भी कुछ-कुछ जादुई यथार्थ लिए हुए है। जैसे उनका जन्म। इधर-उधर न जाकर मैं सीधे अज्ञेय को ही रखता हूँ-
मेरा जन्म ही खुले खेत में हुआ, अक्षरशः खुले खेत में। मेरे पिता पुरातत्ववेत्ता थे और कुशीनगर की खुदाई करवा रहे थे, तो एक छोटे से तम्बू में तब रहते थे। उस समय जब मेरा जन्म हुआ तो माँ तो वहां थी ही, एक मेरी अविवाहिता बुआ थीं उनके पास और मेरी बड़ी बहन भी, अविवाहिता बहन। उनके साथ उस समय और कोई नहीं था। तो कुछ संकोच कहिए या जो भी कारण कहिये वे वहां से बाहर खेत में चली गईं, वहां मेरा जन्म हुआ।
कवि रघुवीर सहाय को दिए इस इंटरव्यू को देखने के पूर्व मेरे मन में अज्ञेय के प्रति एक शिकायत थी कि शेखर जैसा नास्तिक नायक खड़ा करने वाला लेखक अपने जीवन के आखिरी दौर में जानकी जीवन यात्रा पर कैसे निकल गया? इस बाबत मैंने उनके जीवनकाल में ही एक टिप्पणी भी लिखी थी और जैसा कि ऐसी टिप्पणियों की चर्चा होती है उसकी भी हुई थी, लेकिन उनकी जन्मकथा को जानकर जानकी जीवन यात्रा के प्रति लेखक की भावना को समझ पाया। पौराणिक जानकी सीता का जन्म भी खेत में हुआ था यह कथा है। सीता से इस बहनापे के कारण ही अज्ञेय के मन में जानकी के प्रति आकर्षण उमड़ा होगा। इस भाव के आते ही मैं भीग गया। कहा न! अज्ञेय को समझना थोड़ा मुश्किल तो है।
अज्ञेय जब लिख रहे थे तब हमारे राजनैतिक क्षितिज पर दो राष्ट्र ही नहीं उभर रहे थे, हमारे काव्य जगत में भी दो राष्ट्रकवि एक साथ विराजमान थे (बल्कि इसे लेकर वह मजाक किया करते थे कि हमारे यहां राष्ट्रकवि (गुप्तजी) हैं, उपराष्ट्रकवि (दिनकर) हैं, धृतराष्ट्रकवि (धर्मवीर भारती ) हैं और परराष्ट्रकवि (माचवे) भी हैं।) अज्ञेय दिनकर को गहरे स्तर पर नापसंद करते थे। इसका विवरण स्मृतिलेखा के उनके लेख से मिल जाता है, लेकिन गुप्तजी को वह गुरु मानते थे। चरण-स्पर्श करते थे। इसके साथ ही निराला के व्यक्तित्व को महान स्वीकारते हुए भी वह उनके काव्य के प्रति शंकित होते थे। निराला पर उनका एक अंग्रेजी लेख जो विश्वभारती क्वार्टरली में विश्वयुद्ध के इर्द-गिर्द छपा था, चर्चित भी हुआ था। शीर्षक था ‘निराला इज़ डेड’।

निराला बंगाल में पैदा हुए और उनके मानस का कुछ भाग वहीँ निर्मित हुआ। उन्होंने कृतिवास रामायण से राम की शक्ति पूजा की पृष्ठभूमि तो ग्रहण कर ली, लेकिन बंगला नवजागरण के संस्कार ग्रहण नहीं कर सके। एक आक्रामक हिंदुत्व निराला की कविता में चुपचाप छुपा होता है, हालांकि वह गुप्त जी के मुकाबले क्रान्तिकारी-प्रगतिशील दीखते हैं। गुप्त जी बात-बात में राम को गुहराते हैं, निराला ऐसे नहीं हैं। राम की शक्ति पूजा के राम इतने मानवीय और आधुनिक दीखते हैं कि निराला पर प्रथमदृष्टया हिंदुत्ववादी होने का आरोप लगाते सौ बार सोचना पड़ता है, लेकिन गुप्त जी का हिंदुत्व आक्रामक नहीं है। वह उस भागवत-वैष्णव हिंदुत्व को रेखांकित करते हैं जो अपने हिंदुत्व पर न शर्म करता है न गर्व। वह अन्य धर्मों के प्रति भी कोई बैर नहीं रखता। निराला का हिंदुत्व किंचित डींग मारता है। उसमें आक्रामकता है। इसीलिए अज्ञेय उसे नापसंद करते हैं। यह एक अद्भुत विरोधाभास है कि अज्ञेय, निराला की कृति तुलसीदास के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण और महान मानते हैं।
अज्ञेय साहित्यालोचक नहीं थे, लेकिन समकालीन कविता की उनकी समझ कितनी पैनी थी इसे तारसप्तक संकलनों के चयन से परखा जा सकता है। आखिरी सप्तक के अलावे तीनों सप्तक छायावादोत्तर आधुनिक हिंदी कविता के रैखिक विकास को व्यवस्थित करते हैं। हिंदी कविता के बारे में उन्होंने निबंध रूप में कुछ लिखा है या नहीं यह नहीं जानता, लेकिन उनकी छिटपुट टिप्पणियां महत्व रखती हैं। वह स्वयं कवि थे और जब भी उन्होंने कविता को देखा तो उसे बाहर से नहीं, भीतर से देखा। आधुनिक कविता अनेक स्तरों पर उन उपकरणों से नहीं समझी या आत्मसात की जा सकती, जिन उपकरणों से संस्कृत का काव्य समझा गया था। उन्होंने इस समस्या को अत्यंत सूक्ष्म अथवा बारीक़ अंदाज में समझा है। एक जगह वह लिखते हैं-
एक समय था जब कि काव्य एक छोटे-से समाज की थाती थी। उस समाज के सभी सदस्यों का जीवन एकरूप होता था, अतः उनकी विचार संयोजनाओं के सूत्र भी बहुत कुछ मिलते-जुलते थे- कोई एक शब्द उन के मन में प्रायः सामान चित्र या विचार या भाव उत्पन्न करता था। इस एक का संकेत इसी बात से मिलता है कि आचार्यों ने काव्य-विषयों का वर्गीकरण संभव पाया, अउ कवि को मार्ग-दर्शन करने के लिए बता सके कि अमुक प्रसंग में अमुक-अमुक वस्तुओं का वर्णन या चित्रण करने से सफलता मिल सकेगी। आज यह बात सच नहीं रही। आज काव्य के पाठकों की जीवन-परिपाटियों में घोर वैषम्य हो सकता है; एक ही सामाजिक स्तर के दो पाठकों की जीवन-परिपाटियाँ इतनी भिन्न हो सकती हैं कि उन की विचार-संयोजनाओं में समानता हो ही नहीं, ऐसे शब्द बहुत कम हों जिन से दोनों के मन में एक ही प्रकार के चित्र या भाव उदित हों।” (तार सप्तक में उनका वक्तव्य)
अपने काव्य में अपने समकालीन हिन्दी कवियों से अलग उनमें बड़बोलेपन का नितांत अभाव है। कविता हो या कि गद्य विधा, उनके साहित्य का संधान बस जीवन रहा। अध्यात्म या राष्ट्र या राजनीति उनके अनुसन्धान विषय शायद ही बन सके। इन विषयों पर जब भी उन्हें लिखना हुआ, लेखों में लिखा। दिनमान का संपादन करते हुए उन्होंने लोहिया के जीवनकाल में ही उनके नेहरू विरोध की अपने सम्पादकीय वक्तव्य में ऐसी-तैसी कर दी थी। 8 दिसम्बर, 1968 में उनके सम्पादकीय (दिनमान साप्ताहिक) का शीर्षक है ‘हिंदुत्व की परिभाषा’। इस लेख में उन ने खुले और सगुण स्वर में आरएसएस के संकीर्ण सोच की बखिया उधेड़ दी है। लेकिन अपने काव्य या साहित्य को उन ने दूसरे कई प्रगतिशील कवियों की तरह राजनीति का मंच नहीं बनने दिया। अपने तीनों उपन्यासों में भी उन्होंने बस जीवन की खोज की है। बहुत आर्थिक संघर्ष उनके जीवन में नहीं रहा, लेकिन अपने इर्द-गिर्द एक आवारगी को उन्होंने विकसित होने दिया। आम हिन्दी कवियों की तरह उन्होंने अपने जीवन संघर्ष का कभी रोना नहीं रोया। साहित्य के अतिरिक्त किसी अन्य तरह के टोटे का इस्तेमाल कभी नहीं किया। न विचारधारा, न प्रतिबद्धता, न निज की दरिद्रता। अपने जीवन संघर्ष के लिए उन्होंने कई तरह के काम किये और उस से आनंद और स्फूर्ति ग्रहण किया; जैसे कबीर और रैदास ने मध्य युग में किया था। यह एक जटिल आधुनिकता बोध था, जिसे उन पर काम करने वाले लोगों ने भी कितना समझा है, नहीं जानता।
अपने समकालीन कवियों को समझने में भी उन्होंने पर्याप्त समय दिया। तार सप्तक श्रृंखला के चार संकलन इसके सबूत हैं। न केवल नए अपितु बड़े से बड़े और प्रसिद्धि प्राप्त कवियों को भी उन्होंने उन के काव्य के आधार पर ही महत्वपूर्ण माना। किसी प्रभाव में आकर कुछ कहना उन्होंने कभी नहीं जाना था। अपने आलेख के आखिर में समकालीन कुछ कवियों पर उनकी टिप्पणी उनके ही शब्दों में रखूँगा, जिसे उन्होंने रघुवीर सहाय से एक साक्षात्कार में कहा है-
पंत, निराला और बच्चन, इन तीनों से मेरा व्यक्तिगत परिचय, सम्बन्ध कह लीजिए रहा। प्रसाद जी को मैंने दो-तीन बार देखा, उनके घर भी गया। उनसे उनकी कविताएं भी सुनीं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनसे कोई निकट परिचय या सम्बन्ध रहा। महादेवी जी से भी इधर दो-चार वर्षों से, पहले कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं था। लेकिन यह व्यक्तिगत परिचय और सम्बन्ध की बात अपनी जगह है और कवि के रूप में उनके सम्मान की बात अपनी जगह। व्यक्तिगत परिचय होने से कवि के प्रति सम्मान के मामले में कुछ सुविधाएँ भी होती हैं, कुछ कठिनाइयां भी होती हैं। मैंने अभी कहा कि निराला को मैं महान व्यक्ति मानता था, अब भी मानता हूँ, और बहुत-सी बातों के बावजूद मानता हूँ। उस समय भी मानता रहा जब उनके काव्य के बारे में इतना आश्वस्त नहीं होता था। पंत जी को मैंने महान कभी नहीं माना, अब भी नहीं मानता हूँ। उनके काव्य के प्रति हमेशा मेरे मन में सम्मान का भाव रहा। बच्चनजी मेरी समझ में दोनों कोटियों में उन्नीस रहे हैं। व्यक्ति के रूप में कभी बहुत अधिक सम्मान मैं उनका नहीं कर पाया, उनके काव्य के कुछ गुणों का प्रशंसक था और हूँ, लेकिन इसको महान काव्य मैं नहीं मानता…।
अज्ञेय के अंतर्मन को समझने के लिए साक्षात्कार का यह अंश किन्ही स्तर पर सहायक हो सकता है। शायद नहीं भी हो सकता हो। इसलिए कि किसी पर कोई राय थोपी नहीं जा सकती, लेकिन सब मिला कर एकबार मैं यह जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि अज्ञेय को फिर से समझने की कोशिश की जानी चाहिए। आज जब दुनिया की राजनीति से शीतयुद्ध पूरी तरह खत्म हो गया है और मनुष्यता पर अन्य कई तरह के खतरे हावी हो रहे हैं, तब अज्ञेय अधिक साहस के साथ हमारे पक्ष में होंगे। वह हमें अपने भीतर झाँकने और खुद को समझने में सहयोग कर सकेंगे। अज्ञेय की खासियत यही है कि हर बार आप उन्हें एक ही रूप में अनुभव नहीं कर सकते। उनका साहित्य आप से एक रासायनिक अंतर्संबंध स्थापित करता है। यदि आप संवेदनशील हैं और थोड़े कम जिद्दी हैं यानी सहज हैं, तो वृहत्तर अर्थों में उनके काव्य की गुनगुनाहट आपके वजूद का हिस्सा हो जाने के लिए प्रयासरत अनुभव होगी।
प्रेम कुमार मणि वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं। यह टिप्पणी उनके फ़ेसबुक से साभार प्रकाशित है।