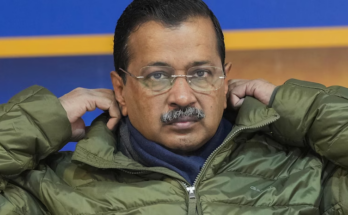दिल्ली में यमुना को देखकर आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? हो सकता है आपके मन में कोई खयाल आता ही न हो. आप नाले में बदल चुकी इस नदी को मरते हुए देखने के मौन गवाह बन रहे हों. मेट्रो से गुजरते हुए तो शायद बदबू नहीं आती, लेकिन अगर आप किसी सड़क पुल से इसको पार कर रहे होंगे तो कार का शीशा बंद करना जरूर सुनिश्चित करते होंगे.
बहरहाल, यमुना की यह दुर्दशा सुप्रीम कोर्ट की नजर में आई है. पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और याचिका लगाई थी दिल्ली जल बोर्ड ने. दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत हरियाणा सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा को न्याय मित्र नियुक्त किया है. दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश बोबडे की पीठ ने कहा कि पूरी यमुना में प्रदूषण पर हम स्वतः संज्ञान ले रहे हैं.
अब अदालत ने हरियाणा सरकार से मंगलवार तक जवाब मांगा है. उसी दिन अगली सुनवाई होनी है. दिल्ली जल बोर्ड की वकील अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा के ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं जिससे कारखानों का बगैर शोधित हुआ रासायनिक अपशिष्टों वाला जहरीला पानी सीधे यमुना में आ रहा है और इसमें अमोनिया काफी ज्यादा है, इससे यह पीने लायक नहीं बचता.
यह अच्छा है कि आखिर शीर्ष अदालत नदियों के प्रदूषण और उसकी हालत को लेकर जवाबदेही तय कर रही है. ज्यादा दिन नहीं बीते, टेलिविज़न पर आपने हहाती हुई यमुना का दृश्य जरूर देखा होगा. बरसात में यमुना का यौवन देखने लायक हो जाता है, लेकिन खबरिया चैनल यमुना के बढ़े हुए पानी को बाढ़ का खतरा या संकट बताते हैं. एक क्रैश कोर्स होना चाहिए जिसमें पत्रकारों को भी यह बताया जाना चाहिए कि नदियों में बाढ़ आना कोई अनहोनी नहीं है. बहुत कुदरती बात है यह. हर नदी में हर साल बाढ़ आती है और आनी ही चाहिए. लोगों को तर्क होता है कि दिल्ली में आखिर बाढ़ आए ही क्यों, जबकि बारिश तो उतनी होती नहीं यहां पर.
ऐसा कहने वाले लोग न तो नदियों के स्वभाव को जानते हैं न नदीतंत्र को समझते हैं. कैचमेंट और बेसिन जैसे शब्दों से अनजान लोग यमुना पर बने लोहे को पुल को यमुना के पानी घटने-बढ़ने का आधार बताते हैं.

बस, दिल्ली से पहले वजीराबाद बराज ही वह जगह है जहां पर यमुना का पानी काला नहीं होता. लेकिन वहां तो हम यमुना का करीबन सारा पानी रोक लेते हैं और उसके आगे जो पानी हमें दिखता है वह दिल्ली का सीवर है. उद्योगों और घरों का गंदा प्रदूषित पानी जो बिना ट्रीटमेंट के सीधे उसमें गिराया जाता है.
यमुना नदी की बदहाली वजीराबाद से ही शुरू हो जाती है. दिल्ली में वजीराबाद से ओखला बैराज के बीच की यह दूरी, दुनिया में किसी भी नदी की तुलना में यमुना के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. इसी हिस्से में यमुना सबसे अधिक प्रदूषित है.
आखिर यमुना को यूं ही वैज्ञानिक जैविक रेगिस्तान नहीं कहते. इसे भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी का शर्मनाक दर्जा मिला हुआ है. इसके पानी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और बायोमाइडस जैसे कृषि रसायनों की मौजूदगी में पिछले 25 वर्षों में चार गुना वृद्धि हुई है. देहरादून, यमुना नगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा और आगरा घरेलू और औद्योगिक कचरा सीधे यमुना में गिराते हैं. एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि हरियाणा की 22, दिल्ली की 42 और उत्तर प्रदेश की 17 फैक्टरियां यमुना में सीधे तरल कचरा बहाती हैं.
इसी हिस्से में आकर यमुना का पाट भी सिकुड़कर डेढ़ से तीन किलोमीटर चौड़ा रह जाता है. यमुना पर किए गए कई शोधों में से एक शोध कहता है कि दिल्ली के इलाके में गरमियों में इसकी गहराई भी महज एक मीटर और चौड़ाई महज 80 मीटर रह जाती है. तो बरसात के समय जिस धारा के विजुअल दिखाकर आपको बाढ़ की धमकी दी जाती है, गरमी में यमुना उसका महज 16 फीसद ही रह जाती है.
यमुना को दिल्ली ने मौत दी है और उसमें भी सबसे अधिक चुनौती सरकारी एजेंसियों से मिली है. 100 एकड़ पर शास्त्री पार्क मेट्रो, 100 एकड़ में यमुना खादर आइटीओ मेट्रो, 100 एकड़ में खेलगांव और उससे जुड़े दूसरे निर्माण, 61 एकड़ में इन्द्रप्रस्थ बस डिपो और 100 एकड़ में बनाया अक्षरधाम. नगर निगम के नालों ने यमुना का आंचल रोजाना मैला करने का ठेका लिया हुआ है सो अलग.
महरौली, वसन्त विहार से लेकर द्वारका तक की हरियाणा से सटी पट्टी साल भर त्राहि-त्राहि करती है.
यही वह हिस्सा है, जिसने 1947 से 2010 के बीच नौ बाढ़ देखे हैं. 1947, 1964, 1977, 1978, 1988, 1995, 1998, 2008 और 2010. यमुना के पेटे में धड़ाधड़ निर्माण किए जा रहे हैं. यह भूलकर कि यमुना भ्रंश रेखा में बहती है और कभी भी भूकंप के तगड़े झटके लगे तो यह सब ठाठ धरा रह जाएगा.
केन्द्रीय जल आयोग का प्रस्ताव कहता है कि यमुना धारा के मध्य बिन्दु और एकतरफ के पुश्ते के बीच की दूरी कम-से-कम पांच किमी रहनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि मेट्रो, खेलगांव, अक्षरधाम जैसे सारे निर्माण सुरक्षा से समझौता कर बनाए गए हैं.
पर्यावरण संरक्षण कानून- 1986 की मंशा के मुताबिक, नदियों को ‘रिवर रेगुलेशन जोन’ के रूप में अधिसूचित कर सुरक्षित किया जाना चाहिए था. 2001-2002 में की गई पहल के बावजूद, पर्यावरण मंत्रालय आज तक ऐसा करने में अक्षम साबित हुआ है. बाढ़ क्षेत्र को ‘ग्राउंड वाटर सेंचुरी’ घोषित करने के केन्द्रीय भूजल आयोग के प्रस्ताव को हम कहां लागू कर सके?
बहरहाल, अच्छी बात यही है कि अब यमुना की बदतर हालत पर बड़ी अदालत की निगाह गई है. दिलचस्प होगा कि हरियाणा सरकार मंगलवार को जवाब में क्या कहती है.