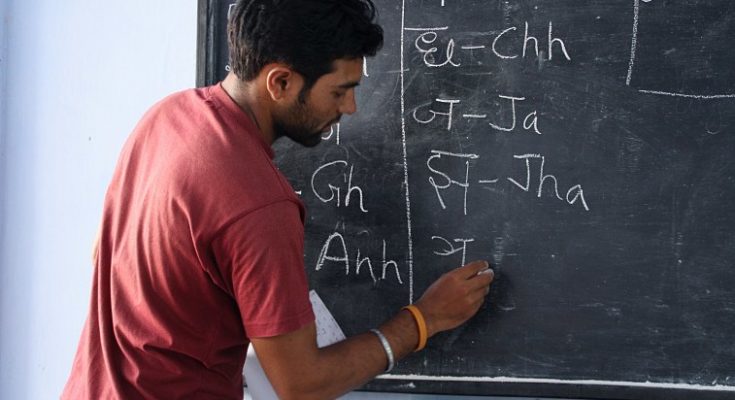आचार्यों के चेहरे मुरझाये हुए हैं। ये क्या कर डाला नासपीटो। इसी दिन के लिए तुम्हें रट्टा मारना सिखाया था? इसी दिन के लिए तुम्हें घुट्टी पिलायी थी – क के कबूतर, ख खरबूज, ग से गोबर? हुआ यूं है कि उत्तर प्रदेश में कबूतरों ने खरबूज खाकर गोबर कर दिया है। अब ये मत पूछिएगा कि कबूतर गोबर कैसे करेगा? व्यवस्था पर उठे प्रश्नों से नकारात्मकता पैदा होती है। नकारात्मकता से देश में निराशा फैलती है। निराशा देश का नुकसान करती है। देश का नुकसान मतलब सीधे-सीधे राष्ट्रद्रोह। तो समझ जाइए मामला कितना गंभीर है।
तो बात कुछ यूं है कि उ प्र में हि शि का थैंक्यू हो गया है। मतलब उत्तर प्रदेश में हिंदी शिक्षा का थैंक्यू हो गया है। चीनी ऐप का बहिष्कार होना था और बच्चों ने हिंदी का बहिष्कार पहले किया। अब हिंदी से ज्यादा देसी चीज़ क्या होगी? हिंदी भाषा नहीं है, राष्ट्रवाद है। सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर एक उक्ति अक्सर आपको मिल जाएगी कि हिंदी राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है। यूपी के बच्चों ने कह दिया- हमसे ना हो पाएगा! अब या तो हिंदी बचा लो नहीं तो हिंदू बचा लो। आचार्यों ने सोचा हिंदू वैसे ही खतरे में है और रिस्क ठीक नहीं तो कह दिया ठीक है हिंदी की रक्षा बाद में कर लेंगे। छात्रों ने कहा- जी, गुरुजी! सादर चरण स्पर्श…
यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजों का एलान किया है। कोरोना के हिसाब से रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 10वीं में 83 फीसद और 12वीं में 76 फीसद, लेकिन हिंदी का हिसाब प्रचंड गड़बड़ाया हुआ है। आठ लाख से अधिक छात्र हिंदी की वैतरणी पार नहीं कर पाये। वैसे सरकार के हिसाब से देखें तो इसे हिंदी का अभूतपूर्व विकास भी कह सकते हैं। वह ऐसे, कि 2019 में 10वीं-12वीं में हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 10 लाख थी। तो हिंदी का सीधे 20 फीसद विकास हुआ है। और अगर कहीं 2018 वाला देख लें तब तो लगेगा भारतेंदु युग यही है। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। उस साल 11 लाख बच्चे बोर्ड की हिंदी परीक्षा में फेल हुए थे। मतलब 30 फीसद का सीधा लाभ हिंदी को मिला है।
इस पर तो आचार्यों को खुश हो जाना चाहिए था। खुश थे। लेकिन जब रिजल्ट पर ठीक से गौर किया तो उनकी जुबान से निकला ‘ओह गॉड’। कुछ लोगों को गॉड सुनने में सेकुलर लगता है और भगवान जरा कम्युनल। श्री राम तो खैर जाने ही दीजिए। बहरहाल, उ प्र के आचार्यों की हि शि को लेकर हालत इसलिए खराब है कि अंग्रेजी माथे पर बैठती जा रही है। हाई स्कूल में हिंदी में 5 लाख 27 हजार बच्चे फेल हुए हैं तो अंग्रेजी में 5 लाख 19 हजार। पिछले साल भी यही हाल था। हिंदी में 5 लाख 74 हजार फेल हुए थे तो अंग्रेजी में केवल 5 लाख 2 हजार।

हिंदी का मसला इतना भी हल्का नहीं है। 2 लाख 39 हजार छात्रों ने तो हिंदी की परीक्षा दी ही नहीं। सानू की? हिंदी में कौन सी नौकरी मिल जानी है? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी को छात्र एक अगंभीर विषय के तौर पर देख रहे हैं। मतलब इसे पढ़ना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। हाय हिंदी हाय हिंदी। हिंदी बर्बाद हो तो हो लेकिन अंग्रेजी तू कैसे आबाद हुई? जब हिंदी में 12वीं ही पास नहीं करेंगे बच्चे तो बीए की सीटें कैसे भरेंगी? एमए कौन करेगा? और जब दाखिले ही नहीं होंगे तो देवतुल्य आचार्यों को कौन पूछेगा? दरअसल 10वीं-12वीं की परीक्षा में हिंदी की दुर्दशा से असल संकट है विश्वविद्यालयों में चेला और झोला संस्कृति के मिटने का अंदेशा। सोचिए, गुरुजी के चरणों में बैठे चेलों और गुरुजी के कंधों पर लटके झोलों को हिंदी विभागों से हटा दीजिए तो बचेगा क्या?
दरअसल, हिंदी की इस हालत के लिए 10वीं 12वीं के छात्र जिम्मेदार नहीं हैं। इस भाषा के लिए आचार्य जिम्मेदार हैं। बरसों बरसों में उन्होंने इस विभाग के कमरों को बौद्धिक यतीमखाने में बदलकर छोड़ दिया है। आलोचना के आचार्य प्रवरों ने एक बहुत संभावनाशील भाषा को जुगाड़ और जोड़-तोड़ से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। यह कहना बहुत जोखिम भरा है लेकिन यह बात कहनी तो पड़ेगी कि हिंदी कभी भी विज्ञान, विचार और विवेक की एक विराट भाषा के तौर पर नहीं जानी गयी। एक भाषा के तौर पर इसका आकर्षण आजादी के बाद से ही धूमिल पड़ रहा था। हिंदी के सामने खड़े हुए क्षेत्रीय भाषा आंदोलनों को देखिए। खासकर तमिल, मलयाली और बांग्ला। इन भाषाओं के लेखकों ने जनपक्षधरता की राह चुनी। ये भाषाएं दलितों-पिछड़ों-औरतों के पक्ष में विमर्श की आवाज बनीं। आप सोचिए तो संत कवि तिरुवल्लुवर के सामने हिंदी पट्टी में आप किसको याद करना चाहेंगे? नामदेव ढसाल, सिद्धालिंगैया या आज की तारीख में सूरज येंगड़े या आनंद तेलतुंबड़े के सामने हिंदी पट्टी का जवाब क्या है? आखिर वो वजहें क्या हैं कि हिंदी में न बाबा साहेब आंबेडकर होते हैं, न सावित्री बाई फुले, न पेरियार न कोई अपना बुल्लेशाह, बाबा फरीद?
सच यह है कि हिंदी के आचार्यों ने हिंदी के संघर्षशील लेखकों, विचारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उनके संघर्षों की हमेशा तौहीन की है उन्हें नीचा दिखाया है। एक भाषा के तौर पर हिंदी सामाजिक न्याय और संघर्ष का जरिया कभी नहीं बन पायी। इसकी जड़ें जातिवाद में हैं क्योंकि जिन आचार्यों ने हिंदी को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था वो अपने-अपने तरीके से उसी जातिवाद के लाभार्थी थे। बाद में उन्होंने अपने चेलों को ये गुर सिखाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी से होते हुए नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नागेंद्र, सुधीश पचौरी तक। इनके मठों में सामाजिक वैचारिकी की कोई जगह नहीं थी। इन्होंने दलित, पिछड़े, स्त्री और आदिवासी लेखकों के खिलाफ एक संगठित अभियान चलाकर उन्हें खत्म करने की कोशिश की। वो उस दिन भी जानते थे कि यह हिंदी को कमजोर करने की शर्त पर ही संभव है, लेकिन मठों की सत्ता में शर्तों की नैतिकताएं केवल मठाधीश तय करता है।
सच यह है कि हिंदी के पास बौद्धिक आकर्षण का घोर अभाव है। मार्क्स और लेनिन छोड़ दीजिए। आप पाब्लो नेरुदा, मार्तिन फिएरो, नोआ हरारी या मार्खेज का पासंग भी हिंदी अगर नहीं हासिल कर सकी है तो इसकी पहली वजह है हिंदी को आचार्यों ने संघर्ष, न्याय और सरोकार की भाषा बनने ही नहीं दिया। तो आज क्यों रो रहे हैं आचार्य?
हिंदी का बेड़ा गर्क 10वीं, 12वीं के छोकरों ने नहीं किया है, आपके सामंती लौंडपन ने किया है। लेकिन मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है.. यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। आचार्य! आप जीते, हिंदी हारी। आपके चेलों और झोलों पर यह कुर्बानी कबूल है, कबूल है, कबूल है।