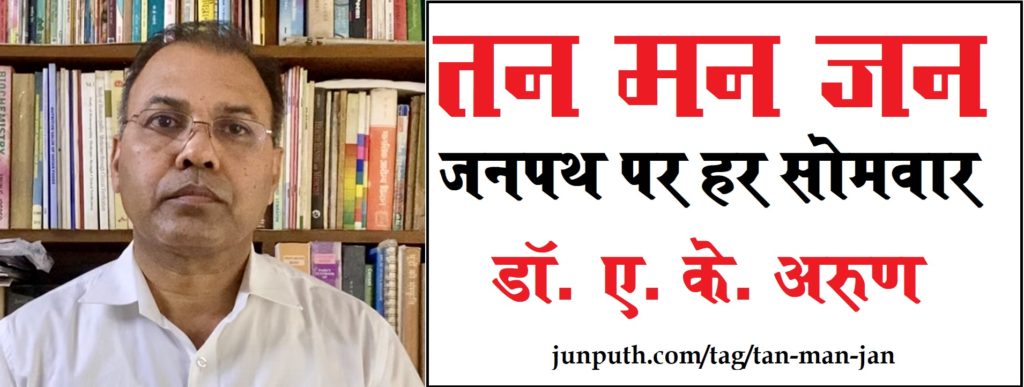जब देश की जनता प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ताली और थाली बजा रही थी तभी कोरोना वायरस देश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। उनके अगले राष्ट्रीय प्रसारण तक इस वायरस का कहर रंग दिखाने लगा था। लाशों से श्मशान पटने लगे थे। उसी समय एक जाने-माने ब्रिटिश अर्थशास्त्री टैरेन्स जेम्स ओ’ नील की भारत और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर की गयी टिप्पणी की कड़ी आलोचना भी हो रही थी।
जेम्स ओ’ नील एक चर्चित अर्थशास्त्री हैं। कोई दो दशक पहले आपने सन् 2002 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को ‘‘ब्रिक्स’’ के रूप में पहचाना था। नील ने ही सन् 2013 में नरेन्द्र मोदी को बेहद सम्भावनाओं से भरा नेता बताया था। जेम्स ओ’ नील ने टिप्पणी की थी कि, ‘‘खैर मनाइए कि कोरोना वायरस संक्रमण चीन में शुरू हुआ, भारत जैसे किसी देश में नहीं। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि यह कोरोना वायरस से प्रभावी तरीके से निबट ही नहीं सकती थी। चीन ने जिस प्रकार चैतरफा मुस्तैदी से वायरस पर नियंत्रण पाया वह भारत में सम्भव नहीं था।’’ उन्होंने चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि चीन ने अन्ततः स्थिति संभाल ली।
कोरोना वायरस संक्रमण ने एक तरह से देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मार्च के आरम्भ तक तो सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की भयावहता को ही नकार रही थी जबकि वायरस का देश में ताण्डव शुरू हो चुका था। इस वायरस ने तो जनवरी में ही दस्तक दे दी थी। उस समय चीन, इटली, स्पेन, ब्रिटेन तथा इरान आदि देशों में बड़ी संख्या में लोग वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर मारे जा चुके थे। इन सभी देशों के भयावह परिदृश्य से आतंकित दुनिया में इस जानलेवा वायरस से निबटने के निवारक और नियंत्रक उपाय तथा शोध शुरू हो चुके थे, तब हमारी सरकार अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अगवानी की तैयारी में ढोल-नगाड़ों के साथ व्यस्त थी। ट्रम्प की भारत यात्रा और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने-बनाने के उपक्रम के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जिस तरह तेजी आयी और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में जो भी कहा, उससे ही स्पष्ट हो गया था कि भारत की स्वास्थ्य सेवा और व्यवस्था पर जेम्स ओ’ नील की टिप्पणी वास्तव में एक कड़वी हकीकत है।

जब हम भारत के लोगों के स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो एक अलग ही दृश्य सामने आता है। देश में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि कुछ अपवादों को छोड़कर देश के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों की हालत दयनीय है। संक्रामक रोगों से ग्रस्त मरीज भी अस्पताल के बाहर खुले और गन्दे में रहने को मजबूर हैं। अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है तो गम्भीर रोगियों को भी मेडिकल जांच के लिए महीनों/बरसों तक प्रतीक्षा सूची में इन्तजार करना पड़ता है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसे क्या बदलाव आ गये हैं जो लोगों के जान की मुसीबत बन गये हैं?
बदली जीवनशैली में आराम और अनावश्यक खानपान, फास्ट फूड, साफ्ट/हार्ड ड्रिंक्स आदि ने इतनी पैठ बना ली है कि अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। लोगों ने आरामपरस्त जिन्दगी के नाम पर शारीरिक श्रम और समुचित विश्राम करना बन्द कर दिया है, मसलन उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तनाव, अवसाद, यहां तक कि कैंसर जैसे रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। डब्लूएचओ की उच्च रक्तचाप व अन्य जीवनशैली के रोगों के बढ़ते मामले को लेकर व्यक्त चिन्ता जायज है लेकिन भारत व अन्य विकासशील देशों में यह चिन्ता करना इसलिए भी बेहद जरूरी है कि कथित विकास के नाम पर बन रहे मेगा प्रोजेक्ट, बड़े बांध, रियल स्टेट, सुपर हाइवे आदि पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और यहां के नागरिकों को भीषण आर्थिक संकट में फंसना पड़ रहा है।
आइए, सत्तर साल पहले की स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर डालें। सन् 1943 में अंग्रेजों ने भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति (भोर समिति) का गठन किया था। भोर समिति ने सन् 1945 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और स्वास्थ्य सेवा के विकास के लिए एक श्रेणीबद्ध प्रणाली के गठन का सुझाव दिया। इस सुझाव के अनुसार प्रत्येक 20,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की बात थी। समिति ने स्पष्ट कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकांश लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिलना चाहिए।
विडम्बना देखिए कि आजादी के बाद सन् 1950 में जो भारतीय स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर उभरी उसमें 81 प्रतिशत सुविधाएं शहरों में स्थापित की गयीं। आज भी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। सन् 1960 के अन्त तक जब देश में बढ़ती विषमता की वजह से जन आन्दोलन उभरने लगे तब सरकार को मानना पड़ा कि सरकारी सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंच रही हैं। स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने भी माना कि डाक्टरों से गांव में जाकर सेवा देने की उम्मीद लगभग नामुकिन है। फिर सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा को विकसित करने का मन बनाया। इसी नजरिये से डॉ. जे.बी. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक और समिति बनी। इस समिति ने सुझाव दिया कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार किये जाएं। इसके लिए भारत ने विदेशी बैंकों से कर्ज लेना शुरू किया।
धीरे-धीरे भारत अन्र्तराष्ट्रीय बैंकों के कर्ज जाल में फंसता चला गया। 1991 से तो भारत सरकार ने खुले रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की आर्थिक नीतियों को ही लागू करना आरम्भ कर दिया। इसका देश के आम लोगों के जीवन पर गहरा असर भी दिखा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी खर्च में कटौती तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के परिणामस्वरूप बीमारी से जूझते आम लोगों की तादाद बढ़ने लगी। दवा कम्पनियों ने भी दवाओं पर कीमतों का नियंत्रण समाप्त करने का दबाव बनाया और दवाएं महंगी होने लगी। दवाओं के महंगा होने का सबसे दुखद पहलू था जीवनरक्षक दवाओं का बेहद महंगा हो जाना।
इस बीच जीवनरक्षक दवाएं बनाने वाली देशी कम्पनियां धीरे-धीरे दम तोड़ने लगीं। नई नीतियों की आड़ में गैट (जेनरल एग्रीमेंट आफ ट्रेड एन्ड टैरिफ) के पेटेन्ट प्रावधानों का दखल शुरू हो गया और नतीजा हुआ कि देश के पेटेन्ट कानून 1971 को बदल दिया गया। दवाइयां बेहद महंगी हो गईं। उदाहरण के लिए, टी.बी. की दवा आइसोनियाजिड, कुष्ठ रोग की दवा डेप्सोन और क्लोफजमीन, मलेरिया की दवा सल्फाडौक्सीन और पाइरीमेतमीन इतनी महंगी हो गयी कि लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे। स्वास्थ्य पर बाजार का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा था।
सन् 1993 में विश्व बैंक ने एक निर्देशिका प्रकाशित की। शीर्षक या- ‘‘इन्वेस्टिंग इन हेल्थ।’’ इसमें साफ निर्देश था कि कर्जदार देश फंड-बैंक के इशारे पर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मामलों में बजट कटौती करें। धीरे-धीरे स्वास्थ्य का क्षेत्र मुनाफे की दुकान में तबदील हो चुका है। गम्भीरता से विचार करें तो ‘आयुष्मान भारत’ या ‘स्वास्थ्य बीमा योजना’ या ‘मोदी हेल्थ केयर’ की पृष्ठभूमि में यह कहानी आपको सहज दिख जाएगी।
WDR-1993-Englishअब रोगों की वर्तमान स्थिति पर थोड़ी चर्चा कर लें। भारत में कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, श्वास की बीमारियाँ, तनाव, अनिद्रा, चर्मरोग व मौसमी महामारियों में बेइन्तहा वृद्धि हुई है। बढ़ते रोगों के दौर में जहां मुकम्मल इलाज की जरूरत थी वहां दवाओं को महंगा कर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को निजी कम्पनियों के हाथों में सौंप दिया गया। सन् 2000 के आसपास निजी अस्पतालों की बाढ़ सी आ गयी। कारपोरेट अस्पतालों की संख्या बढ़ी और धीरे-धीरे आम मध्यम वर्ग अपने उपचार के लिए निजी व कारपोरेट अस्पतालों की ओर रुख करने लगा। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था एक तो मजबूत भी नहीं हो पायी थी, ऊपर से ध्वस्त होने लगी और दूसरी ओर बड़े सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज एवं निदान के लिए एक-दो वर्ष की वेटिंग मिलने लगी। भीड़ का आलम यह कि अस्पतालों में अफरा-तफरी और अव्यवस्था का आलम आम हो गया। निजीकरण की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों में भी इलाज महंगा कर दिया गया। लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा के बजाय निजी अस्पतालों का रुख करने लगे। महंगे इलाज की वजह से ‘‘स्वास्थ्य बीमा’’ लोगों के लिए तत्काल जरूरी लगने लगा और देखते-देखते कई बड़े कारपोरेट कम्पनियों स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कूद पड़ीं और स्वास्थ्य बीमा का क्षेत्र मुनाफे का एक बड़ा अखाड़ा सिद्ध हो गया।
कहने को निजीकरण व वैश्वीकरण के लिए कांग्रेस की सरकारें जिम्मेवार हैं लेकिन बाद में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकारों ने तो और भी जोर-शोर से निजीकरण एवं बाजारीकरण को बढ़ाया। कहने को भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वदेशी जागरण मंच के नाम पर स्वदेशी के नारे तो लगाये लेकिन बाजारीकरण एवं निजीकरण को बेशर्मी से आगे बढ़ाया। नतीजा- स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र निजी मुनाफे के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के रूप में बढ़ने लगा। अब जब बीमारियों का इलाज है, दवाएं महंगी हैं और और आम लोग इतनी महंगी दवाएं और इलाज नहीं ले सकते तो उन्हें स्वास्थ्य बीमा की मीठी चटनी के बहाने तसल्ली दी जा रही है।
भारत में स्वास्थ्य की स्थिति पर नज़र डालें तो सूरत-ए-हाल और चिन्ताजनक है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी खस्ता है। अन्य देशों की तुलना में भारत में कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 4 प्रतिशत ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है जबकि चीन 8.3 प्रतिशत, रूस 7.5 प्रतिशत तथा अमेरिका 17.5 प्रतिशत खर्च करता है। विदेशों में हेल्थ की बात करें तो फ्रांस में सरकार और निजी सेक्टर मिलकर फंड देते हैं जबकि जापान में हेल्थकेयर के लिए कम्पनियों और सरकार के बीच समझौता है। आस्ट्रिया में नागरिकों को फ्री स्वास्थ्य सेवा के लिये ”ई-कार्ड“ मिला हुआ है। हमारे देश में फिलहाल स्वास्थ्य बीमा की स्थिति बेहद निराशाजनक है। अभी यहां महज 28.80 करोड लोगों ने ही स्वास्थ्य बीमा करा रखा है। इनमें 18.1 प्रतिशत शहरी और 14.1 प्रतिशत ग्रामीण लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इसमें शक नहीं है कि देश में महज इलाज की वजह से गरीब होते लोगों की एक बड़ी संख्या है। अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के एक शोध में यह बात सामने आयी है कि हर साल देश में कोई 8 करोड लोग महज इलाज की वजह से गरीब हो जाते हैं। यहां की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था ऐसी है कि लगभग 40 प्रतिशत मरीजों को इलाज की वजह से खेत-घर आदि बेचने या गिरवी रखने पड़ जाते है। एम्स का यही अध्ययन बताता है कि बीमारी की वजह से 53.3 प्रतिशत नौकरी वाले लोगों में से आधे से ज्यादा को नौकरी छोड़नी पड़ जाती है।
भारत में स्वास्थ्य पर कुल व्यय अनुमानतः जीडीपी का 5.2 फीसदी है जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय पर निवेश केवल 0.9 फीसदी है, जो गरीबों और जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से काफी दूर है जिनकी संख्या कुल आबादी का करीब तीन-चौथाई है। पंचवर्षीय योजनाओं ने निरंतर स्वास्थ्य को कम आवंटन किया है (कुल बजट के अनुपात के संदर्भ में)। सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा परिवार कल्याण पर खर्च होता है। भारत की 75 फीसदी आबादी गांवों में रहती है फिर भी कुल स्वास्थ्य बजट का केवल 10 फीसदी इस क्षेत्र को आवंटित है। उस पर भी ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की मूल दिशा परिवार नियोजन और शिशु जीविका व सुरक्षित मातृत्व (सीएसएसएम) जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की ओर मोड़ दी गयी है जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा कागज़ी लक्ष्यों के रूप में देखा जाता है।

एक अध्ययन के अनुसार पीएचसी का 85 फीसदी बजट कर्मचारियों के वेतन में खर्च हो जाता है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में प्रतिबद्धता का अभाव स्वास्थ्य अधिरचना की अपर्याप्तता और वित्तीय नियोजन की कम दर में परिलक्षित होता है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जनता की विभिन्न मांगों के प्रति गिरते हुए सहयोग में यह दिखता है। यह प्रक्रिया खासकर अस्सी के दशक से बाद शुरू हुई जब उदारीकरण और वैश्विक बाजारों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खोले जाने का आरंभ हुआ। चिकित्सा सेवा और संचारी रोगों का नियंत्रण जनता की प्राथमिक मांगों और मौजूदा सामाजिक-आर्थिक हालात दोनों के ही मद्देनजर चिंता का अहम विषय है। कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के साथ इन दोनों उपक्षेत्रों में भी आवंटन लगातार घटता हुआ दिखा। चिकित्सीय शोध के क्षेत्र में भी ऐसा ही रुझान दिखता है। कुल शोध अनुदानों का 20 फीसदी कैंसर पर अध्ययनों को दिया जाता है जो कि 1 फीसदी से भी कम मौतों के लिए जिम्मेदार है जबकि 20 फीसदी मौतों के लिए जिम्मेदार श्वास संबंधी रोगों पर शोध के लिए एक फीसदी से भी कम राशि आवंटित की जाती है।
हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ-साथ सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य चिंतन का भी अभाव लगता है। जब देश की जनता का काम लच्छेदार भाषणों और हसीन सपनों से ही चल जाता है तो बाकी के हकीकत की क्या जरूरत? आज के नेता यह बखूबी समझते हैं। अपने क्रमशः दिये राष्ट्रीय भाषणों में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि महामारी का खतरा बढ़ने वाला है मगर उससे बचाव की जिम्मेवारी जनता खुद वहन करे। ऐसे ही इस महामारी की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई का भी कोई रोडमैप उनके पास नहीं था। इस दौरान देश में अन्तरराष्ट्रीय आवाजाही भी बिना किसी खास एहतियात के जारी रही। एयरपोर्ट पर कहने को तो चाक-चौबन्द इन्तजाम था लेकिन हकीकत सिर्फ हवा में थी। जाहिर है कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्था खुद इतनी बीमार है कि उसससे महामारी नियंत्रण, मुकम्मल उपचार जैसी उम्मीदें करना बेकार है। प्रदूषण, गन्दगी, साफ पानी की पर्याप्त अनुपलब्धता, स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना और जागरूकता का अभाव किसी भी महामारी या रोग के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण रखते हैं।
पिछले 70 साल का रोना रोकर मौजूदा सरकार ने बीते 7 साल में स्वास्थ्य के सरकारी ढांचे को मजबूत करना तो दूर खण्डहर में तब्दील होने के लिए छोड़ दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की जो नींव यूपीए सरकार ने डाली थी उस पर एनडीए सरकार ने बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी है। पांच सितारा अस्पताल देश में कथित बेहतर इलाज के पहले माध्यम बन गये हैं। सरकारी या निजी क्षेत्र के अतिविशिष्ट या सामान्य सम्पन्न तबके के लोगों के इलाज के लिए निजी व कारपोरेट अस्पताल ही अब पहली पसन्द हैं। जाहिर है आम आदमी धन के अभाव में इन्हीं बीमार सरकारी अस्पतालों में इलाज करा कर मरने को अभिशप्त है। क्या देश की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई दवा कभी तैयार हो पाएगी?