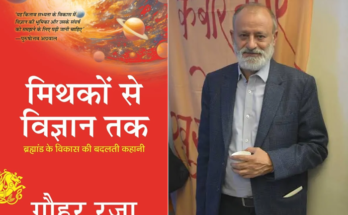“अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो, तो देश के संग गद्दारी कर ही नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है एयरफोर्स को ‘भारत माता की जय’ चिल्लाने वाले चाहिए? उन्हें बेटा, वैसे कैडेट्स चाहिए जिनका कोई लक्ष्य हो। जिनमें जोश हो। जो मेहनत और ईमानदारी से अपनी ट्रेनिंग पूरी करें। क्योंकि वही कैडेट्स आगे चलकर बेहतर ऑफिसर बनते हैं और देश को अपना बेस्ट देते हैं। तुम सिनसिएरिटी से, हार्ड वर्क से, ईमानदारी से एक बेहतर पायलट बन जाओ, देशभक्ति अपने आप हो जाएगी।”
ये एक डायलॉग है नेटफ्लिक्स पर हाल में रिलीज़ हुई फिल्म “गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल” का। यहां पंकज त्रिपाठी एक पिता के रूप में बेटी को उसके सवाल का जवाब दे रहे हैं।
सिनेमा की छवि हमारे समाज में कभी भी अच्छी नहीं रही। यहां जब मैं ‘हमारे’ कह रहा हूं, तो मेरा मतलब उत्तर भारत और खासकर हिंदी पट्टी से है। मैंने दुनिया तो क्या पूरा देश भी नहीं देखा है, लेकिन जितना देखा है उसके बारे में दावे के साथ कह सकता हूं कि किशोरावस्था में सिनेमा के प्रति बढ़ती रुचि को हमेशा आवारागर्दी और बिगड़ने की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम ही माना गया है। क्या घर और क्या स्कूल, हर जगह सबको एक ही लाठी से हांकने की परिपाटी रही है।
किशोरावस्था की कच्ची उम्र में किताबें लुभाती कम, डराती ज्यादा हैं, लेकिन इसी उम्र में किस्से और कहानियां कानों से होते हुए दिमाग में घुसती हैं, वहां घंटी बजाती हैं और फिर रूह तक उतर जाती हैं। कभी-कभी तो इतने गहरे कि रात में खटिया पर लेटे नहीं कि कहानी का कोई किरदार आकर धीरे से आवाज़ देने लगता है। फिर हाथ पकड़ कर अपने साथ ले कर चल देता है। जब नींद उचटती है तो समझ में आता है कि ये तो सपना था।
क्या होता अगर फिल्में बचपन से ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा होतीं? यहां फिल्मों का मतलब अच्छे सिनेमा से है। पंद्रह साल की उम्र में “तारे ज़मीं पर” देखी थी, अच्छी लगी। आठ साल बाद दोबारा देखी, इस बार अद्भुत लगी। फिर ख़याल आया कि ये हमारे स्कूलों में क्यों नहीं दिखायी जा सकती? जब खोखो, कबड्डी और पीटी के लिए एक अलग घंटा (पीरियड) हो सकता है, जब हर शनिवार इंटरवल के बाद गीत गवनई हो सकती है, तो कम से कम महीने में एक बार अच्छा सिनेमा क्यों नहीं दिखाया जा सकता?
“तारे ज़मीं पर” जैसी फिल्म तो बच्चों से ज्यादा शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। यह फिल्म हमारे प्राइमरी लेवल के मास्साब लोगों को ये बात समझने में मदद कर सकती है कि बच्चों, खासकर विशेष बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाए।
2016 में “पिंक” नाम की एक फिल्म आयी थी। ये तीन लड़कियों की कहानी थी जो एक महानगर में परिवार से दूर अकेले रहती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो अनमैरिड हैं लेकिन सेक्शुअली एक्टिव हैं। इनके मेल फ्रेंड्स भी हैं। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। यहां से पुलिस और समाज की वो सोच उघड़ कर सामने आती है जो ये मानती है कि लड़की ने अगर छोटे कपड़े पहन रखे हैं, शराब पीती है और पार्टियों में जाती है तो उसका मोलेस्टेशन और रेप भी जस्टिफाइड है।

फिल्म में लड़कियों की तरफ से केस लड़ रहे वकील का किरदार निभा रहे अमिताभ बच्चन की ये दलीलें पढ़िए जो वो कोर्टरूम में कहते हैं।
1- किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि लड़के को ये इंडिकेट होता है कि अगर वो मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो मेरे साथ सोने में कतराएगी नहीं। शराब यहां पर एक खराब कैरेक्टर की निशानी माना जाता है, लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए नहीं, लड़कों पे ये अप्लाई नहीं होता, उनके लिए ये बस एक हेल्थ हैजर्ड है।
2- “No. No your honour. ‘न’ सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में पूरा वाक्य है। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, explanation या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। न का मतलब न ही होता है… my client said ‘no’, your honour, and these boys must realise, no का मतलब no होता है। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या अपनी बीवी ही क्यों न हो… no means no. And when someone says no, you stop.
ऐसी फिल्में क्यों स्कूलों में नहीं दिखायी जातीं? किशोरावस्था से जवानी की दहलीज पर खड़े लड़के शायद समय रहते बेहतर तरीके सीख पाएं या बेहतर तरीके से सोच पाएं।
इसी साल 2020 में अनुभव सिन्हा निर्देशित फिल्म “थप्पड़” रिलीज़ हुई। परिवार अगर साथ बैठकर ये फिल्म देखें तो शायद उसे अहसास हो कि जिस व्यवस्था पर हम फूले नहीं समाते उसकी बुनियाद कितनी सड़ चुकी है।
“गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल” इसी कड़ी की एक फिल्म है जो यह महसूस कराती है कि पारंपरिक भारतीय परिवारों को कैसे पिताओं की ज़रूरत है।
अच्छे और सार्थक सिनेमा की ये लिस्ट बेहद लंबी हो सकती है और अभी तो इसमें क्षेत्रिय और वैश्विक सिनेमा का जिक्र भी नहीं हुआ है। दरअसल मकसद अच्छी फिल्मों का नाम लेना नहीं बल्कि उससे मिलने वाले संदेश का जीवन पर पड़ने वाले असर की चर्चा करना था।
हम तो यही चाहेंगे कि अगर किसी दिन ये दुनिया खत्म होने वाली हो और धरती से कोई अंतिम अंतरिक्षयान किसी दूसरे ग्रह पर सुरक्षित ठिकाने की ओर निकलने ही वाला हो, तब उसमें मुझे भले ही जगह न मिले लेकिन कुछ अच्छी फिल्मों की सीडी जरूर रख ली जाएं।
शिवेंद्र राय दिल्ली स्थित पत्रकार हैं