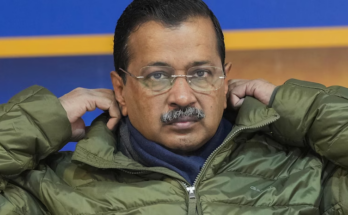फेसबुक पर किसी मित्र ने जब तले हुए मांगुर की तस्वीर साझा की, तब लगा कि पंचतत्व की शुरुआत मछली से ही होनी चाहिए. वैसे भी मिथिला का हूं तो मछली से अलग प्यार है ही. टीवी पर विष्णु पुराण भी आ रहा है इन दिनों, तो हमारे एक अवतार मत्स्यावतार भी रहे हैं.
पर, जरूरी नहीं कि हर मछली से प्रेम किया जाए.
कम से कम आप महानगरीय भारत में रहते हैं तो मांगुर से प्रेम तो कतई न जताइए क्योंकि मांगुर के दीवानों की प्लेट में जिस मछली को मांगुर कहकर परोसा जा रहा है, वह असल में मांगुर है ही नहीं. वह है अफ्रीकन कैट फिश. कई जगहों पर इसे थाई मांगुर भी कहते हैं. देखने में यह मांगुर जैसी ही लगती है, पर मछली से मुहब्बत करने वालों, बड़े धोखे है इस राह में…
वैज्ञानिकों की निगाह में यह कैटफिश असल में इनवेसिव स्पीशीज़ यानी हमलावर नस्ल की है. इसे खाने वालों को कैंसर होने का खतरा होता है. सिर्फ यही नहीं, यह देसी मछलियों के लिए पूरी तरह शाकालनुमा ही है. वैसे, इसको पालना, बेचना भारत में प्रतिबंधित है. यह कैटफिश उर्फ मांगुर भयंकर मांसखोर होती है. एकदम मगरमच्छ ही समझिए. अपने तालाब में मौजूद तमाम दूसरी मछलियों और जलीय जीवों को चट कर जाती है. तीसरी बात कि इसको पालने के लिए मछुआरे बूचड़खाने से लाकर सड़ा हुआ मांस (ताजा और महंगा मांस क्यों खिलाएगा भला!) इसको खिलाते हैं. इससे तालाब के पारितंत्र की क्या हालत होती होगी इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं.

अफ्रीकन कैटफिश आकार में देसी मांगुर के मुकाबले काफी बड़ी और सख्तजान होती है. अफ्रीकन कैटफिश को पालना भारत में प्रतिबंधित है, फिर भी कमाई के लिए यह पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार तक में खूब पाली जा रही है. असल में, फिश फिंगर बनाने के लिए इस नकली मांगुर से बढ़िया दूसरी मछली नहीं होती क्योंकि इसमें कांटे कम होते हैं. और अपन हिंदुस्तानी तो ऐसे हैं कि जहां से दो पैसे आते हों, नियम तोड़ने में जरा भी कोताही नहीं बरतते.
एडवांसेज फिश रिसर्च नाम की एक रिपोर्ट 2013 में प्रकाशित हुई थी और यह रिपोर्ट कहती है, ”भारत में मछलियों की 2,200 से अधिक नस्लें हैं, लेकिन इन नस्लों को हमलावर प्रजातियां धीरे-धीरे खत्म कर रही हैं.”
दुनिया भर में मछलियों की 8 सबसे हमलावर प्रजातियों में से पांच भारत में मौजूद हैं. मसलन, मॉस्क्यूटो फिश, ब्राउन ट्राउट और रेनबो ट्राउट, ये तीनों शिकारी प्रजातियां हैं और स्थानीय नस्लों की मछलियों के अंडे खा जाती हैं. इसी तरह नब्बे के दशक की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर बांध में डाली गई सिल्वर कार्प की वजह से गोल्डन महाशीर मछली सिर्फ 8 फीसद तक ही बची है. अलसबत्ता, सतलुज नदी पर बने करीब 10,000 हेक्टेयर के इस बांध में सिल्वर कार्प की तादाद 65 फीसद हो गई है.
सिर्फ हमलावर मछलियां ही नहीं, इनवेसिव जीवों (इनमें सुंदर दिखने वाले खतरनाक पौधे भी हैं) को दुनिया भर में जैव-विविधता और धरती की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा माना जा रहा है. संकर नस्लों (जिनमें सभी हमलावर नस्लें नहीं हैं) की वजह से अपने देश में मछलियों की 305 नस्लों पर अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है.
भारत के जैव-विविधता पर नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान, 2019 के मुताबिक देश में मछलियों की 28 प्रजातियां ‘गंभीर रूप से विलुप्तीकरण के खतरे’ में हैं और 86 ‘विलुप्त होने की कगार’ पर हैं.
2016 के कानकून शिखर सम्मेलन के जैव-विविधता पर प्रस्ताव में हमलावर नस्लों से एकजुट होकर लड़ने की बात की गई है लेकिन भारत ने अभी तक जीवों या वनस्पति प्रजातियों के लिए कोई ठोस बुनियादी आंकड़ा तैयार नहीं किया है. बेसलाइन डाटा बन जाएगा तभी पता चल पाएगा कि किन प्रजातियों को कितनी मात्रा में खतरा पहुंचा है.
यही नहीं, इन हमलावर विदेशी वनस्पतियों और जीवों पर रोक के लिए कानून बेहद पुराने हैं और अब प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे. भारत में, कृषि मंत्रालय के तहत वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय है जो खर-पतवारों और खतरनाक नस्लों को आने से रोकने के लिए काम करता है पर इसकी नाकामी का सुबूत इसी से मिलता है कि इनकी कथित निगहबानी के बीच पिछले डेढ़ दशक में कम से कम पांच विदेशी खर-पतवार देश में घुसपैठ कर चुके हैं. इस बात की तस्दीक उत्तर प्रदेश जैव-विविधता बोर्ड के आंकड़े भी करते हैं कि 2006-07 के दौरान आयातित गेहूं के साथ भारत में घुसपैठ कर जाएंट रगवीड, स्पीनी बर ग्रास, हाउंड्स टंग, हॉर्स नेटल, यूरोपियन फील्ड पैंसी नाम के ये हमलावर खर-पतवार देश के दस राज्यों में फैल चुके हैं. इनसे नुकसान के बारे में विस्तृत अध्ययन बाकी है मगर वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये तबाही बरपा करेंगे.
असल में, हमलावर नस्लों के देश में आने को लेकर कानून तो कई सारे हैं, लेकिन उनको लागू करने वाली एजेंसियों की आपस में और कस्टम विभाग के साथ आपसी तालमेल की कमी है. मसलन, 1978 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसके तहत राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षित वनों की वनस्पतियों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. यानी, अगर कोई विदेशी हमलावर नस्ल का पौधा भी तेजी से बढ़ रहा हो, तो उसे उखाड़ा नहीं जा सकता. ऐसे में काम मुश्किल हो जाता है.
अनुमान है कि भारत में तकरीबन 18,000 वनस्पतियों, 30 स्तनधारियों, चार परिंदों, 300 मीठे पानी की मछलियों और 1100 ऑर्थोपॉड की नस्लें बाहरी हैं. इनमें से ज्यादातर स्थानीय जैव-विविधता को तेजी से खत्म करती हैं. इनसे देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ रहा है. उत्तर प्रदेश जैव-विविधता बोर्ड की 2009 की रिपोर्ट में अमेरिकी कांग्रेस ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी एसेसमेंट के 2001 के आकलन के हवाले से बताया गया है कि भारत में इनसे सालाना 91 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है. इसमें इन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों का खर्च शामिल नहीं है.
वैसे, भारत में हम लोग बहुत सारी चीजों से लड़ रहे हैं. बहुत सारी चीजों का अस्तित्व खतरे में हैं. बेचारी मछलियों की देसी नस्लें बचाने पर किसका ध्यान जाएगा? बेचारी तो बोल भी नहीं पाती हैं.