 |
| काशीनाथ सिंह |
काशीनाथ सिंह यानी अस्सी के काशी को 2011 का साहित्य अकादमी मिल गया, ये अपने आप में अगर बड़ी नहीं तो दिलचस्प बात ज़रूर है। अव्वल तो साहित्य की सरकारी परिभाषा या कहें ‘अकादमिक’ परिभाषा में काशीनाथ सिंह जैसे लोगों की पूछ और कद्र नहीं होती। दूसरे, नामवर जी ने भी कभी छोटे भाई को, या उनकी किसी कृति को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच उस तरह से अपना कंधा नहीं छुआया, जैसा वे अलका सरावगी या आज भी एकाध स्वनामधन्य नवोदित कवियों के लिए करते आ रहे हैं बतौर सेलिब्रिटी। बावजूद इसके अगर ‘रेहन पर रग्घू’ के लिए ही सही, काशी को साहित्य अकादमी दिया जा रहा है तो इसके पीछे अकादमी के प्रति कोई मुग़ालता नहीं पालना चाहिए। पिछले दिनों जिस तरह से अकादमी ने तमाम लोगों को मरने से ठीक पहले या देरी से कमपन्सेट किया है, 2011 का पुरस्कार उसी कवायद की एक कड़ी समझा जाना चाहिए। बहरहाल, अच्छा ही हुआ ‘काशी का अस्सी’ के लिए उन्हें अकादमी नहीं मिला, वरना जस्टिस काटजू की बात में वज़न जुड़ जाता कि ग़ालिब को नोबेल दिया जाए।
जिन्होंने ‘रेहन पर रग्घू’ नहीं पढ़ी है, उनके लिए नीचे उसकी समीक्षा प्रस्तुत है जो 2008 में तहलका हिंदी की वेबसाइट पर छपी थी। इससे एक तो उपन्यास के बारे में आपको अंदाज़ा लग जाएगा, दूसरे एक बात ये साफ होगी कि ‘रेहन पर रग्घू’ दरअसल काशीनाथ सिंह की टिपिकल संवेदना का विस्तार ही है, उससे कुछ भी अलग नहीं। अपने कंटेंट में अकादमी ने जाने-अनजाने दरअसल ‘काशी का अस्सी’ को ही पुरस्कार दे डाला है, बस भाषा का फ़र्क है।
रेहन पर रग्घू: ‘तन्नी गुरु’ से ‘मुड़ीकट्टा’ होने का सफ़र
किसी ने सच ही कहा है कि उम्र अपना असर दिखाती है। ऐसा लगता था कि काशीनाथ सिंह के लेखन पर उनकी बढ़ती अवस्था का फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा, लेकिन राजकमल से छप कर आया उनका उपन्यास ‘रेहन पर रग्घू‘ इस बात की ताक़ीद करता है कि वास्तव में अब ‘जम्बूद्वीप‘के काल चक्र से शाम को गायब कर दिया गया है, यहां के निवासियों के चेहरों से हंसी गायब हो चुकी हैऔर ‘तन्नी गुरु‘ का ‘मुड़ीकट्टा‘ होना कोई प्रतीकात्मक व्यंग्य नहीं, उनकी नियति में तब्दील हो चुका है। ‘काशी का अस्सी‘ के विभिन्न संस्मरणों से लेकर पिछली पुस्तक ‘घर का जोगी जोगड़ा‘ में अब तक जो कहानी शहर से शुरू होकर शहर पर खत्म होती थी, वह खत्म तो आज भी शहर पर ही होती है लेकिन उसकी शुरुआत उस गांव से होती है जहां से बरसों पहले लेखक का कुनबा उजड़ चुका है। यकीन मानें कि केंद्रीय पात्र रग्घू यानी रघुनाथ, खुद काशीनाथ से जरा भी अलग नहीं दिखता सिवाय इसके कि लैंडस्केप में जरा-मरा हेर-फेर और तब्दीली कर दी गई है।
एक साधारण स्कूल मास्टर रग्घू का निजी जीवन अपने परिवार से इतर कुछ भी नहीं है। दो बेटे,एक बेटी और एक पत्नी से मिल कर बनी इस पंचमेल खिचड़ी में शुरू से लेकर अंत तक रघुनाथ की नियति को ही केंद्र में रखा गया है। बड़ा बेटा एक कायस्थ लड़की से शादी कर अमेरिका चला जाता है तो छोटा बेटा एमबीए करने के नाम पर दिल्ली में एक तलाकशुदा महिला के साथ रहने लगता है। बचती है बेटी जो अब कॉलेज में लेक्चरार हो गई है, सो उसने शादी के लिए इंकार कर बाप की सारी कवायद पर पानी फेर दिया है। उसे प्रेम भी हुआ है तो एक ऐसे दलित अफसर से जिसके रिश्तेदार गांव में रग्घू के ही नहीं उसके पुरखों के भी करनिहार रहे हैं। इन तमाम पारिवारिक त्रासदियों के बीच रघुनाथ का अकेला साथी बचा है झब्बू पहलवान,लेकिन नागपंचमी की एक रात दलितों के टोले में उसकी भी हत्या हो जाती है। झब्बू का बाहुबली साया सिर पर से उठ जाने के बाद रग्घू की जमीन पट्टीदारों के झगड़े में फंस जाती है जिससे निजात पाने के लिए उन्हें शहर का रास्ता सूझता है। यह भी संयोग ही है कि अमेरिका से उनकी बहू बीएचयू में लेक्चरार बन कर वापस बनारस आ जाती है और चाहती है कि सास-ससुर साथ रहें। खुलासा बाद में होता है कि उनके बेटे ने किसी और से शादी कर ली है। काफी सकुचाते हुए मिस्टर एंड मिसेज रग्घू पहुंचते हैं बनारस की अशोक विहार कॉलोनी स्थित अपनी बहू के घर, जहां सास-बहू के सनातन तनाव के चलते मिसेज रग्घू की पटरी बहू के साथ नहीं बैठ पाती और वे बेटी के यहां मिर्जापुर चली जाती हैं। इसके बाद उपन्यास में इस पात्र का जिक्र नहीं है।
जिस गांव को रग्घू पीछे छोड़ आए, वहां बदलाव की बयार बह रही है। दलितों का सशक्तीकरण हुआ है, उन्होंने ठाकुरों-बामनों के यहां काम करने से इनकार कर दिया है। इस स्पेस को भरने के लिए ठाकुरों के करीब यादव आ गए हैं और नया जातीय समीकरण उभर रहा है। उधर जिस शहर में रग्घू गए हैं, वह मोहल्लों-महालों का नहीं बल्कि कॉलोनियों, विहारों और नगरों का शहर बन चुका है। ये वही शहर है जिसके बारे में काशीनाथ ने पहले लिखा है ‘कौन ठगवा नगरिया लूटल हो‘। यह लुटा हुआ बनारस है, जहां विहारों और कॉलोनियों में बसते हैं रिटायर्ड बूढ़े और अपंग, जहां रोजाना दिनदहाड़े किसी वृद्ध के लुटने-पिटने और डकैती-हत्याओं की खबर आम हो चुकी है, जहां हंसी गायब है, जहां तमाम किस्म की असुरक्षा के बीच सिर्फ गांव की स्मृतियों को बचाने की कवायद जारी है। यहीं रग्घू को बरसों बाद अपना एकाकी साथ मिलता है जो बहू के साथ दोस्ताना संबंधों के चलते सजीव हो उठता है,लेकिन गांव की ज़मीन उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ती। अपनी ईमानदारी और भलमनसाहत से ऊब चुके रघुनाथ के मन में अंत समय में खल पैदा होता है। जमीन के कागज़ात पर जबरन दस्तखत करवाने आए दो गुंडों के साथ सौदा कर वे अपना अपहरण करवा लेते हैं, और देखिए कि यह सुख रग्घू के लिए कितना अप्रतिम है-
‘रघुनाथ जब छड़ी के सहारे बाहर आए तब उनका चेहरा बन्दरटोपी के अंदर था और रजाई लड़के के कंधे पर! वे आगे-आगे,दोनों अपहर्ता लड़के पीछे-पीछे- जैसे वे बेटों के साथ मगन मन तीरथ पर जा रहे हों।‘
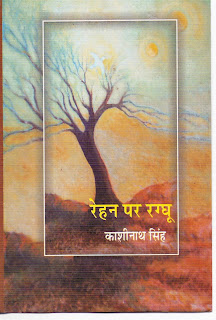 उपन्यास ‘रेहन पर रग्घू‘का आख्यान जितना सपाट दिखता है, उतना है नहीं। इसमें समूचे समाज में हो रहे बदलावों की खतरनाक आहटें हैं जो लेखक के नज़रिये से या कहें रघुनाथ के तटस्थ नज़रिये से भले ही सकारात्मक जान पड़ती हों, लेकिन जो समाज में सामूहिकता और सहकारिता को तोड़ने वाली साबित होती हैं। जहां व्यक्ति अकेला, और अकेला पड़ता जाता है। जहां सीधे-सपाट जीवन का अंत आत्मघात से बेहतर नहीं सूझता- बता दें कि उपन्यास की शुरुआत जिस अध्याय से होती हैवही अध्याय उसका अंत भी होता है,जिसमें रघुनाथ आखिरकार खुद को मुक्त करने के लिए सचेतन तौर पर आत्महत्या न सही, तो बेफिक्री के आलम में जर्जर शरीर लिए तूफान में निकल पड़ते हैं। इसे हम विशुद्ध बनारसी ठाठ कह कर भी पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। खुद का अपहरण करवाना इसी प्रवृत्ति का एक भिन्न संस्करण मात्र है।
उपन्यास ‘रेहन पर रग्घू‘का आख्यान जितना सपाट दिखता है, उतना है नहीं। इसमें समूचे समाज में हो रहे बदलावों की खतरनाक आहटें हैं जो लेखक के नज़रिये से या कहें रघुनाथ के तटस्थ नज़रिये से भले ही सकारात्मक जान पड़ती हों, लेकिन जो समाज में सामूहिकता और सहकारिता को तोड़ने वाली साबित होती हैं। जहां व्यक्ति अकेला, और अकेला पड़ता जाता है। जहां सीधे-सपाट जीवन का अंत आत्मघात से बेहतर नहीं सूझता- बता दें कि उपन्यास की शुरुआत जिस अध्याय से होती हैवही अध्याय उसका अंत भी होता है,जिसमें रघुनाथ आखिरकार खुद को मुक्त करने के लिए सचेतन तौर पर आत्महत्या न सही, तो बेफिक्री के आलम में जर्जर शरीर लिए तूफान में निकल पड़ते हैं। इसे हम विशुद्ध बनारसी ठाठ कह कर भी पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। खुद का अपहरण करवाना इसी प्रवृत्ति का एक भिन्न संस्करण मात्र है। शुरू से लेकर अंत तक कथाक्रम को विभिन्न उपाख्यानों के माध्यम से काफी दिलचस्प बनाया गया है- मसलन, रघुनाथ की बेटी का हिंदी के एक बूढ़े मास्टर के साथ प्रेम प्रसंग आदि। स्त्री-पुरुष के संबंधों के बारे में भी एक अविवाहित महिला पात्र के माध्यम से विमर्श की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वह केंद्रीय विषय से कहीं भी विचलन है। भाषा तो खैर वही ज़मीनी और बनारसी लहजे वाली है, जिसे हम काशीनाथ सिंह की ‘ब्रांड‘ भाषा कह सकते हैं।
जैसा कि महाश्वेता देवी कहती हैं, काशीनाथ सिंह सीधे-सादे हैं ‘तीसरी कसम‘ के हीरामन की तरह- ठीक यही बात उपन्यास के केंद्रीय पात्र रघुनाथ पर भी लागू होती है। दरअसल, यह रघुनाथ कोई और नहीं बल्कि देश भर की उस बुढ़ाती पीढ़ी का प्रतिनिधि है जो पिछले एक दशक में आई नवउदारवादी संस्कृति की आंधी में आत्मघात करने को अभिशप्त हो चला है। सीधी पटरी पर चलने वाले जीवन का अचानक इस दौर में अप्रासंगिक हो जाना ही रेहन पर जी रहे रग्घू की नियति है। यह दुनिया उसके लिए ऐसी टूटी मुंडेर है जहां से नीचे गिरना तय है…देरी है तो बस इस बात की कि लड़खड़ाते समय की चूल कब पूरी तरह उखड़ पाती है।
यहां भी पढ़ें
Read more

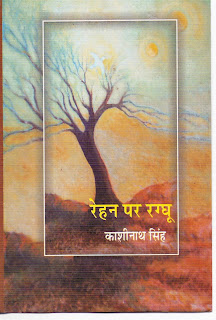 उपन्यास ‘रेहन पर रग्घू‘का आख्यान जितना सपाट दिखता है, उतना है नहीं। इसमें समूचे समाज में हो रहे बदलावों की खतरनाक आहटें हैं जो लेखक के नज़रिये से या कहें रघुनाथ के तटस्थ नज़रिये से भले ही सकारात्मक जान पड़ती हों, लेकिन जो समाज में सामूहिकता और सहकारिता को तोड़ने वाली साबित होती हैं। जहां व्यक्ति अकेला, और अकेला पड़ता जाता है। जहां सीधे-सपाट जीवन का अंत आत्मघात से बेहतर नहीं सूझता- बता दें कि उपन्यास की शुरुआत जिस अध्याय से होती हैवही अध्याय उसका अंत भी होता है,जिसमें रघुनाथ आखिरकार खुद को मुक्त करने के लिए सचेतन तौर पर आत्महत्या न सही, तो बेफिक्री के आलम में जर्जर शरीर लिए तूफान में निकल पड़ते हैं। इसे हम विशुद्ध बनारसी ठाठ कह कर भी पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। खुद का अपहरण करवाना इसी प्रवृत्ति का एक भिन्न संस्करण मात्र है।
उपन्यास ‘रेहन पर रग्घू‘का आख्यान जितना सपाट दिखता है, उतना है नहीं। इसमें समूचे समाज में हो रहे बदलावों की खतरनाक आहटें हैं जो लेखक के नज़रिये से या कहें रघुनाथ के तटस्थ नज़रिये से भले ही सकारात्मक जान पड़ती हों, लेकिन जो समाज में सामूहिकता और सहकारिता को तोड़ने वाली साबित होती हैं। जहां व्यक्ति अकेला, और अकेला पड़ता जाता है। जहां सीधे-सपाट जीवन का अंत आत्मघात से बेहतर नहीं सूझता- बता दें कि उपन्यास की शुरुआत जिस अध्याय से होती हैवही अध्याय उसका अंत भी होता है,जिसमें रघुनाथ आखिरकार खुद को मुक्त करने के लिए सचेतन तौर पर आत्महत्या न सही, तो बेफिक्री के आलम में जर्जर शरीर लिए तूफान में निकल पड़ते हैं। इसे हम विशुद्ध बनारसी ठाठ कह कर भी पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। खुद का अपहरण करवाना इसी प्रवृत्ति का एक भिन्न संस्करण मात्र है। 


