ठहरो मेरे पास यही एक अच्छी कमीज़ है। उसने कमीज़ उतारी और पिता से कहा कि अब पीट लो।
खबर गोवा की है, लेकिन आजकल यह घटना कहीं भी घट सकती है। एक ड्राइवर है, जो महामारी के पहले 700 रुपए रोज कमाता था। चार महीनों में वह कुछ भी नहीं कमा सका। अब फिर काम पर जाने लगा है, पर अब उसे सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं। उसके घर में उसकी मां है, पत्नी है और तीन बच्चे हैं। 18 साल की बेटी, 16 साल का बड़ा बेटा और 12 साल का छोटा बेटा।
वह बच्चों की पढ़ाई को बहुत जरूरी मानता है, इसलिए गरीबी के बावजूद तीनों को पढ़ा रहा है। उसकी पीठ में तकलीफ है, लेकिन वह ड्राइवरी नहीं छोड़ सकता। बच्चे उसकी परेशानी समझते हैं, इसलिए बड़ा बेटा कहता है कि वह 12वीं के बाद काम करने लगेगा और उसे काम नहीं करने देगा।
लेकिन बेटा स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई करता था। 11 अक्टूबर को उसके फोन की स्क्रीन टूट गई और उसने पिता से कहा कि फोन ठीक कराने के लिए 2000 रुपए चाहिए। पिता ने कहा कि फिलहाल उसके पास सिर्फ 500 रुपए हैं, चार दिन बाद ही वह 2000 का इंतजाम कर पायेगा। बेटा चार दिन की पढ़ाई के नुकसान की बात करने लगा तो पिता को गुस्सा आ गया।
बेटे की पिटाई करने के लिए उसने उसका कॉलर पकड़ा तो बेटे ने कहा, ठहरो मेरे पास यही एक अच्छी कमीज़ है। उसने कमीज़ उतारी और पिता से कहा कि अब पीट लो। पिता ने उसे पीटा तो नहीं, पर डांटा। अगले दिन सुबह पिता काम पर जाने लगा तो बेटे ने कहा कि पीटना है तो पीट लो, शाम को मौका नहीं मिलेगा।
और शाम को पिता जब काम पर से लौट रहा था, उसे घर से सूचना मिली कि 16 साल के बड़े बेटे ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है।
पिता का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए क्या गरीब लोग फोन का खर्च उठा सकते हैं।
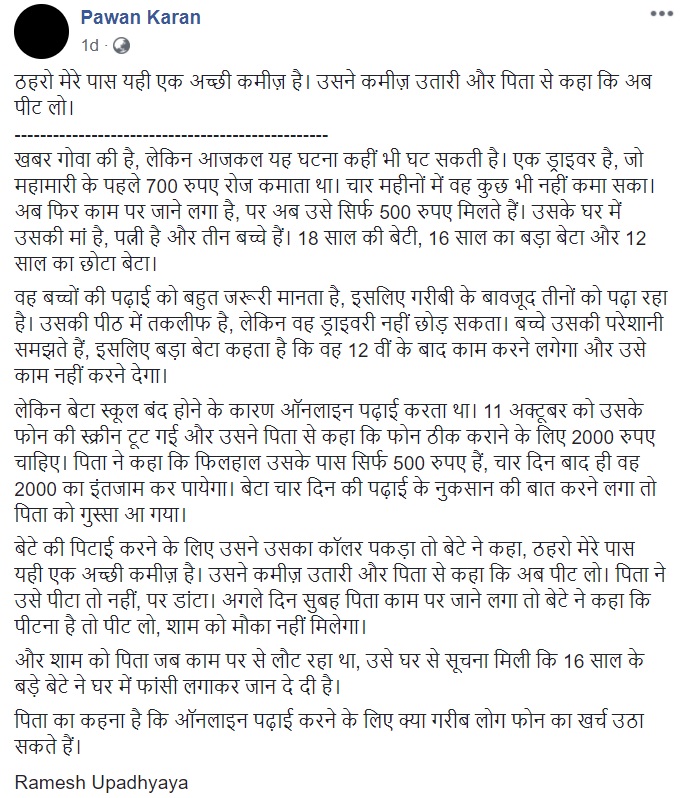
यह एक दर्दनाक कहानी है जो कवि पवन करण ने कथाकार रमेश उपाध्याय की दीवार से लेकर अपने दीवार पर लगाई थी। वास्तव में रीढ़ को सिहरा देने वाले विवरणों से भरी यह कहानी गहरे अवसाद में लाकर छोड़ देती है। इसमें गरीबी और लाचारी की जो ज़मीन दिखाई पड़ रही है फिलहाल भारतीय निम्नवर्ग इसी पर खड़ा है। दूसरा कोई चारा नहीं है। दूसरी कोई जमीन नहीं है। एक आदमी कमा रहा है और छः आदमी खाने वाले हैं। आलू चालीस रुपए किलो है। प्याज सौ रुपए और दाल एक सौ तीस रुपए तक पहुँच गयी है। चावल और आटा तीस रुपए से ऊपर ही हैं। गैस की महंगाई के बारे में लोग अखबारों में पढ़ ही रहे हैं। रोज़मर्रा के खर्चों में और भी छिट-पुट न जाने कितने खर्च होंगे। दूध, तेल, हरी सब्जियाँ, मछली, मंजन, दवाएँ और कपड़े! कपड़े की स्थिति तो बच्चा ही बता रहा है कि मेरे पास एक ही अच्छी कमीज है।
छः लोगों के एक परिवार में प्रतिदिन पाँच सौ रुपये यानी तिरासी रुपए फी आदमी। कम से कम दो बार तो भोजन अनिवार्य है। और इस पाँच सौ में भी तीन बच्चे तो पढ़ने वाले हैं। पिता बच्चों की पढ़ाई को आवश्यक मानता है इसलिए अपनी पीठ में भीषण दर्द के बावजूद उसने ड्रायवरी नहीं छोड़ी। बच्चे इस बात को समझ रहे थे कि पिता का काम अब पहले से अधिक मशक्कत का हो गया है और उस मशक्कत का दाम अधिक सस्ता हो गया है। इतना कि अगर पिता ने पीठ दर्द को नकार दिया है तो बड़ा बेटा सोचने लगा है कि बारहवीं पास करते ही वह काम करने लगेगा। लगता है सबने जिंदगी के कठिन हालात से लड़ने के लिए अपने आप को ढाल लिया है।
प्रायः निम्न वर्गीय जीवन में यह सामंजस्य साधारण बात है। इच्छाएं की। पूरी हुईं तो हुईं नहीं हुईं तो कोई बात नहीं। यह एक तरह से गहरी उदासीनता को जन्म देने वाली प्रवृत्ति बन जाती है। सफलता कोई फ़िनामिना ही नहीं बन पाती। जैसे-तैसे गुजर जाय तो अच्छा। इसीलिए गालिब बार-बार कहते थे कि अरमान तो पूरे ही नहीं हुए। बहुत अरमान किए लेकिन फिर भी कम ही किए और यह तो पता ही नहीं तमन्ना का दूसरा कदम कहाँ है क्योंकि एक ही कदम में इच्छाओं के जंगल हैं। खो गया हूँ। साधारण आदमी इसी में अपने जीने का समीकरण बना लेता है। क्या खाना जरूरी है से ज्यादा क्या नहीं खाने से भी काम चल जाएगा, इसका कौशल विकसित कर लेना। इसलिए जब पीठ दर्द से पीड़ित पिता को देखकर बड़ा बेटा जब बारहवीं पास करने के बाद काम करने की बात करता है तो इसे साधारण बात नहीं माना जाना चाहिए बल्कि यह हमारे निम्न वर्ग का आर्थिक आईना है। ऐसा आईना जिसमें आप केवल लोगों का नहीं, स्टेट का भी चेहरा देख सकते हैं।
ऊपर जिस परिवार की बात की जा रही है वहां जो घटना घटी वह साधारण घटना नहीं है। वह बहुत सी ऐसी बातों की ओर इशारा करती है जो हमारे जीवन में जड़ जमा चुकी हैं और उनका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है, लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। चूंकि पकड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए उनसे लड़ भी नहीं पा रहे हैं। उस परिवार में आर्थिक अभाव से पैदा हुई एक गहरी लाचारी है। किसी का भी दिमाग स्थिर नहीं है। स्थिर हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। अगर इतने अभाव और लाचार होने के बावजूद दिमाग स्थिर है तो इसका मतलब है सहनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आदमी ने हर हाल में जीना सीख लिया है। उसमें असंतोष और गुस्सा नहीं है। वह दुनिया को बदलने के बारे में सोचना छोड़ दिया है। इसलिए जरूरी हो कि दिमाग अस्थिर हों लेकिन इस परिवार में जो अस्थिरता है वह तो आत्मघात की ओर ले जा रही है। वह त्रासदियों में जीवन को लपेट रही है। एक संभावनाशील जवान लड़का अपने ही गले में रस्सी डालकर लटक जा रहा है। एक तरफ वह पिता की मशक्कत से इतनी संवेदना रखता है कि बारहवीं पास करते ही काम करने लगेगा और दूसरी तरफ जीवन से ही हाथ धो लेता है। क्या यह महज़ एक परिवार की त्रासदी है? क्या इसे एक लड़के की त्रासदी माना जाना चाहिए? आखिर वह कौन सी व्यवस्था है जो निम्नवर्गीय लोगों, किसानों, मजदूरों को आत्मघात की तरफ ले जा रही है?
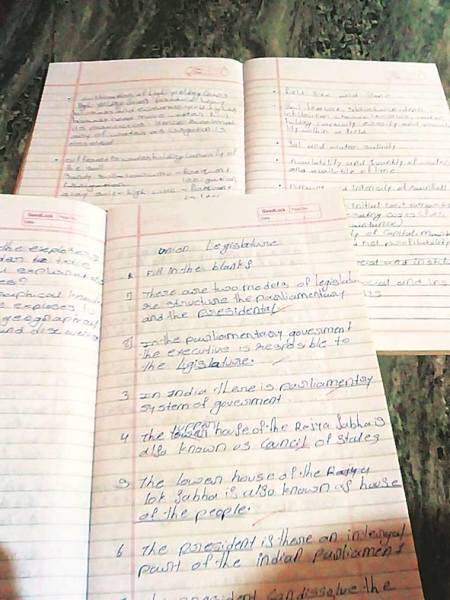
एक तरफ अमित शाह का लड़का है जो एक साल में अपनी संपत्ति सोलह हज़ार करोड़ गुना बढ़ा लेता है। दूसरी तरफ आत्मघात करने वाला यह युवा अपना टूटा हुआ मोबाइल भी नहीं बनवा पा रहा है। वह पिता की मजबूरी नहीं समझ पा रहा है कि उसके पास दो हज़ार रुपए नहीं हैं तो उसे क्या करना चाहिए। क्या अपने पिता की आर्थिक सीमाओं को समझते हुए कुछ दिन के लिए पढ़ाई रोक देनी चाहिए? बहुत से सवाल हैं। लड़का पढ़ाई में पिछड़ जाने को लेकर भारी दबाव में है। उसे लगता है एक साल खराब हो जाएगा। जिंदगी को लेकर उसने जो लक्ष्य तय किए हैं वे पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने पिता द्वारा दिये गए चार दिन के आश्वासन पर भी वह आश्वस्त नहीं है। उसके भीतर इस गरीबी को लेकर एक क्षोभ है। वह पिता से अधिक ज़ोर देकर कहता है कि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा और पिता अपनी लाचारी छिपने के लिए उसका कॉलर थाम लेता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरह के हालात इस परिवार में हैं उससे एक सौ तीस करोड़ लोगों में से कितने पिता अपनी लाचारी छिपाने के लिए बच्चे का कॉलर पकड़ लेते होंगे? क्या हमारे पास इसका कोई विश्वसनीय आंकड़ा है कि इस देश में कितने स्कूली बच्चों के घरों में एंड्रायड मोबाइल है ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें? जब महामारी में स्कूल बंद कर दिये गए तब भी वर्चुअल पढ़ाई पर इतना ज़ोर क्यों है? क्या मोबाइल कंपनियों ने आपदा में अवसर तलाशने के लिए कोई गोपनीय अभियान चलाया है जिसका सिरा बच्चों की शिक्षा तक जा रहा है?
क्या अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों और प्रबन्धकों को इस बात का अंदाजा है कि उनके स्कूल के कितने विद्यार्थियों के पास मोबाइल है? उन्हें महामारी के दौर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में मददगार होना चाहिए था ताकि वातावरण साधारण हो, लेकिन उन्होंने अपना कारोबार चालू रखा। उन्होंने बच्चों के पिछड़ जाने का भय दिखाया और लगभग मजबूर कर दिया कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाय, लेकिन विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं किया गया। जिस देश में शिक्षा का क्या उद्देश्य है यही नहीं पता है वहाँ शिक्षा में पिछड़ने का क्या तात्पर्य है? जिस देश में शिक्षा ने बेरोजगारों की फौज पैदा की है उस देश में साल-छः महीने में ही दुनिया पलट रही है? क्या हम कभी इस बात को समझ सकते हैं कि इस समय बड़ा से बड़ा विशेषज्ञ भी एक शातिर गंवार के इशारों पर नाचने के लिए विवश है और जिन चीजों पर स्पष्ट रूप से वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों की राय के अनुसार काम होना चाहिए उन पर मुनाफाखोर बनिये निर्णायक भूमिका में हैं।
एक लाचार पिता और क्षुब्ध बेटे के बीच व्यवस्था और सत्ता की कितनी ताक़तें काम कर रही होती हैं? इस देश में ऐसे पिताओं और बेटों की संख्या कम नहीं है। जब ऐसे अभावग्रस्त और लाचार लोगों की संख्या कम नहीं है तो यह सवाल उठता है कि स्टेट क्या कर रहा है? साफ-साफ दिख रहा है कि सभी जरूरी चीजों पर चंद लोगों का शिकंजा कसता जा रहा है। तमाम क़ानूनों और प्रावधानों से मेहनतकशों और किसानों को वंचना और लाचारी की गहरी खाइयों में धकेला जा रहा है। एक तरफ अनियंत्रित मुनाफे की सुनियोजित प्रणाली काम कर रही है और दूसरी ओर पहले से भी कम आमदनी हो रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम से मुक्त की गई वस्तुओं पर मुनाफाखोरों का नियंत्रण बढ़ गया है। लोग आकुल-व्याकुल हैं। हर जगह असुरक्षित और अधिकतम गरीब हैं। अपने खेतों और घरों पर आए संकटों से लड़ रहे हैं। अपने छूट गए रोजगारों को वापस पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी दुकानों और रिक्शों-ठेलों को फिर से दुरुस्त कर रहे हैं और स्टेट पुलिस को अपने षडयंत्रों को अंजाम देने के लिए उतार चुका है। न्यायाधीश झूठे फैसले दे रहे हैं। वे स्टेट के दबाव में किसी को भी जेल में डालने और बेदखल करने के फैसले लिख रहे हैं। क्या इन सबका उस लड़के की मौत से कोई भी ताल्लुक नहीं? एक सड़ांध भरे संसार प्रभाव आखिर जन साधारण पर क्या पड़ता होगा। किसी आदमी की बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, आर्थिक विपन्नता और लाचारी क्या कहीं बाहर से आती होगी।
आत्महत्याएं मुझे विचलित करती हैं। निजी रूप से मैं उस आत्महंता को दोष नहीं देता हूँ लेकिन लगता है कि जीवन का दामन नहीं छोडना चाहिए। एक लड़का जो अपने पिता की मजबूरियों और आर्थिक सीमाओं को समझ रहा था उसे इतने अकेलेपन में नहीं होना चाहिए था कि वह सबकुछ खत्म कर लेता। वह उन विकल्पों में से कोई एक चुन लेता जो ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति चुनता है। आखिर उस इकलौती कमीज का क्या उपयोग जब वह रहा ही नहीं। और यह कहना कि अभी पीटना है तो पीट लो, शाम को मौका नहीं मिलेगा, बहुत भयानक और खतरनाक संकेत है। लगता है कि गोया उसके मन में जो उथल-पुथल चल रही थी उसमें उसने पहले से तय किया हुआ था कि उसे आत्महत्या कर लेनी है। आखिर उसे इस कगार पर कौन लाया? कम से कम अब यह बात तो साफ है कि वह लड़का बाप के प्रति संवेदनशील नहीं था और जिस पढ़ाई में पिछड़ जाने का उसके अंदर भय था वह पढ़ाई भी उसे कोई तार्किक युवा नहीं बना सकी। वह अपनी सुविधाओं और जरूरतों के लिए ही चैतन्य था। नहीं मिलने पर आपे से बाहर हो जाना उसकी मानसिकता बन गई थी। ऐसी पीढ़ियाँ किसने तैयार की है? माता-पिता ने या इस पूरी व्यवस्था ने?
मैं उन गरीब और लाचार, मेहनत-मशक्कत से अपने बच्चों को पालने और उनको पढ़ाने की आकांक्षा रखनेवाले पिताओं की तकलीफ़ों को समझता हूँ। आखिर सपना देखने वाले पिता कितने हैं। एक तरफ सारी दुनिया की संपत्ति लूट कर अपनी पीढ़ियों को सम्पन्न, अकर्मण्य और अय्याश बना देने वाले मंत्री, अफसर, किरानी, व्यापारी, माफिया, सांसद-विधायक हैं और दूसरी ओर इच्छाओं और अभाव के बीच झूलते श्रमजीवी पिता हैं। ऐसे पिता कितने अपराधी ठहराए जा सकते हैं।
गालिब कहते हैं कि ‘नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, या रब अगर इन कर्दा गुनाहों की सज़ा है‘!
बेचारे और दुर्भाग्यशाली पिता। मोबाइल नहीं दिला पाएं, लेकिन सपने तो देख ही रहे होते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लें और इतना तो पढ़ ही लें कि मेरी तरह पीठ दर्द के बावजूद गाड़ी न चलानी पड़े। लेकिन सपने निरापद नहीं रहे। कौन उनके सपनों को तहस-नहस कर रहा है!





