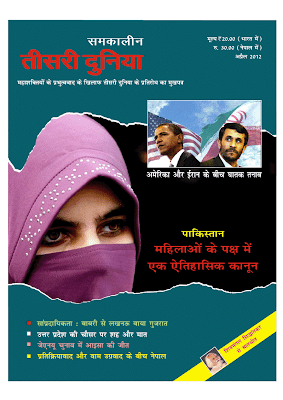प्रस्तुत लेख मैंने तीसरी दुनिया के अप्रैल अंक के लिए लिखा था। अब वह प्रकाशित हो चुका है, इसलिए पूरा लेख जनपथ पर डाल रहा हूं। यह लेख उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद उभरी तस्वीर का एक जायज़ा है सांप्रदायिकता विमर्श के दायरे में। इससे कई असहमतियां भी हो सकती हैं। प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं।
पहला सवाल
गुजरात दंगों के दस साल बाद और बाबरी विध्वंस के बीसवें साल में अगर अचानक यह सवाल खड़ा हो जाए कि हिंदुस्तान की सांप्रदायिक राजनीति का नया चेहरा कौन है, तो शायद जवाब तलाशने में दिक्कत होगी। यह सवाल उतना आसान नहीं है जितना ऊपर से जान पड़ता है। कुछ ताज़ा रुझानों पर ज़रा ग़ौर करें।
अभी पिछले दिनों पांच राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। बात सांप्रदायिकता की कर रहे हैं तो ज़ाहिर है शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा तीसरे स्थान पर रही। सेकुलर लोग इस बात से संतोष कर सकते हैं कि उसे पिछली दफा के मुकाबले चार सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन जिस प्रमाद और निश्चिंतता के साथ भाजपा नेतृत्व ने यह चुनाव लड़ा, उस लिहाज़ से 47 सीटों पर जीत को बेहतर प्रदर्शन कहा जाएगा। भाजपा के रणनीतिकार इस बार राजनाथ या कलराज मिश्र नहीं थे। नितिन गडकरी के निर्देशन में यह चुनाव लड़ा गया था। इस बात को एक से ज्यादा बार कहे जाने की ज़रूरत है। और यह भी, कि उमा भारती की जीत ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि उन्हें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में निपटाने के लिए लाया गया था। पंजाब की ओर बढ़ें, तो वहां शिरोमणि अकाली दल-भाजपा की सरकार बन रही है। उत्तराखंड में 31 सीटों के साथ भाजपा कांग्रेस से महज़ एक सीट पीछे है और सरकार बनाने का खेल बसपा के विधायकों के समर्थन पर टिका है, जबकि गोवा में भाजपा सरकार बना रही है। यानी चार राज्यों में भाजपा दो में दूसरे स्थान पर, एक में पहले और एक में तीसरे स्थान पर है। नितिन गडकरी ने इन चुनावों को कांग्रेस के खिलाफ जनादेश बताते हुए कहा है कि जनता का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। यह बात उतनी ही घिसी-पिटी है जितनी यह, कि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं इसलिए वह बार-बार भाजपा या कांग्रेस में से किसी एक को चुनती है। तो आखिर इन नतीजों का सबक क्या है? ज़रा पीछे चलें और दो बातें याद करें।
पहली बात, पिछले साल पूरे देश में चला भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसका शुरुआती चेहरा बाबा रामदेव बने और स्थायी चेहरा अन्ना हज़ारे। इस आंदोलन ने कांग्रेस को बीते चुनावों में निश्चित तौर पर काफी चोट पहुंचाई है, लेकिन इस बात को कहते हुए भूलें नहीं कि उत्तराखंड में भाजपाई निशंक की सरकार और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल-भाजपा की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, वहीं उत्तर प्रदेश की जनता अब भी समाजवादी पार्टी के राज में हुआ भ्रष्टाचार भूल नहीं पाई है। गोवा में खनन घोटाला भाजपा का किया है या कांग्रेस का, इसे समझने में ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री दिगंबर कामत टिकट नहीं मिलने पर 1994 में कांग्रेस से भाजपा में आए जब वह बाबरी की लहर पर सवार थी। उसके बाद 2005 में दोबारा इसी वजह से कांग्रेस में वापस चले गए थे। गोया दो बातें कही जा सकती हैं- या तो भ्रष्टाचार इस चुनाव में मुद्दा नहीं था, या फिर कांग्रेस का भ्रष्टाचार ही मुद्दा था, बाकी का नहीं। आप रामदेव और अन्ना की फेहरिस्त में 2जी घोटाले के ”क्रूसेडर” सुब्रमण्यम स्वामी का नाम भी जोड़ सकते हैं जो दक्षिणपंथ की ही एक अन्य राजनीतिक धारा के प्रतिनिधि हैं। बहरहाल, जनादेश का पूरा सम्मान करते हुए यह बात कही जा सकती है कि उत्तराखंड, गोवा और पंजाब की जनता ने सांप्रदायिक पार्टी के भ्रष्टाचार को दरकिनार करते हुए उसकी सांप्रदायिकता को चुनने का फैसला लिया है। भ्रष्टाचार तो अनुलग्नक की तरह नत्थी है ही। लेकिन रुकिए, बात पूरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश अभी बाकी है।
जो दूसरी बात गिनाए जाने की ज़रूरत है, उसके लिए चुनाव के दौरान शाही इमाम बुखारी का बयान याद करना पड़ेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील की थी कि वे समाजवादी पार्टी को वोट दें। इस बात को हम हलके में लेकर निकल गए थे। हमने सोचा कि मुसलमान ”टैक्टिकल वोटिंग” करेगा, बाकी पीस पार्टी और कौमी एकता दल जैसे दलों की मौजूदगी ने भ्रम को और बढ़ा दिया। नतीजा? बसपा को 126 सीटों का नुकसान और सपा को 127 सीटों का फायदा हुआ। ज़ाहिर है, सपा के लिए यह भरपाई उन्हीं मुस्लिम वोटों ने की है जो पिछली बार मायावती के साथ चले गए थे, और कोई फैक्टर सपा की सीट वृद्धि में प्रत्यक्षत: नहीं दिखता। तो क्या बुखारी की अपील ने काम किया? यदि ऐसा है, तो स्थिति गंभीर मानी जा सकती है क्योंकि किसी संप्रदाय के धर्मगुरु द्वारा की गई राजनीतिक अपील को सांप्रदायिकता न कहें तो और क्या कहें (भले वह संप्रदाय अल्पसंख्यक ही क्यों न हो), खासकर तब जब इस सूरत में संबद्ध राजनीतिक दल बहुमत हासिल कर चुका हो? तो क्या इस बात को कहने का जोखिम उठाया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली नई सरकार अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की लहर पर सवार है?
अब उन सभी राज्यों को मिला कर देखें (मणिपुर छोड़ कर) जहां चुनाव हुए हैं। चारों राज्यों की जनता ने जाने-अनजाने सांप्रदायिकता को चुना है और भ्रष्टाचार (कांग्रेसी) के खिलाफ वोट दिया है। इस संदर्भ में एक बात यहां विस्तार से बताई जानी ज़रूरी है। चूंकि अन्ना और रामदेव के आंदोलनों का केंद्र दिल्ली में था, चूंकि लोकपाल विधेयक केंद्र की कांग्रेसनीत सरकार को पारित करना था, चूंकि काला धन विदेश से मंगवाने की जि़म्मेदारी कांग्रेस की थी, चूंकि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला यूपीए के कार्यकाल में हुआ (और भी बहुत कुछ) – लिहाज़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस का प्रधान पक्ष हो गया और कांग्रेसी सांप्रदायिकता (या ऐसी ही अन्य प्रतिगामी प्रवृत्तियां) गौड़ हो गईं। इस तरह एक प्रक्रिया में कांग्रेस का पर्याय भ्रष्टाचार को बना दिया गया। बीच-बीच में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड आदि से भाजपा के भ्रष्टाचार की खबरें सिर उठाती रहीं, लेकिन उन्हें संतुलित करने के लिए पहले से नरेंद्र मोदी और नीतिश कुमार का बहुप्रचारित सुशासन मौजूद था। एक ओर रामदेव, अन्ना और सुब्रमण्यम स्वामी जैसों का ‘क्रूसेड’ भाजपाई भ्रष्टाचार की कहानी को डाइल्यूट करता रहा, तो दूसरी ओर सुशासन, सद्भावना और विकास का ‘मोदी’ मॉडल भाजपाई सांप्रदायिकता की छवियों को धुंधला करने में लगा रहा। ये सब समानांतर प्रक्रियाएं थीं जिनके तहत भाजपा के पुराने नेताओं को उत्तर प्रदेश के चुनाव में किनारे लगाया गया, नितिन गडकरी यानी संघ के प्रतिनिधि ने कमान अपने हाथ में ले ली, उमा भारती ने बुंदेलखंड को संभाला और तकरीबन पिछला प्रदर्शन करते हुए भाजपा में ‘पावर शिफ्ट’ बड़े महीन तरीके से संघ की ओर हो गया। इस दौरान अयोध्या (फैजाबाद) से लल्लू सिंह की हार और किन्नर प्रत्याशी को मिले 22000 से ज्यादा वोट जैसी घटनाओं को अपवाद माना जा सकता है, लेकिन भाजपा से कभी भी जीतने की उम्मीद नहीं की गई थी, लिहाज़ा उस पर कोई सवाल नहीं है। हालांकि अपवाद ही नियम को सिद्ध करता है, यह बात समझने के लिए हमें कुछ दूसरी दिशाओं में जाने की ज़रूरत है।
सांप्रदायिक राजनीति का पहला चरण1
दरअसल, ऊपर कही गई सारी बातों का प्रस्थान बिंदु या कहें निष्कर्ष एक ही है, कि सांप्रदायिकता का धर्म से कोई लेना-देना नहीं। सांप्रदायिकता अपनी बुनियाद में एक राजनीति है, फिर इसका आवरण चाहे जो भी हो। अगर यह धार्मिक प्रवृत्ति होती, तो मध्यकालीन होती। संगठित धर्म को मानने वाले समूहों के स्वार्थ (हित) इसे जन्म देते हैं। एक बात और है। सांप्रदायिकता का आम जनता से कोई लेना-देना नहीं। यह पढे-लिखे मध्यवर्ग की पैदा की हुई परिघटना है, जिसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के शासनकाल में होती दिखती है और जिसकी परिणति देश के विभाजन में होती है। पचास के दशक में देश में कोई सांप्रदायिक तनाव प्रत्यक्षत: नहीं था। पहली बार आज़ादी के बाद 1962 में जबलपुर का दंगा हुआ था। यह दंगा हिंदू और मुस्लिम बीड़ी निर्माताओं के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा का नतीजा था। इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि एक हिंदू बीड़ी निर्माता की बेटी को और मुस्लिम बीड़ी निर्माता के बेटे से प्रेम हो गया था और दोनों के शादी करने के फैसले ने उन्माद पैदा कर दिया। जबलपुर का एक स्थानीय हिंदी अखबार लिखता है कि मस्जिद में लगे ट्रांसमीटर के ज़रिए पाकिस्तान जबलपुर के मुसलमानों से जुड़ा था और दंगे भडके थे। ऐसी अफ़वाहें दंगे भड़काने का बहुत काम करती थीं। साठ के दशक में पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के कारण दंगे पैदा हुए। दुर्गापुर, जमशेदपुर, रांची आदि जगहों पर हुए दंगे इसी का नतीजा थे। साठ के दशक में इंदिरा गांधी के सत्ता में आते ही धर्मनिरपेक्षता को लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ माना गया और मुसलमान कांग्रेसी खेमे में चले आए। वामपंथी और ब्राह्मण पहले से ही उनके साथ थे, लिहाजा इंदिरा गांधी का एकाधिकार सा कायम हो गया। इसे चुनौती देने के लिए गुजरात में पहली बार कांग्रेस(ओ), स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ ने हाथ मिलाया और सांप्रदायिक दंगे करवाए जिससे इंदिरा गांधी की साख को झटका लग सके। 1969 में अहमदाबाद का दंगा इसी परिघटना की पैदाइश था। अगले ही साल भिवंडी और जलगांव में दंगे हुए जिसमें शिवसेना का भी हाथ था। यह चरण भाषाई अस्मिता और सांप्रदायिक तत्व के मेल का था, जिसे शिवसेना ने अंजाम दिया। सत्तर के दशक में देखिए कि कैसे दंगे करवा चुकी जनसंघ ने अन्य के साथ मिल कर जनता पार्टी बना ली और महात्मा गांधी की समाधि पर धर्मनिरपेक्षता की झूठी कसम खाई। लेकिन ये नाटक जल्द ही खुल गया जब जनता पार्टी के भीतर दोहरी सदस्यता का विवाद पैदा हो गया। नतीजतन जनसंघ के सदस्यों ने आरएसएस की सदस्यता को छोड़ने से इनकार कर दिया। इस दौरान आरएसएस ने जमशेदपुर, बनारस और अलीगढ़ में दंगे करवाए क्योंकि समाजवादियों ने दोहरी सदस्यता पर आपत्ति जताई थी जिस वजह से जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। यह 1977-78 का दौर था। लगातार साबित हो रहा था कि सांप्रदायिकता दरअसल एक राजनीतिक परिघटना है जो धर्म के खोल में जनता के बीच मौजूद थी।
यह सिलसिला इंदिरा गांधी के उलटे रुख के बावजूद 1980 में कायम रहा। श्रीमती गांधी ने हिंदू समर्थित भावनाओं का फायदा इस बार उठाया। मीनाक्षीपुरम के दलितों द्वारा इस्लाम अपना लिए जाने पर वे चुप रहीं जिससे बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता का पहली बार प्रत्यक्ष राजनीतिक उभार हुआ। बिहारशरीफ(1981), मेरठ(1982), बंबई-भिवंडी(1984) और अहमदाबाद(1985) में दंगों का एक नया सिलसिला पनपा। जानकारों की मानें तो यही वह दौर था जब गुप्तचर एजेंसी आईबी और रॉ के भीतर मराठी ब्राह्मणों की भर्तियों का सिलसिला भी तेज़ हुआ और इसी दौर में कांग्रेस स्पष्ट तौर पर हिंदू सांप्रदायिकता को लेकर सबसे ज्यादा नरम हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ भड़के सांप्रदायिक दंगों के ज़ख्म अब भी हरे हैं जिनमें कांग्रेसियों की सीधी भूमिका को देख चुके कई लोग अब भी जिंदा हैं। कहा जा सकता है कि चौरासी का दंगा सांप्रदायिकता की राजनीति के पहले चरण का एंटी क्लाइमैक्स था क्योंकि अब तक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का राजनीतिक औजार कांग्रेस के हाथों में था, उसी कांग्रेस के हाथ में जिसने आज़ादी के बाद से लेकर अस्सी के दशक तक तमाम रणनीतिक संस्थानों का सांप्रदायीकरण किया और खुद को भारतीय राजनीति का सेकुलर चेहरा बनाए रखा। लेकिन सांप्रदायिकता की राजनीति अब भी पहले की तरह धर्म के आवरण में ही लिपटी हुई थी। शाह बानो मामले ने इस कवच को मज़बूत किया, बाबरी मस्जिद के दरवाज़े राजीव गांधी द्वारा खोले जाने ने आग में घी का काम किया और रामजन्मभूमि का पुराना जिन्न एक बार फिर बोतल से निकल आया। राजीव के मारे जाने के बाद वी.पी. सिंह द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, लेकिन इस बार हिंदू धर्म के आवरण में लिपटी सांप्रदायिकता ने रिटैलिएट किया। बरसों से कांग्रेसी सरकारों द्वारा पुचकारे जाने पर ये ताकतें मज़बूत हो चुकी थीं और इस बार हार नहीं मानने वाली थीं। मेरठ, भागलपुर, जयपुर, हैदराबाद आदि दंगे की चपेट में आए और आखिरकार बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। बंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता, पटना, बनारस सब जगह दंगे हुए। इस बार हालांकि सांप्रदायिकता का औज़ार अकेले कांग्रेस के हाथ में नहीं था। पुलिस, प्रशासन, राज्य, धार्मिक संगठन, नेता सबके अपने-अपने हित थे। कह सकते हैं कि बाबरी विध्वंस सांप्रदायिकता की राजनीति के पहले चरण का पटाक्षेप था। इसके दो लक्षण अहम थे- पहला, देश में दक्षिणपंथी पार्टी का स्पष्ट राजनीतिक उभार और दूसरा, दंगों से मुक्ति की ज़मीन का तैयार होना। इन दोनों के ज़मीन पर उतरने में हालांकि पांच-छह साल का वक्त लगा जब 1998 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बना। कहा गया कि देश अब गठबंधन के दौर में आ चुका है।
आखिरी दंगा
सुनने में अजीब लग सकता है कि दक्षिणपंथी पार्टी भाजपा के केंद्र में उभार के साथ दंगों से मुक्ति कैसे संभव है। अनुभव और तथ्य दोनों बताते हैं कि ऐसा ही हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने और एनडीए के सत्ता में आने के बाद बहुत सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिकता को धर्म के आवरण से बाहर निकाला गया। अब इसकी एक वजह आप गठबंधन धर्म के तौर पर भी गिना सकते हैं, तो दूसरी कांग्रेस द्वारा शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीति जो भाजपा को विरासत में मिली थी। अब भारत खुल चुका था दुनिया के लिए और यहां दंगों का पुराना रूढ़ फॉर्मूला काम नहीं आने वाला था। लेकिन भाजपा की एक दिक्कत यह भी थी कि उसने कभी राज नहीं किया था। अर्थव्यवस्था और प्रशासन को चलाने के तौर-तरीकों को सीखने में उसे वक्त लगना ही था और आर्थिक उदारीकरण की नीति को आगे बढ़ाना उसकी विकल्पहीनता (विवेकहीनता भी कह सकते हैं) का परिणाम था। वाजपेयी के रूप में भाजपा का राजनीतिक चेहरा भले ही उदार था, लेकिन अब भी उसकी लगाम संघ के हाथ में ही थी। संघ के भीतर आज भी सांप्रदायिकता और धर्म में कोई फर्क नहीं है, तब भी नहीं था। देश चलाने और वैचारिक एजेंडा लागू करने की कशमकश ने 2002 में इस देश का कथित तौर पर आखिरी दंगा करवाया। गुजरात जल चुका था, नरेंद्र मोदी हंस रहे थे और वाजपेयी चुप थे। मुसलमानों के इस नरसंहार को क्रिया की प्रतिक्रिया बताया गया। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार किया जा चुका था और पहली बार निजीकरण, उदारीकरण व भूमंडलीकरण के दस साल में ‘कंडीशन्ड’ हुआ शहरी मध्यवर्ग का एक तबका क्रिया-प्रतिक्रिया की परिभाषा को स्वीकार कर चुका था। ध्यान रहे बाबरी विध्वंस में शहरी मध्यवर्ग कहीं नहीं था और उस वक्त बाज़ार की ताकतें भी मौजूद नहीं थी। बाबरी प्रिमिटिव सांप्रदायिकता की आखिरी ‘स्टेज’ है, जबकि ‘गुजरात’ आधुनिक सांप्रदायिकता की पहली ‘स्टेज’। और यह फर्क महज़ दस साल में आया है। हम 1992 से 2002 को सांप्रदायिकता के चोला बदलने का संक्रमण काल मान सकते हैं।
गुजरात नरसंहार के वक्त किसी को नहीं पता था कि सांप्रदायिकता का चेहरा भविष्य में कैसा होने वाला है, लेकिन इसकी पहली तस्वीर हमें दिखती है गुजरात के विधानसभा चुनावों में जो दंगे के ठीक नौ महीने बाद होते हैं और जिसकी गर्भ से निकल कर आते हैं एक बार फिर नरेंद्र मोदी। इस अजीबोगरीब जनादेश पर शायद उस वक्त सभी चौंके थे, लेकिन अब यह बात समझ में आती है कि दरअसल 2002 के अंत तक शहरों में रह रही आम आबादी के बीच सांप्रदायिकता को एक हद तक स्वीकार्यता मिल चुकी थी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दस साल के आर्थिक सुधारों की चकाचौंध ने सांप्रदायिकता के प्रति लोगों को संवेदनहीन बना दिया था। बहरहाल, यह चमक ऐसे ही ज़ाया नहीं होनी थी। गुजरात में बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता का नया प्रयोग शुरू हो चुका था तो राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का फॉर्मेट भी बदला जा चुका था। दंगे वास्तव में जा चुके थे। अब विस्फोटों का दौर था।
नए प्रयोग2
मुंबई, मालेगांव-मोडासा, नांदेड़, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, समझौता बम विस्फोट, हैदराबाद मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, उत्तर प्रदेश की अदालतों में विस्फोट, जयपुर, बनारस, फिर मुंबई और दिल्ली… और अंत में देश पर हुआ कथित तौर पर सबसे बड़ा हमला जिसे हम सत्ता के दिए नाम 26/11 से याद करते हैं। देश में लगातार इतने बम पहले कभी नहीं फटे थे और इतने मुस्लिमों की गिरफ्तारी पहले कभी नहीं हुई थी। इस बात को कहने का हालांकि कोई मतलब नहीं, फिर भी शायद 26/11 अगर नहीं हुआ होता, तो सांप्रदायिकता के दूसरे चरण पर से आवरण हटने में देर लगती। लेकिन 26/11 में मारे गए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के नेतृत्व में तैयार की गई मालेगांव-मोडासा ब्लास्ट की चार्जशीट ने आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस के हाथ में सांप्रदायिक राजनीति का औज़ार इस तरह थमाया जिसके निशाने पर घोषित तौर पर सांप्रदायिक संगठन आ गए। एक के बाद एक कांग्रेस की बनाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आठ विस्फोटों में हिंदू चरमपंथियों का हाथ उजागर किया और साधु संत माने जाने वाले लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई। इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में हुए तमाम विस्फोटों में (26/11 को छोड़ कर) हिंदू संगठनों की साजि़श का परदाफाश हुआ। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक शब्दावली में इस किस्म के हमलों को फॉल्स फ्लैग अटैक कहा गया। इसका मतलब होता है दूसरे के बैनर तले अपनी कार्रवाई। इसे समझाने के लिए अकसर हिटलर का उदाहरण दिया जाता है जिसने अपनी ही संसद में बम फेंकवा कर उसका आरोप कम्युनिस्टों पर लगा दिया था। भारत में इसके सबूत भी मिले हैं। कानपुर में एक दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं के कमरे से मिली नकली दाढ़ी और पायजामे ने पहली बार साबित किया कि यहां ऐसे हमले होने शुरू हो चुके हैं।
इससे एक बात तो साफ हो गई कि दंगों को दरकिनार कर बड़े सुनियोजित तरीके से शहरी ठिकानों को उड़ाने का फॉर्मेट गुजरात दंगों के बाद इस देश में स्थापित किया गया था। कुछ बुद्धिजीवियों की तो यह राय 26/11 के बारे में भी है कि यह एक फॉल्स फ्लैग हमला था। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास के पास एक इज़रायली कार में हुआ हमला भी इसी श्रेणी का बताया गया, हालांकि हर बार की तरह इस बार भी एक मुस्लिम को ही निशाना बनाया गया। दिल्ली के प्रतिष्ठित पत्रकार अहमद काज़मी को इस मामले में पकड़ा गया है जिनके पक्ष में सईद नक़वी जैसे बड़े पत्रकार तक ने बयान दिए हैं। आम तौर पर ऐसे हमलों की सच्चाई छुपी ही रहती है जिसके कारण परिणाम लक्षित संप्रदाय को भुगतना पड़ता है जैसा कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम युवकों की धरपकड़ में हमने देखा है। लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार ने मालेगांव की चार्जशीट का इस्तेमाल आंशिक तौर पर फॉल्स फ्लैग हमलों को सुलझाने के लिए किया जिसके चलते हिंदू चरमपंथियों पर भी शिकंजा कसा जाने लगा। यह बात अलग है कि विस्फोटों के मामले में पकड़े गए कई मुस्लिम युवक अब तक जेल में बंद पड़े हैं। अपने ऊपर आंच आते देख प्रतिक्रिया में संघ और विश्व हिंदू परिषद समेत उनसे जुड़े संगठनों ने अपनी खुली सदस्यता के प्रारूप का फायदा उठाते हुए तमाम आरोपियों की खुद से संबद्धता को नकार दिया। स्वामी असीमानंद का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चित-पट और सियासी ब्लैकमेल के इस सांप्रदायिक खेल के बीच जनता भ्रम में थी, लिहाज़ा उसे भरमाना ज़रूरी था। इसके लिए सांप्रदायिकता की दो नई प्रतिमाओं का क्रमवार अनावरण किया गया। नरेंद्र मोदी और नीतिश कुमार। ये दोनों क्रमश: विकास पुरुष और सुशासन पुरुष के रूप में स्थापित किए गए। नरेंद्र मोदी ने सद्भावना मिशन चला कर गुजरात दंगे के दसवें साल में अपने ऊपर लगे खून के बचे-खुचे छींटे भी धो डाले और दूसरे छोर पर नीतिश कुमार पुराने समाजवादियों के नए सांप्रदायिक मुहावरे में फिट होने का नायाब उदाहरण बन गए। नवीन पटनायक और रमन सिंह भी इसी परंपरा के वाहक बने, हालांकि ‘हीरोइक’ तत्व की कमी के कारण राष्ट्रीय परिदृश्य पर उनका उभार अब तक अधूरा है।
पॉपुलर राइट
अब पुरानी सांप्रदायिक राजनीति विकास के नए लिहाफ में लिपट कर लोगों के घरों में घुस चुकी थी। यह नया लिहाफ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में रंग कर पक्का हो चुका था। आारामदेह भी था। बस एक कमी थी। बिहार और गुजरात ने केंद्रीय राजनीति को कभी भी तय नहीं किया है। ज़रूरत थी कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रयोग हो। कह सकते हैं कि बिल्ली के भाग्य से छींका फूटा, हालांकि कार्य-कारण का वैज्ञानिक नियम समाज-राजनीति पर भी लागू होता है। वैश्विक स्तर पर घटने वाली घटनाओं से देश अछूता नहीं रह सकता, खासकर जब आर्थिक सीमाएं पारदर्शी हों। तो 2008 में पहली मंदी के बाद से जो हाल मध्य पूर्व और यूरोप के छोटे देशों का हुआ था, उसकी परिणति ”अरब स्प्रिंग’ के रूप में हुई। तानाशाही (स्वायत्त) सत्ताओं के खिलाफ एक ओर जहां मध्य-पूर्व में आंदोलन पनपा, वहीं भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल विधेयक की पीठ पर चढ़ कर समानांतर आंदोलन पैदा हुआ। एक साथ यह बात साफ होती गई कि अन्ना का आंदोलन भी उतना ही दक्षिणाभिमुख है जितना नाटो द्वारा समर्थित विद्रोहियों का लीबिया में आंदोलन। 2010 से 2011 के बीच पूरी दुनिया में नव-दक्षिणपंथी ताकतों को मज़बूती मिली, और इसे जनता के स्वत: स्फूर्त आंदोलन के रूप में पूंजी संचालित मीडिया ने पेश किया। हमें बताया गया कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद देश का पहला बड़ा आंदोलन लोकपाल के समर्थन में किया जा रहा है और अन्ना हज़ारे नए गांधी हैं। गौ रक्षा के नारों में भ्रष्टाचार विरोध का नारा मिल गया और दिल्ली के जंतर-मंतर पर अन्ना के मंच पर चढ़ने से जहां वामपंथी नेताओं को रोका गया, वहीं दूसरे भ्रष्ट नेताओं को भी वहां से खदेड़ दिया गया। यह पॉपुलर आंदोलन की ऐसी खिचड़ी थी जिसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी वीकेंड पर आकर दो बूंद घी डाल सकता था। यह शहरी मध्यवर्ग की नई क्रांति थी, जिसने भ्रष्टाचार को कांग्रेस का पर्याय बना कर भाजपा समेत बाकी सारे दलों को रियायत दे दी।
ज़ाहिर है, इतिहास की अपनी गति होती है और बीच में पैदा होने वाली विकृतियां उसे सिद्ध ही करती हैं। टीम अन्ना ने खुद को भाजपा से अलग दिखाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका अनशन तोड़ने आई एक मुस्लिम और एक दलित बच्ची अगले दस साल की भारतीय राजनीति का कम से कम संकेत तो कही जा सकती हैं। यह मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं था, न ही दलित सशक्तीकरण। यह एक बार फिर अपने स्वभाव से एक हिंदू राष्ट्र द्वारा मुस्लिमों और दलितों को ‘कोऑप्ट’ किए जाने का संकेत था। इसमें पुराने समाजवादी थे, गांधीवादी भी थे, सर्वोदयी थे और यहां तक कि मोहभंग की अवस्था प्राप्त कर चुके वामपंथी और वामपंथी दल भी शामिल थे। इसमें पांच सितारा अस्पताल के मालिक से लेकर कॉरपोरेट कारोबारी थे तो भ्रष्टाचार की पोषक ऑटो यूनियनों से लेकर व्यापारी संघ भी थे। नरेंद्र मोदी से शुरू हुआ नायक बनाने का खेल नीतिश कुमार से होते हुए कहां तक पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगाना वास्तव में छह महीने पहले मुश्किल था। और यह भी कहना मुश्किल था कि अन्ना का आंदोलन कहां, किसे मारेगा। हां, एक बात जो लगातार कुछ लोग कह रहे थे वो यह थी कि अन्ना का आंदोलन देश को बाबरी विध्वंस के बाद वाली स्थिति तक पीछे धकेल देगा। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की सत्ता में बुखारी की अपील पर आना क्या अब भी समझाने वाली बात रह गई है? ध्यान रहे मुलायम सिंह और उनकी समाजवादी पार्टी बाबरी विध्वंस की राजनीतिक पैदाइश हैं।
आशंकाओं के बीच
इस देश की जनता ने बाबरी विध्वंसकों को भी पचा लिया, मुलायम सिंह को भी। इसने विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी को भी पचा लिया और हिंदू आतंकवाद की शब्दावली गढ़ने वाले पी. चिदंबरम को भी बचा लिया। हिंदू सांप्रदायिक नेताओं के पीछे विकास खड़ा है तो बाकी सब के पीछे भ्रष्टाचार विरोध। गुजरात में भ्रष्टाचार कोई सवाल ही नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में विकास कोई सवाल नहीं। क्या हम पूछ सकते हैं कि मुलायम सिंह ने अपने कार्यकाल में विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, फिर भी क्यों चुन कर आए? क्या हम इमाम बुखारी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने ऐसे नेता को वोट देने की अपील एक समूची कौम से क्यों की? क्या हम अन्ना हज़ारे से पूछ सकते हैं कि उन्होंने जनता को क्यों नहीं आगाह किया कि अकेले बसपा और कांग्रेस ही नहीं, सपा भी भ्रष्ट है? क्या हम लाखों की भीड़ इकट्ठा करने वाले अरविंद केजरीवाल से पूछ सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड में उनके अभियान और खुद को सेकुलर बताने की कोशिशों के बावजूद वहां के लोगों ने भाजपा को क्यों नहीं साफ कर दिया? माफ करें, लेकिन क्या हम गुजरात के मुस्लिमों से पूछ सकते हैं कि वे बार-बार क्यों अनहद कार्यक्रमों में दंगों की बरसी मनाने दिल्ली आते हैं जहां उनका प्रचार कर के सिर्फ अगले कार्यक्रमों के लिए फंड जुटाया जाता है? क्या हम बहादुर पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट से पूछ सकते हैं कि अपने ऊपर हुए अत्याचार की लड़ाई में उन्होंने क्यों उसी एनजीओ द्वारा हाइजैक होना स्वीकार किया जो दस साल से सिर्फ लोगों की गवाहियां दिलवा रहा है?
सवाल और भी हैं। हम क्यों नहीं पूछें कि अगर रामजन्मभूमि मामले को कोर्ट में ही पनाह मिलनी थी, तो मस्जिद क्यों ढहाई गई? क्यों न हम पूछें कि समाचार चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में नरेंद्र मोदी के गुर्गों के चीख-चीख कर हत्या की स्वीकारोक्ति के बावजूद उसका कोई महत्व क्यों नहीं बन सका? बार-बार मोदी की जीत क्या वास्तव में यही कहती है कि मुसलमानों ने उन्हें माफ कर दिया है? ये सवाल पूछने में डर लगता है, लेकिन हम पूछेंगे कि क्या गुजरात-2002, बाबरी-1992, दिल्ली-1984, भोपाल-1984 सिर्फ तारीखें हैं जो लोगों की याद्दाश्त के हिसाब से धुल जाती हैं? साथ ही हम ये भी पूछेंगे कि 26/11 इन्हीं की तरह महज़ तारीख क्यों नहीं है, राष्ट्रीय गौरव पर हमला क्यों है? क्या ये तमाम ‘तारीखें’ भ्रष्टाचार और विकास की बहस से बाहर की चीज़ हैं? एक सवाल और। क्या 1992 से लेकर 2012 तक के बीस साल में हुए तमाम चुनावों में कभी भी अर्थनीति मुद्दा रही? अगर नहीं, तो क्यों?
अगर इनके जवाब हमें नहीं मिलते, यदि जो है सो ऐसा ही है, तो हम विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और धर्मनिरपेक्षता को क्यों न जनता के खिलाफ चलाए जा रहे एक ‘परपेचुअल’ युद्ध के औज़ार मान लें? हम क्यों न मान लें कि दरअसल सारे सीधे शब्दों में दरअसल उलटे अर्थ भर दिए गए हैं? और हम क्यों न मान लें कि मुलायम सिंह की उत्तर प्रदेश में हुई जीत सांप्रदायिक राजनीति के तीसरे चरण की आहट है, जहां विकास के आवरण की भी ज़रूरत नहीं रह जाती? दिक्कत सिर्फ एक है कि इन सारी मान्यताओं के बाद ‘पॉलिटिकली इनकरेक्ट’ हो जाने का खतरा मोल लेना पड़ता है।
दो दशक का मर्सिया
हमारा शुरुआती सवाल यही था कि गुजरात दंगों के दस साल बाद और बाबरी विध्वंस के बीसवें साल में हिंदुस्तान की सांप्रदायिक राजनीति का नया चेहरा कौन है। शब्दों को ज़रा सा सीधा कर लें, तो समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी- चूंकि सांप्रदायिकता को जनता में स्वीकार्य बनाया जा चुका है (बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों की सांप्रदायिकता), चूंकि उदारीकरण की अर्थनीति अब बेडरूम का हिस्सा बन चुकी है, लिहाजा ‘सांप्रदायिकता’ और ‘उदारीकरण’ अब जनता की थाती हैं। उसे ‘सांप्रदायिकता’ का दड़बा भी चाहिए और ‘उदारीकरण’ का खुला आकाश भी। वह जानती है कि जिस ‘विकास’ के लिए पिछले बीस साल में रास्ते बना दिए गए हैं और उसकी आदत जो ‘विकास’ बन चुका है, वह बिना मांगे भी उसे अब मिल जाएगा। इतना कुछ मिलने के बाद भी वह अपनी छवि का ख्याल न रखे तो लोग क्या कहेंगे। आखिर भारतीय दर्शन में व्यक्तिगत शुचिता सबसे ऊपर होती है। लिहाज़ा सबसे तेज़ चोर-चोर चीखना ज़रूरी है। चोरों पकड़े न जाएं, इसका इंतज़ाम करने के लिए उसके प्रतिनिधि हैं ही।
यह सांप्रदायिक राजनीति का नया चेहरा है- बिल्कुल साफ, स्वच्छ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर। बाबरी से शुरू हुआ आधुनिक सांप्रदायिकता का रथ गुजरात के राजमार्गों से होते हुए वापस यूपी साइकिल पर पहुंच चुका है। समय का एक चक्र पूरा हो गया है। धर्म और विकास के बाद अब भ्रष्टाचार विरोध की केंचुल में बैठी सांप्रदायिकता है यह, जिसके खिलाफ बोलना अपनी विश्वसनीयता को संकट में डाल देना है। ‘पॉलिटिकली इनकरेक्ट’ तो आप पहले से ही हो चुके होते हैं। इससे भी बढ़ कर चूंकि इस सांप्रदायिकता को संसदीय लोकतंत्र का जनादेश भी प्राप्त है, इसलिए इस पर सवाल उठाना खुद को असंसदीय भी ठहरा देना है, अपनी नागरिकता को खतरे में डालना है। और हिंदुस्तान का मुसलमान इतना कुछ गंवाने के बाद अब अपनी बची-खुची नागरिकता नहीं गंवा सकता। बाबरी की बीसवीं और गुजरात की दसवीं बरसी पर यही इस देश की श्रद्धांजलि है और यही उपलब्धि भी, अब इसे आप चाहे जो समझें।
संदर्भ
1. दंगों पर सारे तथ्य- सांप्रदायिकता का इतिहास: असगर अली इंजीनियर
2. क. हू किल्ड करकरे: एस.एम. मुशरिफ
ख. मालेगांव ब्लास्ट की चार्जशीट से मीडिया में लीक तथ्य (मुंबई मिरर, टाइम्स ऑफ इंडिया)
ग. 26/11 पर पाक अलर्ट प्रेस, अमरेश मिश्र, फि़रोज़ मिठिबोरवाला के आलेख
Read more